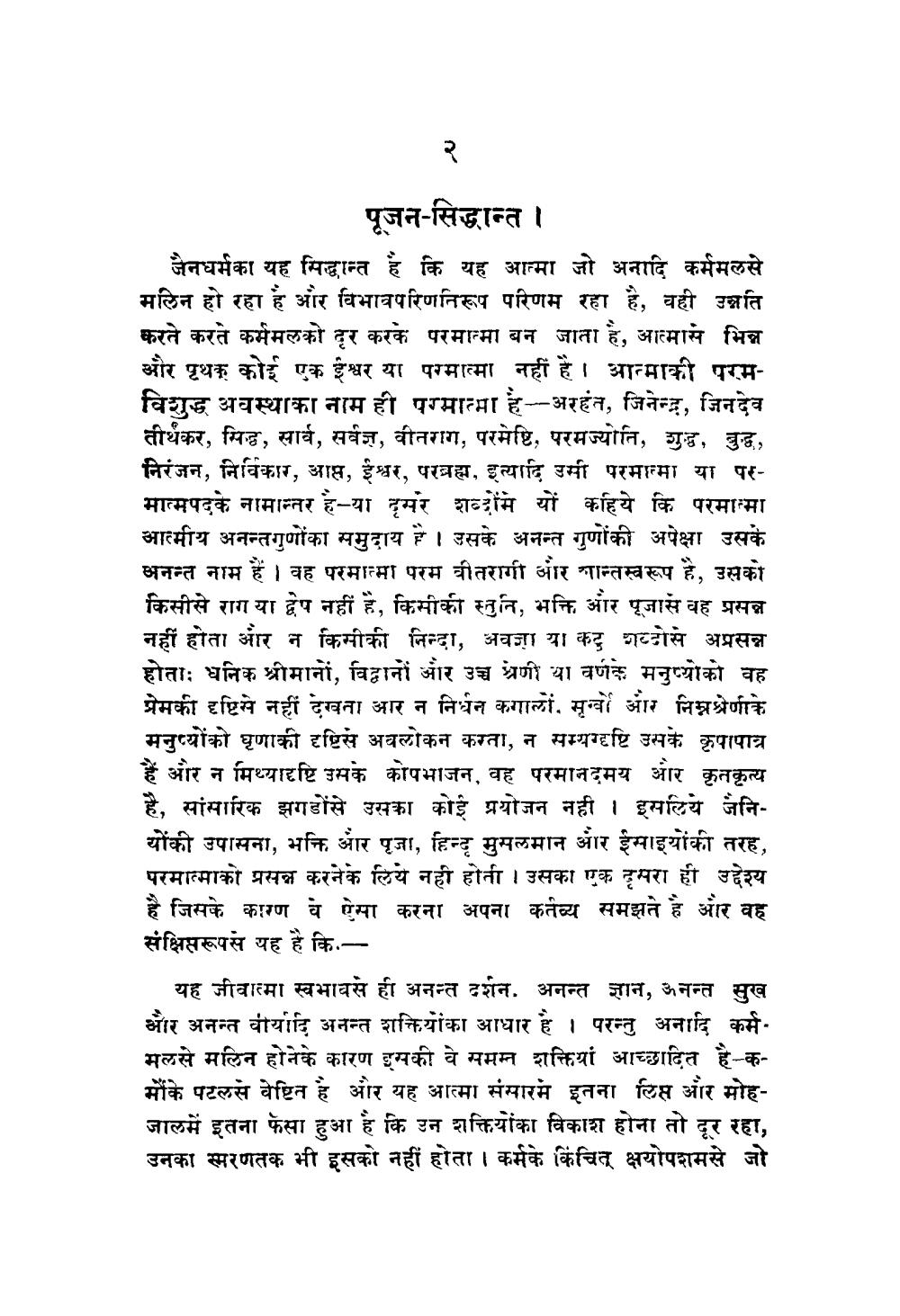________________
पूजन-सिद्धान्त । जैनधर्मका यह सिद्धान्त है कि यह आत्मा जो अनादि कर्ममलसे मलिन हो रहा है और विभावपरिणतिरूप परिणम रहा है, वही उन्नति करते करते कर्ममलको दर करके परमात्मा बन जाता है, आत्मास भिन्न
और पृथक् कोई एक ईश्वर या परमात्मा नहीं है। आत्माकी परमविशुद्ध अवस्थाका नाम ही परमात्मा है-अरहंत, जिनेन्द्र, जिनदेव तीर्थकर, सिद्ध, सार्व, सर्वज्ञ, वीतराग, परमेष्टि, परमज्योति, शुद्ध, बुद्ध, निरंजन, निर्विकार, आप्त, ईश्वर, परब्रह्म, इत्यादि उसी परमात्मा या परमात्मपदके नामान्तर है-या दृमर शब्दोंमे यों कहिये कि परमात्मा आत्मीय अनन्तगुणोंका समुदाय है । उसके अनन्त गुणोंकी अपेक्षा उसके अनन्त नाम हैं। वह परमात्मा परम वीतरागी और शान्तस्वरूप है, उसको किसीसे राग या द्वेप नहीं है, किमीकी स्तुनि, भक्ति और पूजास वह प्रसन्न नहीं होता और न किमीकी निन्दा, अवज्ञा या कद शब्दोसे अप्रसन्न होताः धनिक श्रीमानों, विद्वानों और उच्च श्रेणी या वर्णक मनुप्योको वह प्रेमकी दृष्टिसे नहीं देखना आर न निर्धन कगालों. मृर्वो और निम्नश्रेणीके मनुप्योंको घृणाकी दृष्टिसं अवलोकन करता, न सम्यग्दृष्टि उसके कृपापात्र हैं और न मिथ्यादृष्टि उसके कोपभाजन, वह परमानदमय और कृतकृत्य है, सांसारिक झगडोंसे उसका कोई प्रयोजन नही । इसलिये जैनियोंकी उपासना, भक्ति और पूजा, हिन्द मुसलमान और ईसाइयोंकी तरह, परमात्माको प्रसन्न करने के लिये नहीं होती । उसका एक दृप्सरा ही उद्देश्य है जिसके कारण वे ऐसा करना अपना कर्तव्य समझते है और वह संक्षिप्तरूपस यह है कि.
यह जीवात्मा स्वभावसे ही अनन्त दर्शन. अनन्त ज्ञान, अनन्त सुख और अनन्त वीर्यादि अनन्त शक्तियोंका आधार है । परन्तु अनादि कर्म मलसे मलिन होनेके कारण इसकी वे समम्न शक्तियां आच्छादित है-कमौके पटलसे वेष्टित है और यह आत्मा संसारम इतना लिप्त और मोहजालमें इतना फेसा हुआ है कि उन शक्तियोंका विकाश होना तो दूर रहा, उनका स्मरणतक भी इसको नहीं होता । कर्मके किंचित् क्षयोपशमसे जो