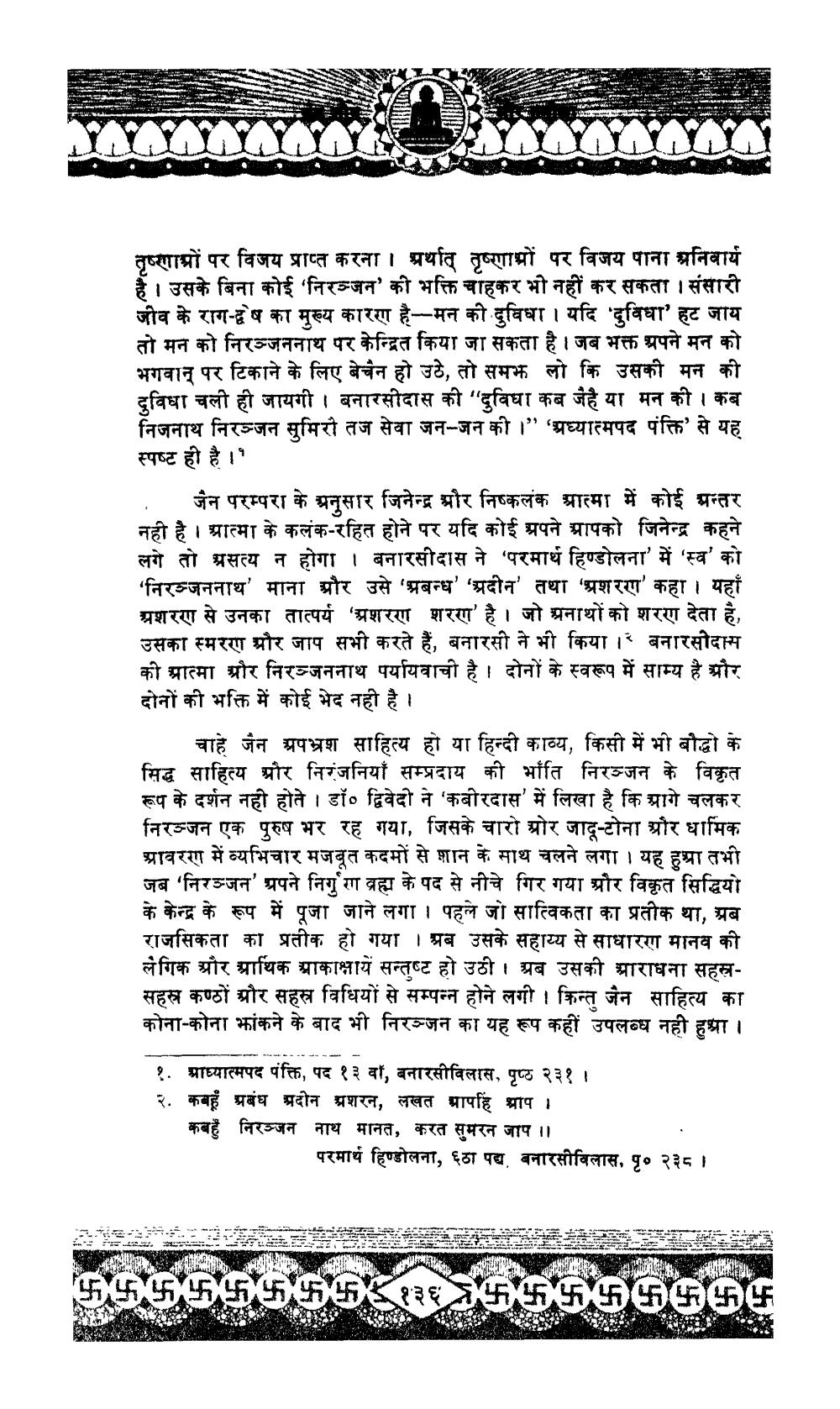________________
wwww
तृष्णाओं पर विजय प्राप्त करना । श्रर्थात् तृष्णाभों पर विजय पाना अनिवार्य है । उसके बिना कोई 'निरञ्जन' की भक्ति चाहकर भी नहीं कर सकता । संसारी जीव के राग-द्वेष का मुख्य कारण है--मन की दुविधा । यदि 'दुविधा' हट जाय तो मन को निरञ्जननाथ पर केन्द्रित किया जा सकता है। जब भक्त अपने मन को भगवान् पर टिकाने के लिए बेचैन हो उठे, तो समझ लो कि उसकी मन की दुविधा चली ही जायगी । बनारसीदास की "दुविधा कब जैहै या मन की । कब निजनाथ निरञ्जन सुमिरौ तज सेवा जन-जन की ।" 'अध्यात्मपद पंक्ति' से यह स्पष्ट ही है । "
जैन परम्परा के अनुसार जिनेन्द्र और निष्कलंक आत्मा में कोई अन्तर नही है । श्रात्मा के कलंक - रहित होने पर यदि कोई अपने आपको जिनेन्द्र कहने लगे तो असत्य न होगा । बनारसीदास ने 'परमार्थ हिण्डोलना' में 'स्व' को 'निरञ्जननाथ' माना और उसे 'प्रबन्ध' 'दीन' तथा 'अशररण' कहा । यहाँ अशरण से उनका तात्पर्य 'अशरण शरण' है । जो अनाथों को शरण देता है, उसका स्मरण और जाप सभी करते हैं, बनारसी ने भी किया । बनारसीदाम की आत्मा और निरञ्जननाथ पर्यायवाची है । दोनों के स्वरूप में साम्य है और दोनों की भक्ति में कोई भेद नही है ।
चाहे जैन अपभ्रंश साहित्य हो या हिन्दी काव्य, किसी में भी बौद्धो के सिद्ध साहित्य और निरंजनियाँ सम्प्रदाय की भाँति निरञ्जन के विकृत रूप के दर्शन नही होते । डॉ० द्विवेदी ने 'कबीरदास' में लिखा है कि आगे चलकर निरञ्जन एक पुरुष भर रह गया, जिसके चारो प्रोर जादू-टोना और धार्मिक आवरण में व्यभिचार मजबूत कदमों से शान के साथ चलने लगा। यह हुआ तभी जब 'निरञ्जन' श्रपने निर्गुण ब्रह्म के पद से नीचे गिर गया और विकृत सिद्धियो के केन्द्र के रूप में पूजा जाने लगा। पहले जो सात्विकता का प्रतीक था, अब राजसिकता का प्रतीक हो गया । अब उसके सहाय्य से साधारण मानव की लैंगिक और आर्थिक आकाक्षायें सन्तुष्ट हो उठी। अब उसकी आराधना सहस्रसहस्र कण्ठों और सहस्र विधियों से सम्पन्न होने लगी । किन्तु जैन साहित्य का कोना-कोना झांकने के बाद भी निरञ्जन का यह रूप कहीं उपलब्ध नही हुआ ।
१. श्राध्यात्मपद पंक्ति, पद १३ वॉ, बनारसीविलास, पृष्ठ २३१ ।
२. कबहूं प्रबंध प्रदीन अशरन, लखत प्रापहि श्राप । कबहुँ निरञ्जन नाथ मानत, करत सुमरन जाप ।।
परमार्थ हिण्डोलना, ६ठा पद्य, बनारसीविलास, पृ० २३८ ।
फफफफफफफफ १३६ फफफफफफफ