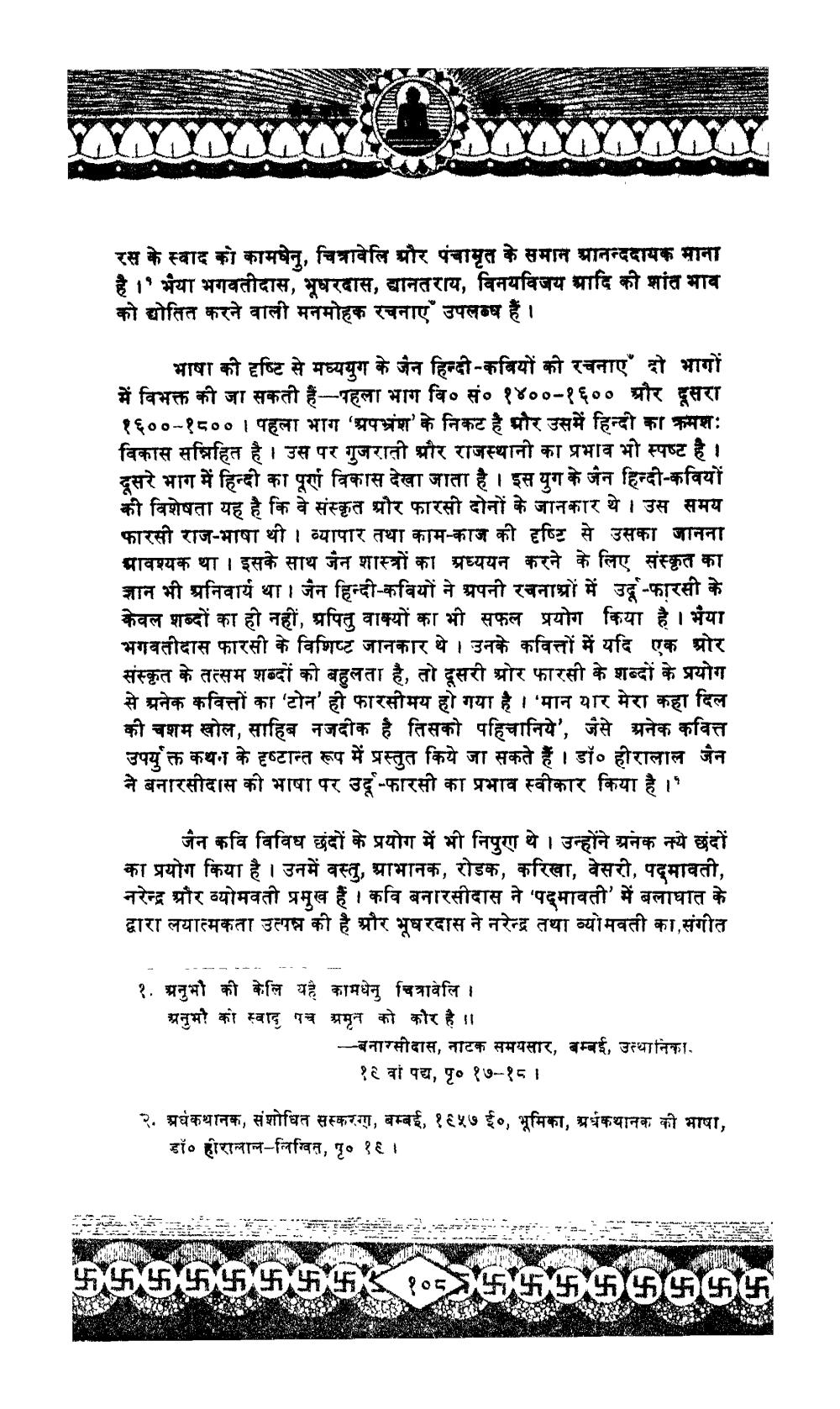________________
0000
रस के स्वाद को कामधेनु, चित्रावेलि और पंचामृत के समान आनन्ददायक माना है ।" भैया भगवतीदास, भूधरदास, बानतराय, विनयविजय आदि की शांत भाव को द्योतित करने वाली मनमोहक रचनाएँ उपलब्ध हैं ।
भाषा की दृष्टि से मध्ययुग के जैन हिन्दी कवियों की रचनाएँ दो भागों में विभक्त की जा सकती हैं- पहला भाग वि० सं० १४००-१६०० और दूसरा १६००-१८०० | पहला भाग 'अपभ्रंश' के निकट है और उसमें हिन्दी का क्रमशः विकास सन्निहित है । उस पर गुजराती और राजस्थानी का प्रभाव भी स्पष्ट है । दूसरे भाग में हिन्दी का पूर्ण विकास देखा जाता है। इस युग के जैन हिन्दी कवियों की विशेषता यह है कि वे संस्कृत और फारसी दोनों के जानकार थे । उस समय फारसी राज-भाषा थी । व्यापार तथा काम-काज की दृष्टि से उसका जानना श्रावश्यक था । इसके साथ जैन शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए संस्कृत का ज्ञान भी अनिवार्य था। जैन हिन्दी-कवियों ने अपनी रचनात्रों में उर्दू-फारसी के केवल शब्दों का ही नहीं, अपितु वाक्यों का भी सफल प्रयोग किया है। भैया भगवतीदास फारसी के विशिष्ट जानकार थे । उनके कवित्तों में यदि एक ओर संस्कृत के तत्सम शब्दों की बहुलता है, तो दूसरी ओर फारसी के शब्दों के प्रयोग से अनेक कवित्तों का 'टोन' ही फारसीमय हो गया है । 'मान यार मेरा कहा दिल की चशम खोल, साहिब नजदीक है तिसको पहिचानिये', जैसे अनेक कवित्त उपर्युक्त कथन के दृष्टान्त रूप में प्रस्तुत किये जा सकते हैं। डॉ० हीरालाल जैन ने बनारसीदास की भाषा पर उर्दू-फारसी का प्रभाव स्वीकार किया है । "
-
जैन कवि विविध छंदों के प्रयोग में भी निपुण थे। उन्होंने अनेक नये छंदों का प्रयोग किया है । उनमें वस्तु, आभानक, रोडक, करिखा, वेसरी, पद्मावती, नरेन्द्र और व्योमवती प्रमुख हैं । कवि बनारसीदास ने 'पद्मावती' में बलाघात के द्वारा लयात्मकता उत्पन्न की है और भूधरदास ने नरेन्द्र तथा व्योमवती का, संगीत
१. अनुभो की केलि यह कामधेनु चित्रावेलि । अभी को स्वादु पच
अमृत को कौर है ।
- बनारसीदास, नाटक समयसार, बम्बई, उत्थानिका
१० वां पद्य, पृ० १७-१८ ।
२. अर्धकथानक, संशोधित संस्करण, बम्बई, १६५७ ई०, भूमिका, अर्धकथानक की भाषा, डॉ० हीरालाल - लिखित, पृ० १६ ।
5 5 5 5 5 5 १०55555555
596995