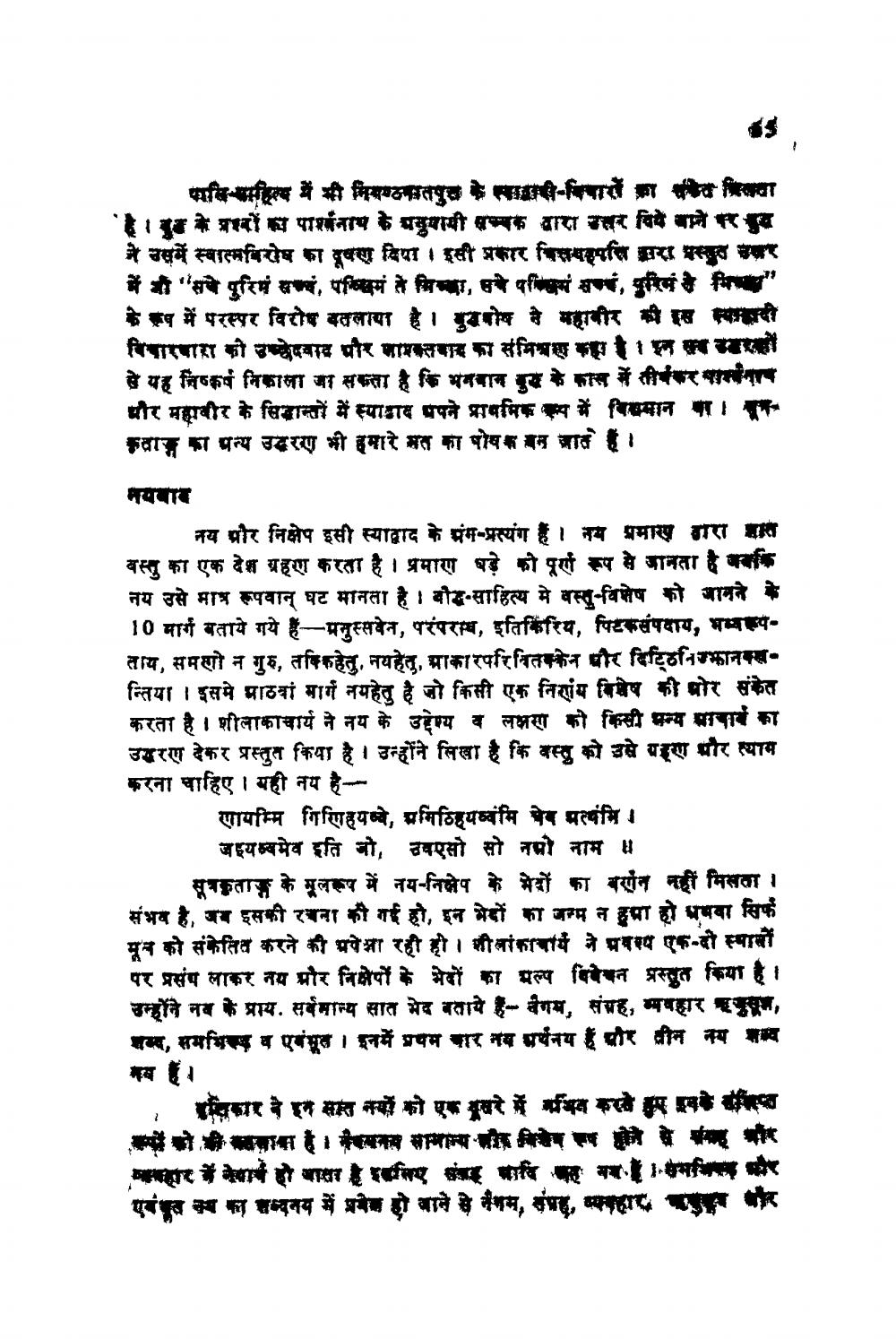________________
पहिल्य में भी नया
केस विचारों का वि 'है। बुद्ध के प्रश्नों का पार्श्वनाथ के अनुयायी सम्पक द्वारा उत्तर दिये जाने पर बुद्ध ने उसमें स्वात्मविरोध का दूवा दिया। इसी प्रकार विपति द्वारा प्रस्तुत में भी "सबै पुरिमं खच्यं, पछि ते चिच्चा, सबै पन्धिमं सच्चे पुरिमं से" के रूप में परस्पर विरोध बतलाया है । बुद्धपोष ने महावीर की इस स्वादी विचारधारा को उच्छेदवाद पीर माक्सबाद का संमिश्र कहा है । इन से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि भगवान बुद्ध के काल में तीर्थकर पाना और महावीर के सिद्धान्तों में स्वाद्वाद अपने प्राथमिक रूप में विद्यमान था । सूनकवाङ्ग का अन्य उद्धरण भी हमारे मत का पोषक बन जाते हैं ।
मयवाद
नय और निक्षेप इसी स्याद्वाद के अंग-प्रत्यंग हैं। नय प्रमाण द्वारा वस्तु का एक देश ग्रहण करता है । प्रमाण घड़े को पूर्ण रूप से जानता है जबकि नय उसे मात्र रूपवान् घट मानता है। बोद्ध-साहित्य मे वस्तु-विशेष को जानने के 10 मार्ग बताये गये हैं- प्रतुस्तवेन, परंपरा, इतिकिंरिय, पिटकसंपदाय, भव्यरूपताय, समणो न गुरु, तक्किहेतु, नयहेतु, आकारपरिचितक्केन धीर दिट्ठिनिज्झानक्खन्तिया । इसमे भाठवां मार्ग नमहेतु है जो किसी एक निर्णय विशेष की धोर संकेत करता है । शीलाकाचार्य ने नय के उद्देश्य व लक्षण को किसी अन्य प्राचार्य का उद्धरण देकर प्रस्तुत किया है। उन्होंने लिखा है कि वस्तु को उसे ग्रहण और स्थान करना चाहिए । यही नय है
सायम्मि गिरिणयब्बे, प्रमिठिहयध्वंसि भेव प्रत्यंगि aeroयमेव इति जो, उबएसो सो नम्रो नाम
सूत्रकृताङ्ग के मूलरूप में नय-निक्षेप के भेदों का वर्णन नहीं मिलता । संभव है, जब इसकी रचना की गई हो, इन भेदों का जन्म न हुआ हो भ्रमवा सिर्फ मूल को संकेतित करने की अपेक्षा रही हो । शीलांकाचार्य ने प्रवस्य एक-दो स्थानों पर प्रसंग लाकर नय और निक्षेपों के भेदों का प्रल्प विवेचन प्रस्तुत किया है। उन्होंने नब के प्राय. सर्वमान्य सात भेद बताये हैं- वेगम, संग्रह, व्यवहार शब्द, समभिरूद व एवंभूत। इनमें प्रथम चार नव अर्थनय हैं और तीन नय सब्य सब हैं।
कार ने इन सात नयों को एक दूसरे में करते हुए इसके कोकी है। सामान्य विशेष रूप से व्यवहार में नेवाने हो जाता है इसलिए यदि यह मग हूँ - समर एवं नमक नय में प्रवेश हो जाने से नैगम, संव्यवहार