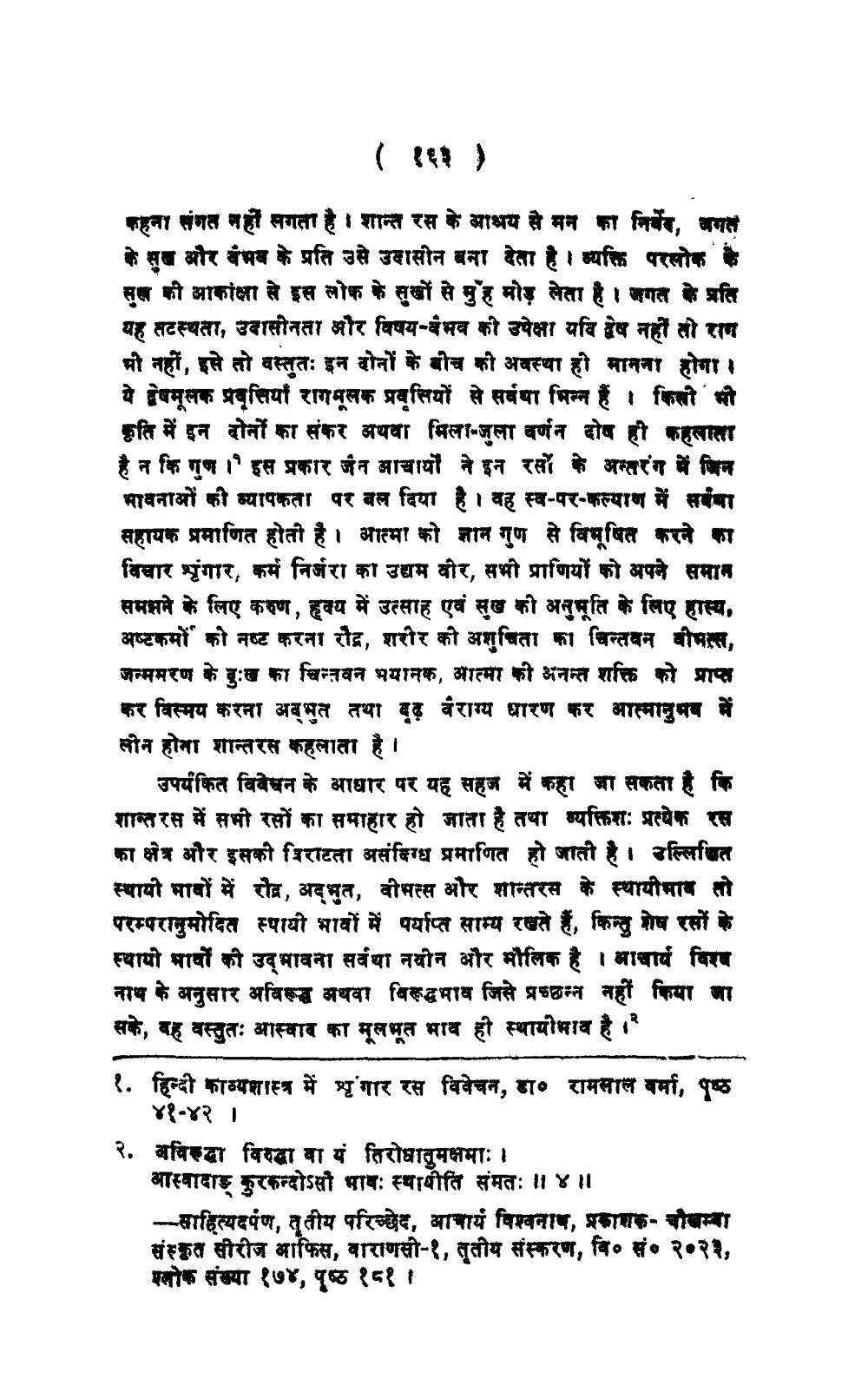________________
( १६३ )
वगत
कहना संगत नहीं लगता है। शान्त रस के आश्रय से मन का निर्वेद, के सुख और वैभव के प्रति उसे उदासीन बना देता है । व्यक्ति परलोक सुख की आकांक्षा से इस लोक के सुखों से मुँह मोड़ लेता है । जगत के प्रति यह तटस्थता, उदासीनता और विषय-वैभव की उपेक्षा यदि द्वेष नहीं तो राम भी नहीं, इसे तो वस्तुतः इन दोनों के बीच की अवस्था हो मानना होगा । ये द्वेषमूलक प्रवृतियाँ रागमूलक प्रवृतियों से सर्वथा भिन्न हैं । किसी भी कृति में इन दोनों का संकर अथवा मिला-जुला वर्णन दोष ही कहलाता है न कि गुण ।" इस प्रकार जैन आचार्यों ने इन रसों के अन्तरंग में जिन भावनाओं की व्यापकता पर बल दिया है। वह स्व-पर-कल्याण में सर्वा सहायक प्रमाणित होती है। आत्मा को ज्ञान गुण से विभूषित करने का विचार श्रृंगार, कर्म निर्जरा का उद्यम वीर, सभी प्राणियों को अपने समान समझने के लिए करुण, हृक्य में उत्साह एवं सुख की अनुभूति के लिए हास्य, अष्टकों को नष्ट करना रौद्र, शरीर को अशुचिता का चिन्तवन बीभत्स, जन्ममरण के दुःख का चिन्तवन भयानक, आत्मा की अनन्त शक्ति को प्राप्त कर विस्मय करना अद्भुत तथा दृढ़ वंराग्य धारण कर आत्मानुभव में लोन होगा शान्तरस कहलाता है ।
उपर्यंत विवेचन के आधार पर यह सहज में कहा जा सकता है कि शान्तरस में सभी रसों का समाहार हो जाता है तथा व्यक्तिशः प्रत्येक रस का क्षेत्र और इसकी विराटता असंदिग्ध प्रमाणित हो जाती है । उल्लिखित स्थायी भावों में रौद्र, अद्भुत, वीभत्स और शान्तरस के स्थायीभाव तो परम्परानुमोदित स्थायी भावों में पर्याप्त साम्य रखते हैं, किन्तु शेष रसों के स्थायी भावों की उद्भावना सर्वथा नवीन और मौलिक है । आचार्य विश्व नाथ के अनुसार अविरूद्ध अथवा विरूद्धभाव जिसे प्रच्छन्न नहीं किया जा सके, वह वस्तुतः आस्वाद का मूलभूत भाव ही स्थायीभाव है ।"
१. हिन्दी काव्यशास्त्र में शृंगार रस विवेचन, डा० रामलाल वर्मा, पृष्ठ ४१-४२ ।
२. aftear विरुद्धा वा यं तिरोधातुमक्षमाः ।
आस्वादाङ् कुरकन्दोsaौ भावः स्थायीति संमतः ॥ ४ ॥
-साहित्यदर्पण, तृतीय परिच्छेद, आचार्य विश्वनाथ, प्रकाशक- चौखम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी-१, तृतीय संस्करण, वि० सं० २०२३, श्लोक संख्या १७४, पृष्ठ १८१ ।