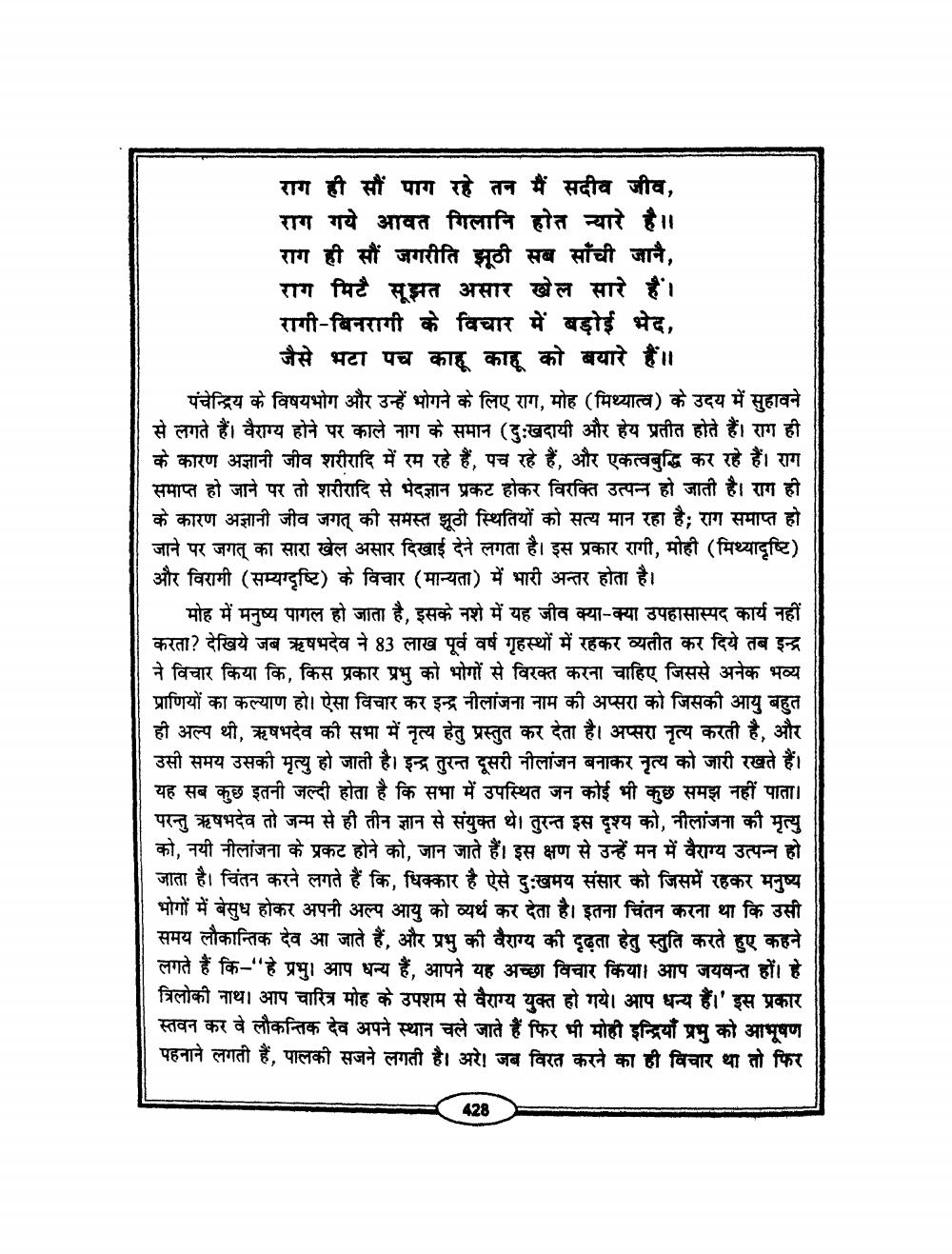________________
राग ही सौं पाग रहे तन मैं सदीव जीव, राग गये आवत गिलानि होत न्यारे है। राग ही सौं जगरीति झूठी सब साँची जानै, राग मिटै सूझत असार खेल सारे हैं। रागी-बिनरागी के विचार में बड़ोई भेद,
जैसे भटा पच काहू काहू को बयारे हैं। पंचेन्द्रिय के विषयभोग और उन्हें भोगने के लिए राग, मोह (मिथ्यात्व) के उदय में सुहावने से लगते हैं। वैराग्य होने पर काले नाग के समान (दु:खदायी और हेय प्रतीत होते हैं। राग ही के कारण अज्ञानी जीव शरीरादि में रम रहे हैं, पच रहे हैं, और एकत्वबुद्धि कर रहे हैं। राग समाप्त हो जाने पर तो शरीरादि से भेदज्ञान प्रकट होकर विरक्ति उत्पन्न हो जाती है। राग ही के कारण अज्ञानी जीव जगत् की समस्त झूठी स्थितियों को सत्य मान रहा है; राग समाप्त हो जाने पर जगत् का सारा खेल असार दिखाई देने लगता है। इस प्रकार रागी, मोही (मिथ्यादृष्टि) और विरामी (सम्यग्दृष्टि) के विचार (मान्यता) में भारी अन्तर होता है।
मोह में मनुष्य पागल हो जाता है, इसके नशे में यह जीव क्या-क्या उपहासास्पद कार्य नहीं करता? देखिये जब ऋषभदेव ने 83 लाख पूर्व वर्ष गृहस्थों में रहकर व्यतीत कर दिये तब इन्द्र ने विचार किया कि, किस प्रकार प्रभु को भोगों से विरक्त करना चाहिए जिससे अनेक भव्य प्राणियों का कल्याण हो। ऐसा विचार कर इन्द्र नीलांजना नाम की अप्सरा को जिसकी आयु बहुत ही अल्प थी, ऋषभदेव की सभा में नृत्य हेतु प्रस्तुत कर देता है। अप्सरा नृत्य करती है, और उसी समय उसकी मृत्यु हो जाती है। इन्द्र तुरन्त दूसरी नीलांजन बनाकर नृत्य को जारी रखते हैं। यह सब कुछ इतनी जल्दी होता है कि सभा में उपस्थित जन कोई भी कुछ समझ नहीं पाता। परन्तु ऋषभदेव तो जन्म से ही तीन ज्ञान से संयुक्त थे। तुरन्त इस दृश्य को, नीलांजना की मृत्यु को, नयी नीलांजना के प्रकट होने को, जान जाते हैं। इस क्षण से उन्हें मन में वैराग्य उत्पन्न हो जाता है। चिंतन करने लगते हैं कि, धिक्कार है ऐसे दु:खमय संसार को जिसमें रहकर मनुष्य भोगों में बेसुध होकर अपनी अल्प आयु को व्यर्थ कर देता है। इतना चिंतन करना था कि उसी समय लौकान्तिक देव आ जाते हैं, और प्रभु की वैराग्य की दृढ़ता हेतु स्तुति करते हुए कहने लगते हैं कि-"हे प्रभु। आप धन्य हैं, आपने यह अच्छा विचार किया। आप जयवन्त हों। हे त्रिलोकी नाथ। आप चारित्र मोह के उपशम से वैराग्य युक्त हो गये। आप धन्य हैं।' इस प्रकार स्तवन कर वे लौकन्तिक देव अपने स्थान चले जाते हैं फिर भी मोही इन्द्रियाँ प्रभु को आभूषण पहनान लगती हैं, पालकी सजने लगती है। अरे। जब विरत करने का ही विचार था तो फिर
-
428