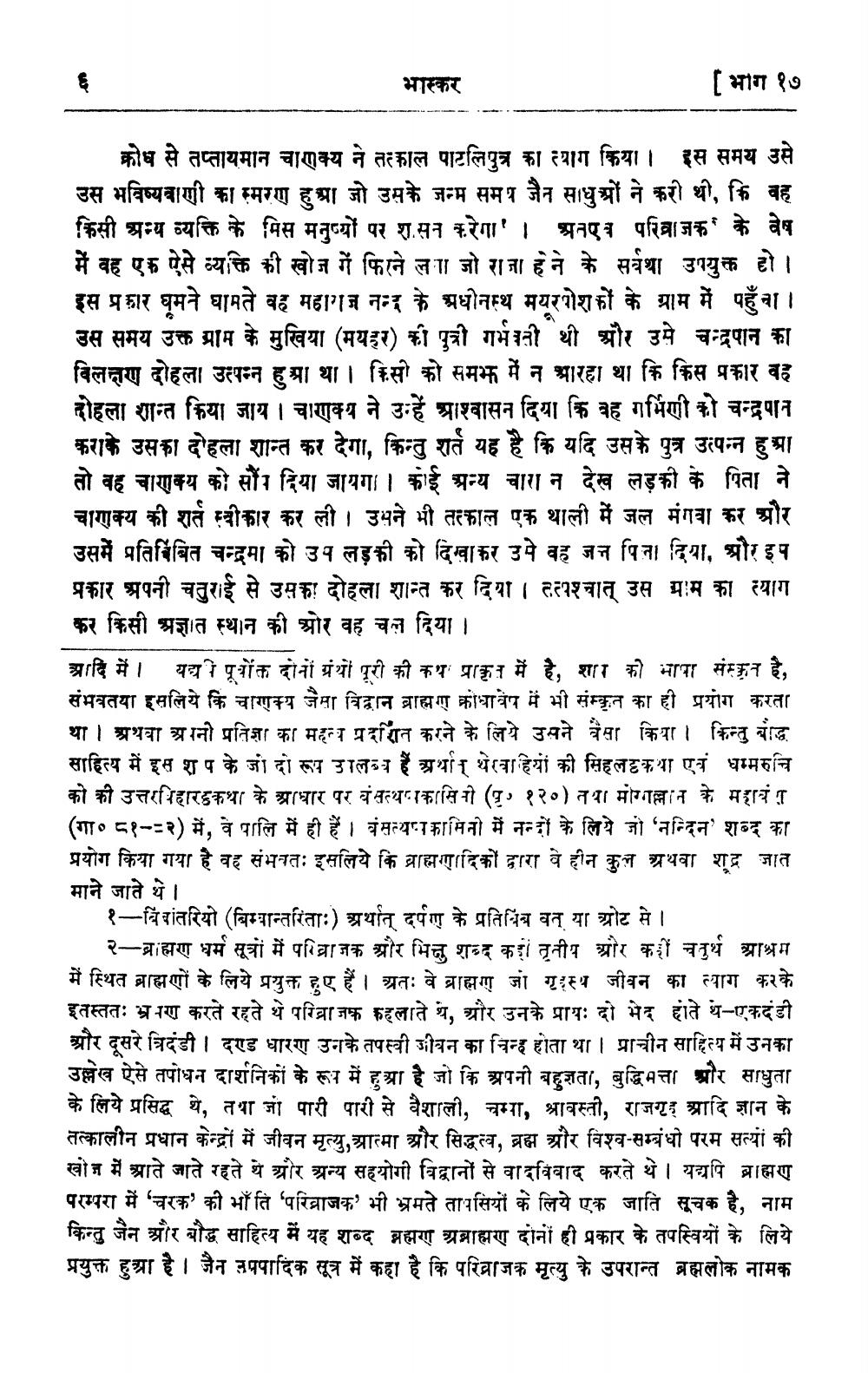________________
[ भाग १७
क्रोध से तप्तायमान चाणक्य ने तत्काल पाटलिपुत्र का त्याग किया। इस समय उसे उस भविष्यवाणी का स्मरण हुआ जो उसके जन्म समय जैन साधुओं ने करी थी, कि वह किसी अन्य व्यक्ति के मिस मनुष्यों पर शासन करेगा' । अतएव परिव्राजक के वेष में वह एक ऐसे व्यक्ति की खोज में फिरने लगा जो राजा हेने के सर्वथा उपयुक्त हो । इस प्रकार घूमने घामते वह महाराज नन्द के अधीनस्थ मयूरगेशकों के ग्राम में पहुँचा । उस समय उक्त ग्राम के मुखिया (मयहर) की पुत्री गर्भवती थी और उसे चन्द्रपान का विलक्षण दोहला उत्पन्न हुआ था। किसी को समझ में न आारहा था कि किस प्रकार वह दोहला शान्त किया जाय । चाणक्य ने उन्हें श्राश्वासन दिया कि वह गर्भिणी को चन्द्रपान कराके उसका दोहला शान्त कर देगा, किन्तु शर्त यह है कि यदि उसके पुत्र उत्पन्न हुआ तो वह चाणक्य को सौंप दिया जायगा । कोई अन्य चारा न देख लड़की के पिता ने चाणक्य की शर्त स्वीकार कर ली। उसने भी तत्काल एक थाली में जल मंगवा कर और उसमें प्रतिबिंबित चन्द्रमा को उप लड़की को दिखाकर उसे वह जन पिता दिया, और इस प्रकार अपनी चतुराई से उसका दोहला शान्त कर दिया। तत्पश्चात् उस ग्राम का त्याग कर किसी अज्ञात स्थान की ओर वह चल दिया ।
भास्कर
आदि में । पूर्वोक्त दोनों ग्रंथों पूरी की कथ प्राकृत में है, शार को भाषा संस्कृत है, संभवतया इसलिये किं चाणक्य जैसा विद्वान ब्राह्मण क्रोधावेव में भी संस्कृत का ही प्रयोग करता था । अथवा अपनी प्रतिज्ञा का महत्व प्रदर्शित करने के लिये उसने वैसा किया । किन्तु बौद्ध साहित्य में इस शप के जो दो रूप उपलब्ध हैं अर्थात् थेरवाहियों की सिहल कथा एवं धम्मरुचि को की उत्तरविहारकथा के आधार पर सत्थकासिनी ( १२० ) तथा मोग्गल्लान के महावं ( गा० ८१-८२) में, वे पालि में ही हैं । सत्यपकामिनी में नन्दों के लिये जो 'नन्दिन' शब्द का प्रयोग किया गया है वह संभवतः इसलिये कि ब्राह्मणादिकों द्वारा वे हीन कुल अथवा शूद्र जात माने जाते थे ।
१ - विचांतरियो (बिम्वान्तरिताः) अर्थात् दर्पण के प्रतिनित्रवत् या चोट से ।
२ – ब्राह्मण धर्म सूत्रों में परिव्राजक और भिक्षु शब्द कहीं तृतीय और कहीं चतुर्थ श्राश्रम में स्थित ब्राह्मणों के लिये प्रयुक्त हुए हैं । अतः वे ब्राह्मण जो गृहस्थ जीवन का त्याग करके इतस्ततः भ्रमण करते रहते थे परिव्राजक कहलाते थे, और उनके प्रायः दो भेद होते थे - एकदंडी और दूसरे त्रिदंडी । दण्ड धारण उनके तपस्वी जीवन का चिन्ह होता था । प्राचीन साहित्य में उनका उल्लेख ऐसे तपोधन दार्शनिकों के रूप में हुआ है जो कि अपनी बहुज्ञता, बुद्धिमत्ता और साधुता के लिये प्रसिद्ध थे, तथा जो पारी पारी से वैशाली, चम्मा, श्रावस्ती, राजगृह आदि ज्ञान के तत्कालीन प्रधान केन्द्रों में जीवन मृत्यु, आत्मा और सिद्धत्व, ब्रह्म और विश्व सम्बंधो परम सत्यों की खोज में आते जाते रहते थे और अन्य सहयोगी विद्वानों से वादविवाद करते थे । यद्यपि ब्राह्मण परम्परा में 'चरक' की भाँति 'परिव्राजक' भी भ्रमते तापसियों के लिये एक जाति सूचक है, नाम किन्तु जैन और बौद्ध साहित्य में यह शब्द ब्रह्मण नाह्मण दोनों ही प्रकार के तपस्वियों के लिये प्रयुक्त हुआ है। जैन उपपादिक सूत्र में कहा है कि परिव्राजक मृत्यु के उपरान्त ब्रह्मलोक नामक