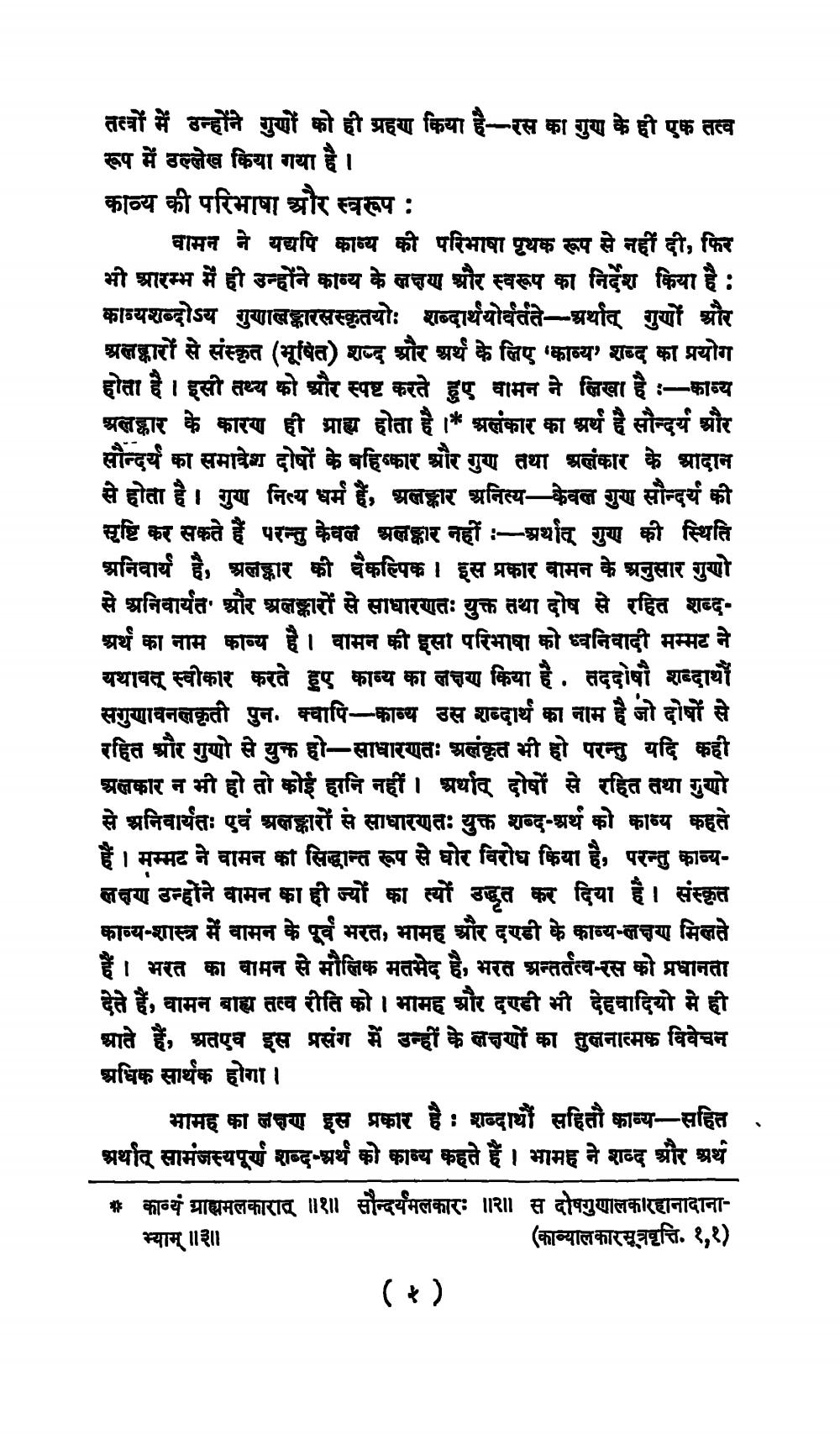________________
तत्त्रों में उन्होंने गुणों को ही ग्रहण किया है - रस का गुण के ही एक तत्व रूप में उल्लेख किया गया है ।
काव्य की परिभाषा और स्वरूप :
वामन ने यद्यपि काव्य की परिभाषा पृथक रूप से नहीं दी, फिर भी आरम्भ में ही उन्होंने काव्य के लक्षण और स्वरूप का निर्देश किया है : काव्यशब्दोऽय गुणालङ्कारसस्कृतयोः शब्दार्थयोर्वर्तते - अर्थात् गुणों और अलङ्कारों से संस्कृत (भूषित) शब्द और अर्थ के लिए 'काव्य' शब्द का प्रयोग होता है । इसी तथ्य को और स्पष्ट करते हुए वामन ने लिखा है :- काव्य अलङ्कार के कारण ही ग्राह्य होता है । * अलंकार का अर्थ है सौन्दर्य और सौन्दर्य का समावेश दोषों के बहिष्कार और गुण तथा अलंकार के आदान से होता है । गुण नित्य धर्म हैं, अलङ्कार अनित्य — केवल गुण सौन्दर्य की सृष्टि कर सकते हैं परन्तु केवल अलङ्कार नहीं : अर्थात् गुण की स्थिति अनिवार्य है, अलङ्कार की वैकल्पिक । इस प्रकार वामन के अनुसार गुणो से अनिवार्यत और अलङ्कारों से साधारणतः युक्त तथा दोष से रहित शब्दअर्थ का नाम काव्य है । वामन की इसा परिभाषा को ध्वनिवादी मम्मट ने यथावत् स्वीकार करते हुए काव्य का लक्षण किया है. तददोषौ शब्दार्थों सगुणावनलकृती पुनः क्वापि - काव्य उस शब्दार्थ का नाम है जो दोषों से रहित और गुणों से युक्त हो— साधारणतः अलंकृत भी हो परन्तु यदि कही अलकार न भी हो तो कोई हानि नहीं । अर्थात् दोषों से रहित तथा गुणो से अनिवार्यतः एवं श्रलङ्कारों से साधारणतः युक्त शब्द- श्रर्थ को काव्य कहते हैं । मम्मट ने वामन का सिद्धान्त रूप से घोर विरोध किया है, परन्तु काव्यलक्षण उन्होंने वामन का ही ज्यों का त्यों उद्धृत कर दिया है । संस्कृत काव्य-शास्त्र में वामन के पूर्व भरत, भामह और दरडी के काव्य-लक्षण मिलते
। भरत का वामन से मौलिक मतभेद है, भरत अन्तर्तत्व- रस को प्रधानता देते हैं, वामन बाह्य तत्व रीति को । भामह और दरडी भी देहवादियो मे ही आते हैं, अतएव इस प्रसंग में उन्हीं के लक्षणों का तुलनात्मक विवेचन अधिक सार्थक होगा ।
भामह का लक्षण इस प्रकार है : शब्दार्थों सहितौ काव्य- सहित अर्थात् सामंजस्यपूर्णं शब्द-अर्थं को काव्य कहते हैं
।
भामह ने शब्द और अर्थ
* काव्यं ग्राह्यमलकारात् ||१|| सौन्दर्यमलकारः ॥२॥
भ्याम् ॥३॥
(+)
स दोषगुणालक | रहानादाना
(कान्याल कारसूत्रवृत्ति. १, १ )