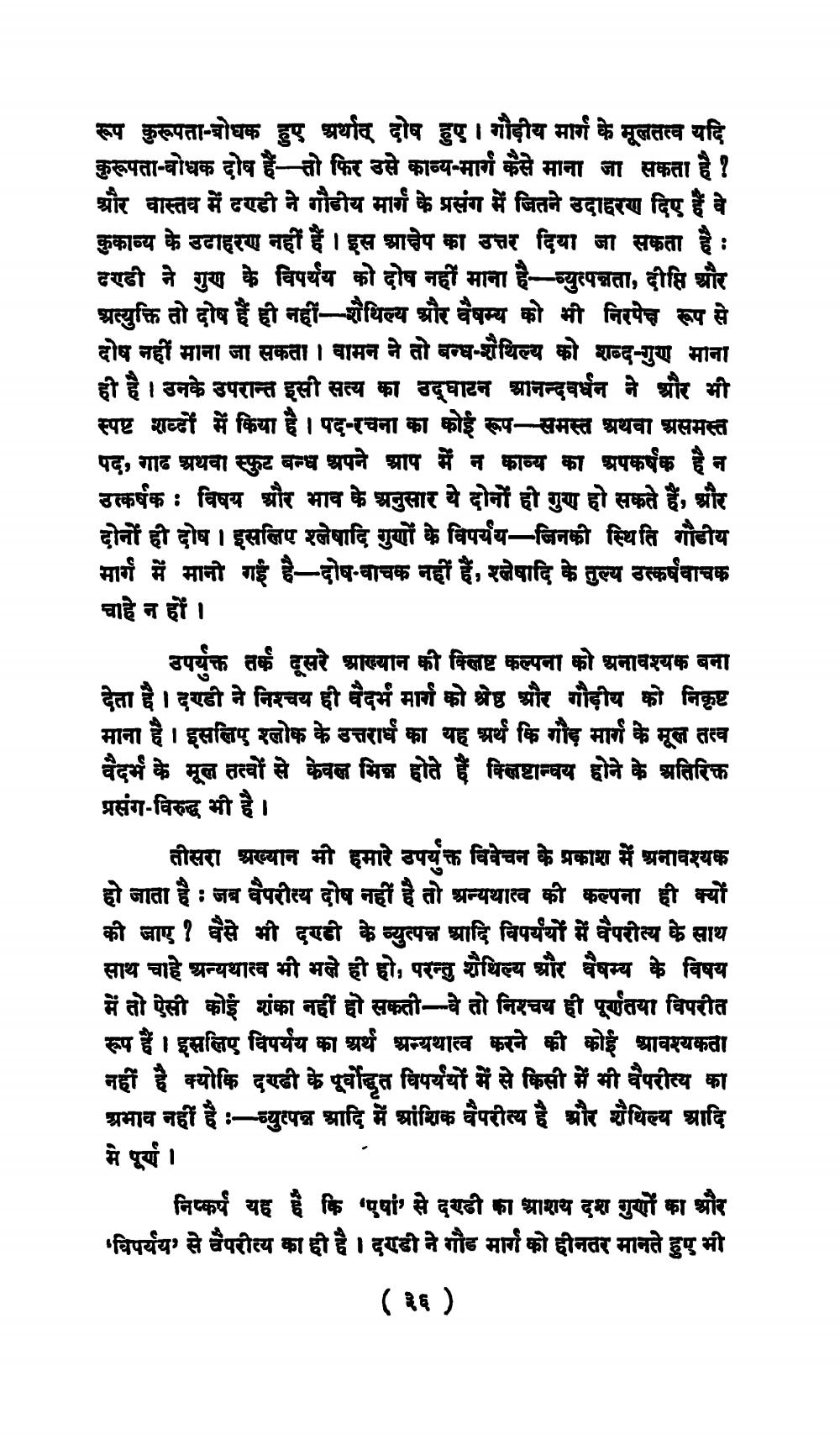________________
रूप कुरूपता-बोधक हुए अर्थात् दोष हुए । गौड़ीय मार्ग के मूलतत्व यदि कुरूपता-बोधक दोष है तो फिर उसे काव्य-मार्ग कैसे माना जा सकता है ?
और वास्तव में दण्डी ने गौडीय मार्ग के प्रसंग में जितने उदाहरण दिए हैं वे कुकाव्य के उदाहरण नहीं हैं । इस आक्षेप का उत्तर दिया जा सकता है: दण्डी ने गुण के विपर्यय को दोष नहीं माना है-व्युत्पन्नता, दीति और अत्युक्ति तो दोष हैं ही नहीं-शैथिल्य और वैषम्य को भी निरपेक्ष रूप से दोष नहीं माना जा सकता । वामन ने तो बन्ध-शैथिल्य को शब्द-गुण माना ही है। उनके उपरान्त इसी सत्य का उद्घाटन आनन्दवर्धन ने और भी स्पष्ट शब्दों में किया है । पद-रचना का कोई रूप-समस्त अथवा असमस्त पद, गाढ अथवा स्फुट बन्ध अपने आप में न काव्य का अपकर्षक है न उत्कर्षक : विषय और भाव के अनुसार ये दोनों ही गुण हो सकते हैं, और दोनों ही दोष । इसलिए श्लेषादि गुणों के विपर्यय-जिनकी स्थिति गौडीय मार्ग में मानी गई है-दोष-वाचक नहीं हैं, श्लेषादि के तुल्य उत्कर्षवाचक चाहे न हों।
उपयुक्त तर्फ दूसरे पाख्यान की क्लिष्ट कल्पना को अनावश्यक बना देता है । दण्डी ने निश्चय ही पैदर्भ मार्ग को श्रेष्ठ और गौड़ीय को निकृष्ट माना है। इसलिए श्लोक के उत्तरार्ध का यह अर्थ कि गौड़ मार्ग के मूल तत्व वैदर्भ के मूल तत्वों से केवल भिन्न होते हैं क्लिष्टान्धय होने के अतिरिक्त प्रसंग-विरुद्ध भी है।
तीसरा अख्यान भी हमारे उपयुक्त विवेचन के प्रकाश में अनावश्यक हो जाता है : जब वैपरीस्य दोष नहीं है तो अन्यथात्व की कल्पना ही क्यों की जाए ? वैसे भी दण्डी के व्युत्पन्न प्रादि विपर्ययों में वैपरीत्य के साथ साथ चाहे अन्यथात्व भी भले ही हो, परन्तु शैथिल्य और वैषम्य के विषय में तो ऐसी कोई शंका नहीं हो सकती-वे तो निश्चय ही पूर्णतया विपरीत रूप हैं। इसलिए विपर्यय का अर्थ अन्यथात्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योकि दण्डी के पूर्वोद्धृत विपर्ययों में से किसी में भी वैपरीत्य का अभाव नहीं है :-व्युत्पन्न आदि में प्रांशिक वैपरीत्य है और शैथिल्य आदि मे पूर्ण।
निष्कर्ष यह है कि 'एषां से दण्डी का श्राशय दश गुणों का और 'विपर्यय से चैपरीत्य का ही है । दण्डी ने गौड मार्ग को हीनतर मानते हुए भी
(३६)