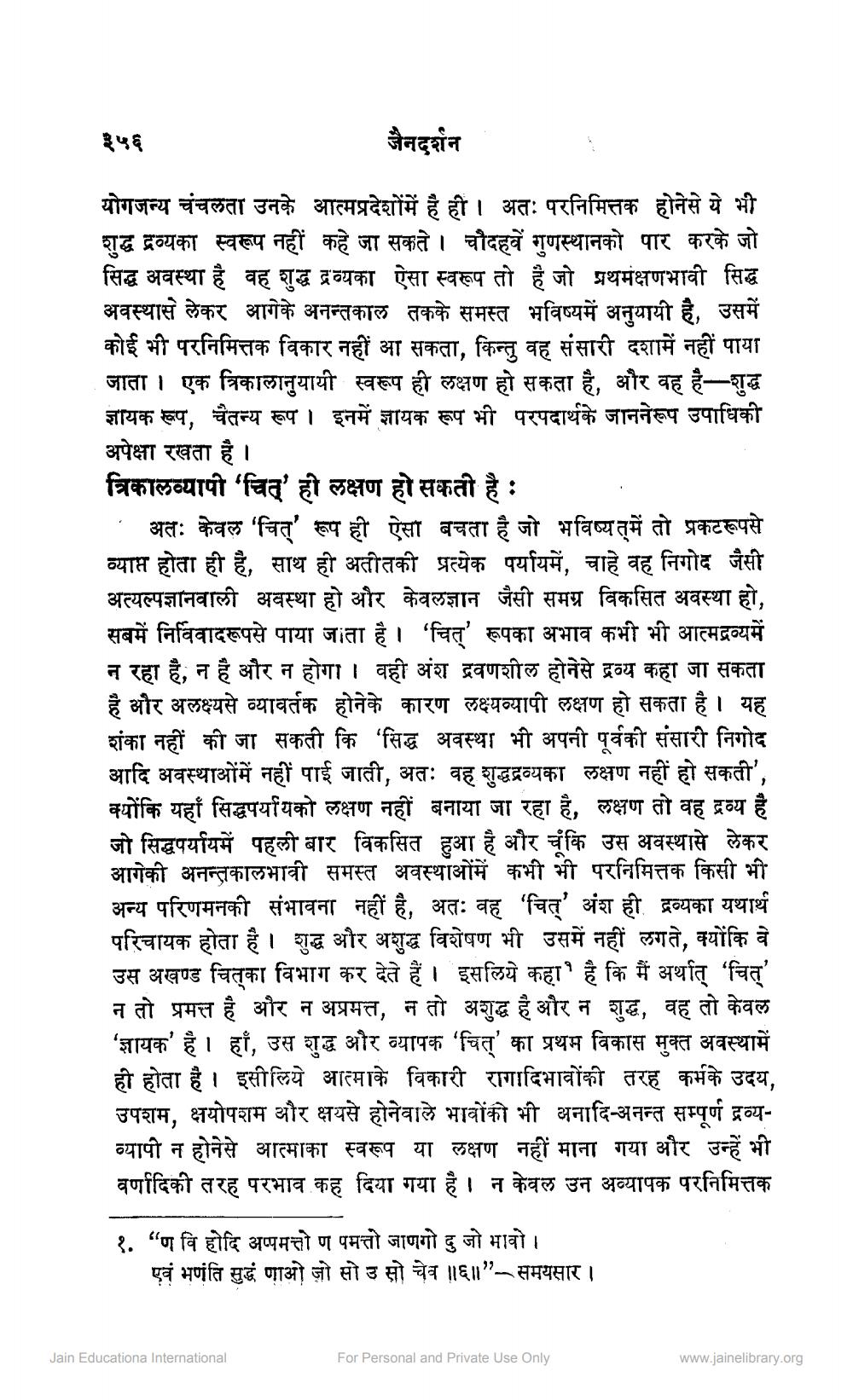________________ 356 जैनदर्शन योगजन्य चंचलता उनके आत्मप्रदेशोंमें है ही। अतः परनिमित्तक होनेसे ये भी शुद्ध द्रव्यका स्वरूप नहीं कहे जा सकते। चौदहवें गणस्थानको पार करके जो सिद्ध अवस्था है वह शुद्ध द्रव्यका ऐसा स्वरूप तो है जो प्रथमक्षणभावी सिद्ध अवस्थासे लेकर आगेके अनन्तकाल तकके समस्त भविष्यमें अनुयायी है, उसमें कोई भी परनिमित्तक विकार नहीं आ सकता, किन्तु वह संसारी दशामें नहीं पाया जाता। एक त्रिकालानुयायी स्वरूप ही लक्षण हो सकता है, और वह है-शुद्ध ज्ञायक रूप, चैतन्य रूप। इनमें ज्ञायक रूप भी परपदार्थके जाननेरूप उपाधिकी अपेक्षा रखता है। त्रिकालव्यापी 'चित्' ही लक्षण हो सकती है : - अतः केवल 'चित्' रूप ही ऐसा बचता है जो भविष्य त्में तो प्रकटरूपसे व्याप्त होता ही है, साथ ही अतीतकी प्रत्येक पर्यायमें, चाहे वह निगोद जैसी अत्यल्पज्ञानवाली अवस्था हो और केवलज्ञान जैसी समग्र विकसित अवस्था हो, सबमें निर्विवादरूपसे पाया जाता है। 'चित्' रूपका अभाव कभी भी आत्मद्रव्यमें न रहा है, न है और न होगा। वही अंश द्रवणशील होनेसे द्रव्य कहा जा सकता है और अलक्ष्यसे व्यावर्तक होनेके कारण लक्ष्यव्यापी लक्षण हो सकता है। यह शंका नहीं की जा सकती कि 'सिद्ध अवस्था भी अपनी पूर्वकी संसारी निगोद आदि अवस्थाओंमें नहीं पाई जाती, अतः वह शुद्धद्रव्यका लक्षण नहीं हो सकती', क्योंकि यहाँ सिद्धपर्यायको लक्षण नहीं बनाया जा रहा है, लक्षण तो वह द्रव्य है जो सिद्धपर्यायमें पहली बार विकसित हुआ है और चूंकि उस अवस्थासे लेकर आगेकी अनन्तकालभावी समस्त अवस्थाओंमें कभी भी परनिमित्तक किसी भी अन्य परिणमनकी संभावना नहीं है, अतः वह 'चित्' अंश ही द्रव्यका यथार्थ परिचायक होता है। शुद्ध और अशुद्ध विशेषण भी उसमें नहीं लगते, क्योंकि वे उस अखण्ड चित्का विभाग कर देते हैं। इसलिये कहा है कि मैं अर्थात् 'चित्' न तो प्रमत्त है और न अप्रमत्त, न तो अशुद्ध है और न शुद्ध, वह तो केवल 'ज्ञायक' है। हाँ, उस शुद्ध और व्यापक 'चित्' का प्रथम विकास मुक्त अवस्थामें ही होता है। इसीलिये आत्माके विकारी रागादिभावोंकी तरह कर्मके उदय, उपशम, क्षयोपशम और क्षयसे होनेवाले भावोंको भी अनादि-अनन्त सम्पूर्ण द्रव्यव्यापी न होनेसे आत्माका स्वरूप या लक्षण नहीं माना गया और उन्हें भी वर्णादिकी तरह परभाव कह दिया गया है। न केवल उन अव्यापक परनिमित्तक 1. "ण वि होदि अप्पमत्तो ण पमत्तो जाणगो दु जो भावो। एवं भणंति सुद्धं णाओ जो सो उ सो चेव // 6 // "- समयसार / Jain Educationa International For Personal and Private Use Only www.jainelibrary.org