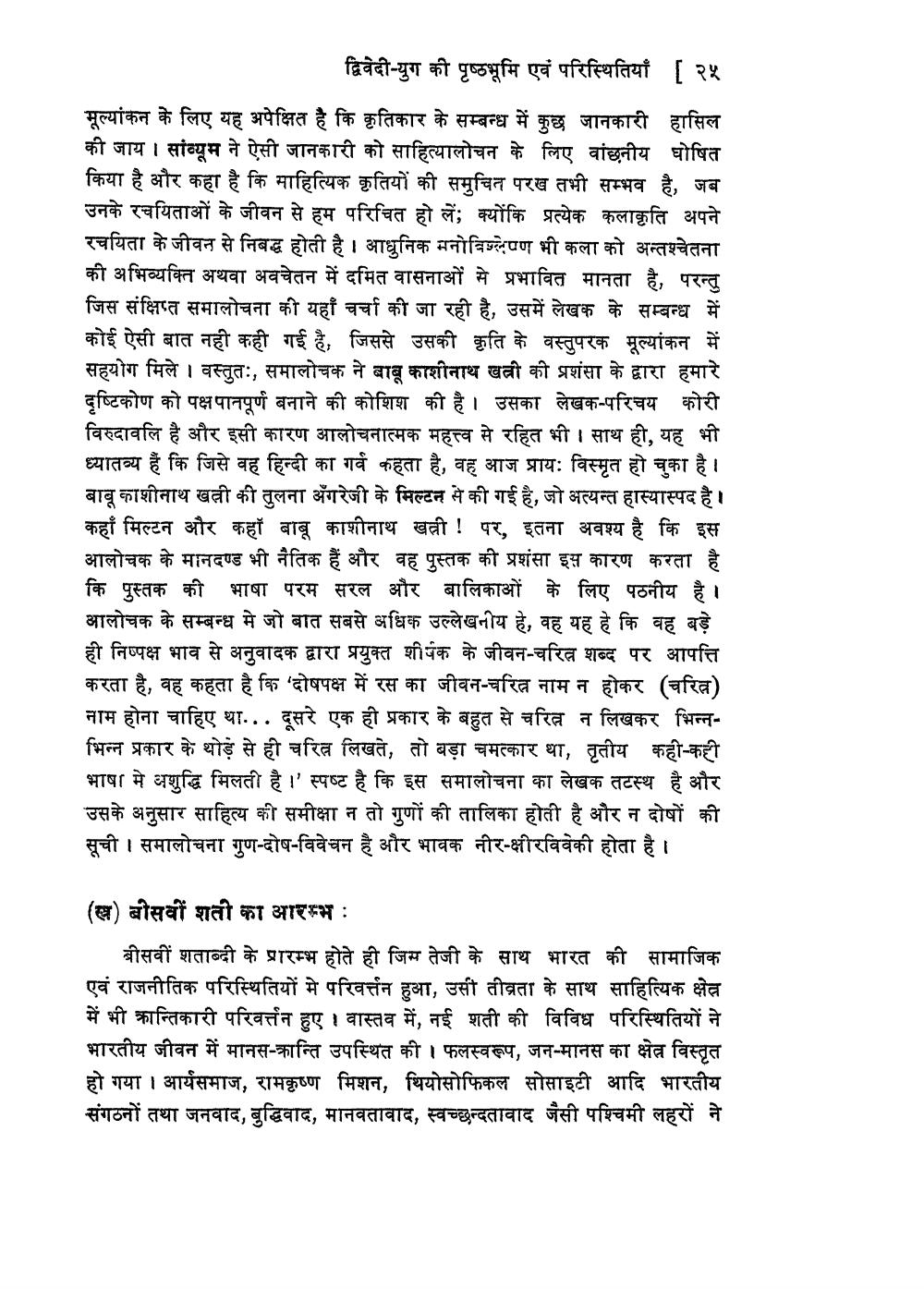________________
द्विवेदी-युग की पृष्ठभूमि एवं परिस्थितियाँ [ २५ मूल्यांकन के लिए यह अपेक्षित है कि कृतिकार के सम्बन्ध में कुछ जानकारी हासिल की जाय । सांव्यूम ने ऐसी जानकारी को साहित्यालोचन के लिए वांछनीय घोषित किया है और कहा है कि माहित्यिक कृतियों की समुचित परख तभी सम्भव है, जब उनके रचयिताओं के जीवन से हम परिचित हो लें; क्योंकि प्रत्येक कलाकृति अपने रचयिता के जीवन से निबद्ध होती है । आधुनिक मनोविश्लेपण भी कला को अन्तश्चेतना की अभिव्यक्ति अथवा अवचेतन में दमित वासनाओं से प्रभावित मानता है, परन्तु जिस संक्षिप्त समालोचना की यहाँ चर्चा की जा रही है, उसमें लेखक के सम्बन्ध में कोई ऐसी बात नही कही गई है, जिससे उसकी कृति के वस्तुपरक मूल्यांकन में सहयोग मिले । वस्तुतः, समालोचक ने बाबू काशीनाथ खत्री की प्रशंसा के द्वारा हमारे दृष्टिकोण को पक्षपातपूर्ण बनाने की कोशिश की है। उसका लेखक-परिचय कोरी विरुदावलि है और इसी कारण आलोचनात्मक महत्त्व से रहित भी। साथ ही, यह भी ध्यातव्य है कि जिसे वह हिन्दी का गर्व कहता है, वह आज प्रायः विस्मृत हो चुका है। बाबू काशीनाथ खत्री की तुलना अँगरेजी के मिल्टन से की गई है, जो अत्यन्त हास्यास्पद है। कहाँ मिल्टन और कहाँ बाबू काशीनाथ खत्री ! पर, इतना अवश्य है कि इस आलोचक के मानदण्ड भी नैतिक हैं और वह पुस्तक की प्रशंसा इस कारण करता है कि पुस्तक की भाषा परम सरल और बालिकाओं के लिए पठनीय है। आलोचक के सम्बन्ध मे जो बात सबसे अधिक उल्लेखनीय है, वह यह है कि वह बड़े ही निष्पक्ष भाव से अनुवादक द्वारा प्रयुक्त शीर्षक के जीवन-चरित्र शब्द पर आपत्ति करता है, वह कहता है कि 'दोषपक्ष में रस का जीवन-चरित्र नाम न होकर (चरित्र) नाम होना चाहिए था... दूसरे एक ही प्रकार के बहुत से चरित्र न लिखकर भिन्नभिन्न प्रकार के थोड़े से ही चरित्र लिखते, तो बड़ा चमत्कार था, तृतीय कही-कही भाषा मे अशुद्धि मिलती है।' स्पष्ट है कि इस समालोचना का लेखक तटस्थ है और उसके अनुसार साहित्य की समीक्षा न तो गुणों की तालिका होती है और न दोषों की सूची । समालोचना गुण-दोष-विवेचन है और भावक नीर-क्षीरविवेकी होता है।
(ख) बीसवीं शती का आरम्भ :
बीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ होते ही जिस तेजी के साथ भारत की सामाजिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ, उसी तीव्रता के साथ साहित्यिक क्षेत्र में भी क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए। वास्तव में, नई शती की विविध परिस्थितियों ने भारतीय जीवन में मानस-क्रान्ति उपस्थित की। फलस्वरूप, जन-मानस का क्षेत्र विस्तृत हो गया । आर्यसमाज, रामकृष्ण मिशन, थियोसोफिकल सोसाइटी आदि भारतीय संगठनों तथा जनवाद, बुद्धिवाद, मानवतावाद, स्वच्छन्दतावाद जैसी पश्चिमी लहरों ने