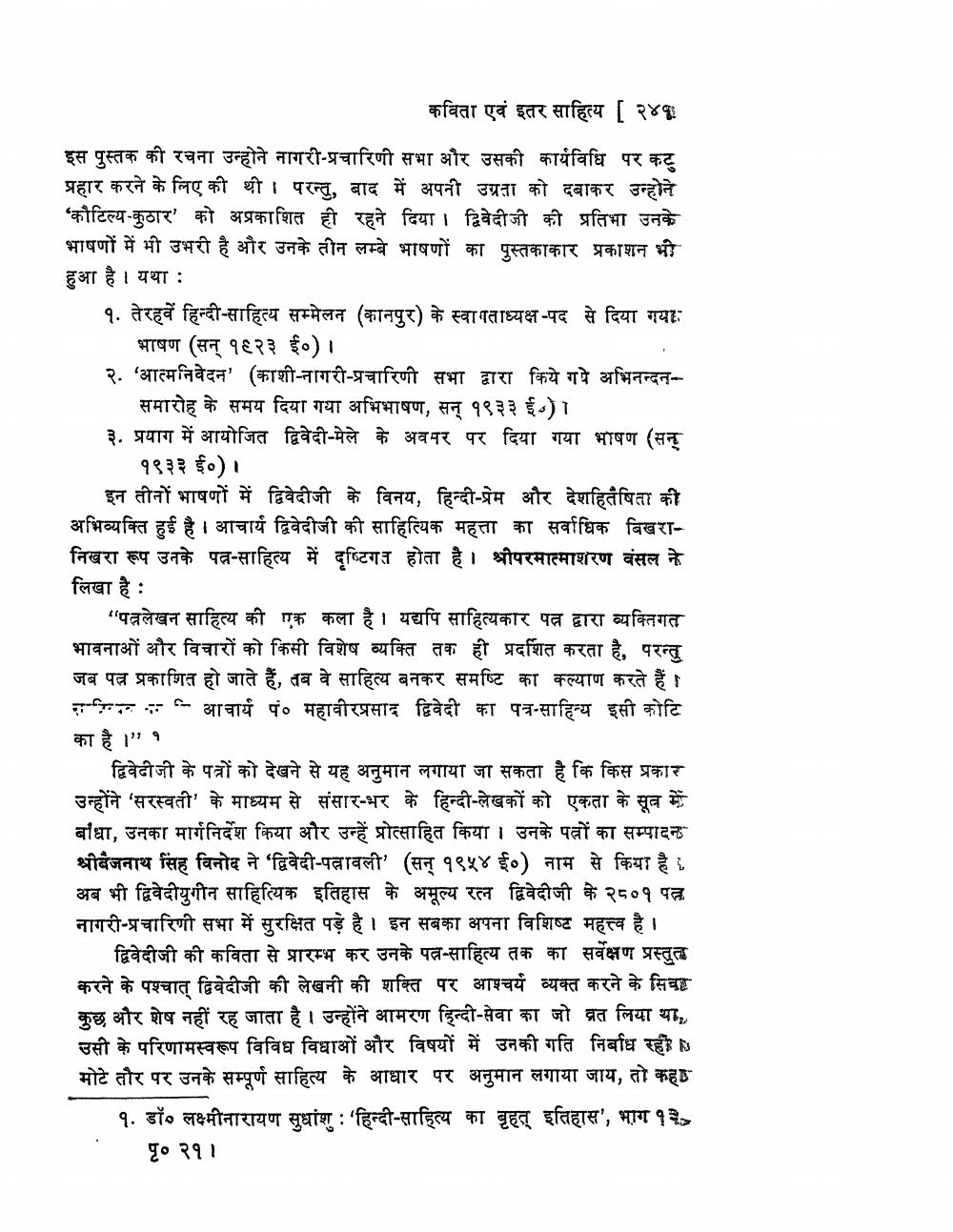________________
कविता एवं इतर साहित्य [२४१
इस पुस्तक की रचना उन्होने नागरी-प्रचारिणी सभा और उसकी कार्यविधि पर कटु प्रहार करने के लिए की थी। परन्तु, बाद में अपनी उग्रता को दबाकर उन्होने 'कौटिल्य-कुठार' को अप्रकाशित ही रहने दिया। द्विवेदीजी की प्रतिभा उनके भाषणों में भी उभरी है और उनके तीन लम्बे भाषणों का पुस्तकाकार प्रकाशन भी हुआ है। यथा :
१. तेरहवें हिन्दी-साहित्य सम्मेलन (कानपुर) के स्वागताध्यक्ष-पद से दिया गया __भाषण (सन् १९२३ ई०)। २. 'आत्मनिवेदन' (काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा द्वारा किये गये अभिनन्दन--
समारोह के समय दिया गया अभिभाषण, सन् १९३३ ई.)। ३. प्रयाग में आयोजित द्विवेदी-मेले के अवसर पर दिया गया भाषण (सन्
इन तीनों भाषणों में द्विवेदीजी के विनय, हिन्दी-प्रेम और देशहितैषिता की अभिव्यक्ति हुई है। आचार्य द्विवेदीजी की साहित्यिक महत्ता का सर्वाधिक बिखरानिखरा रूप उनके पत्र-साहित्य में दृष्टिगत होता है। श्रीपरमात्माशरण बंसल ने लिखा है :
"पत्रलेखन साहित्य की एक कला है। यद्यपि साहित्यकार पत्र द्वारा व्यक्तिगत भावनाओं और विचारों को किसी विशेष व्यक्ति तक ही प्रदर्शित करता है, परन्तु जब पन प्रकाशित हो जाते हैं, तब वे साहित्य बनकर समष्टि का कल्याण करते हैं। म न - आचार्य पं. महावीरप्रसाद द्विवेदी का पत्र-साहित्य इसी कोटि का है।"
द्विवेदीजी के पत्रों को देखने से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि किस प्रकार उन्होंने 'सरस्वती' के माध्यम से संसार-भर के हिन्दी-लेखकों को एकता के सूत्र में बांधा, उनका मार्गनिर्देश किया और उन्हें प्रोत्साहित किया। उनके पत्रों का सम्पादन श्रीबैजनाथ सिंह विनोद ने 'द्विवेदी-पत्रावली' (सन् १९५४ ई०) नाम से किया है। अब भी द्विवेदीयुगीन साहित्यिक इतिहास के अमूल्य रत्न द्विवेदीजी के २८०१ पत्र नागरी-प्रचारिणी सभा में सुरक्षित पड़े है। इन सबका अपना विशिष्ट महत्त्व है।
द्विवेदीजी की कविता से प्रारम्भ कर उनके पत्र-साहित्य तक का सर्वेक्षण प्रस्तुत करने के पश्चात् द्विवेदीजी की लेखनी की शक्ति पर आश्चर्य व्यक्त करने के सिवह कुछ और शेष नहीं रह जाता है। उन्होंने आमरण हिन्दी-सेवा का जो व्रत लिया था,, उसी के परिणामस्वरूप विविध विधाओं और विषयों में उनकी गति निर्बाध रही। मोटे तौर पर उनके सम्पूर्ण साहित्य के आधार पर अनुमान लगाया जाय, तो कहा १. डॉ. लक्ष्मीनारायण सुधांशु : 'हिन्दी-साहित्य का बृहत् इतिहास', भाग १३,
पृ० २१।