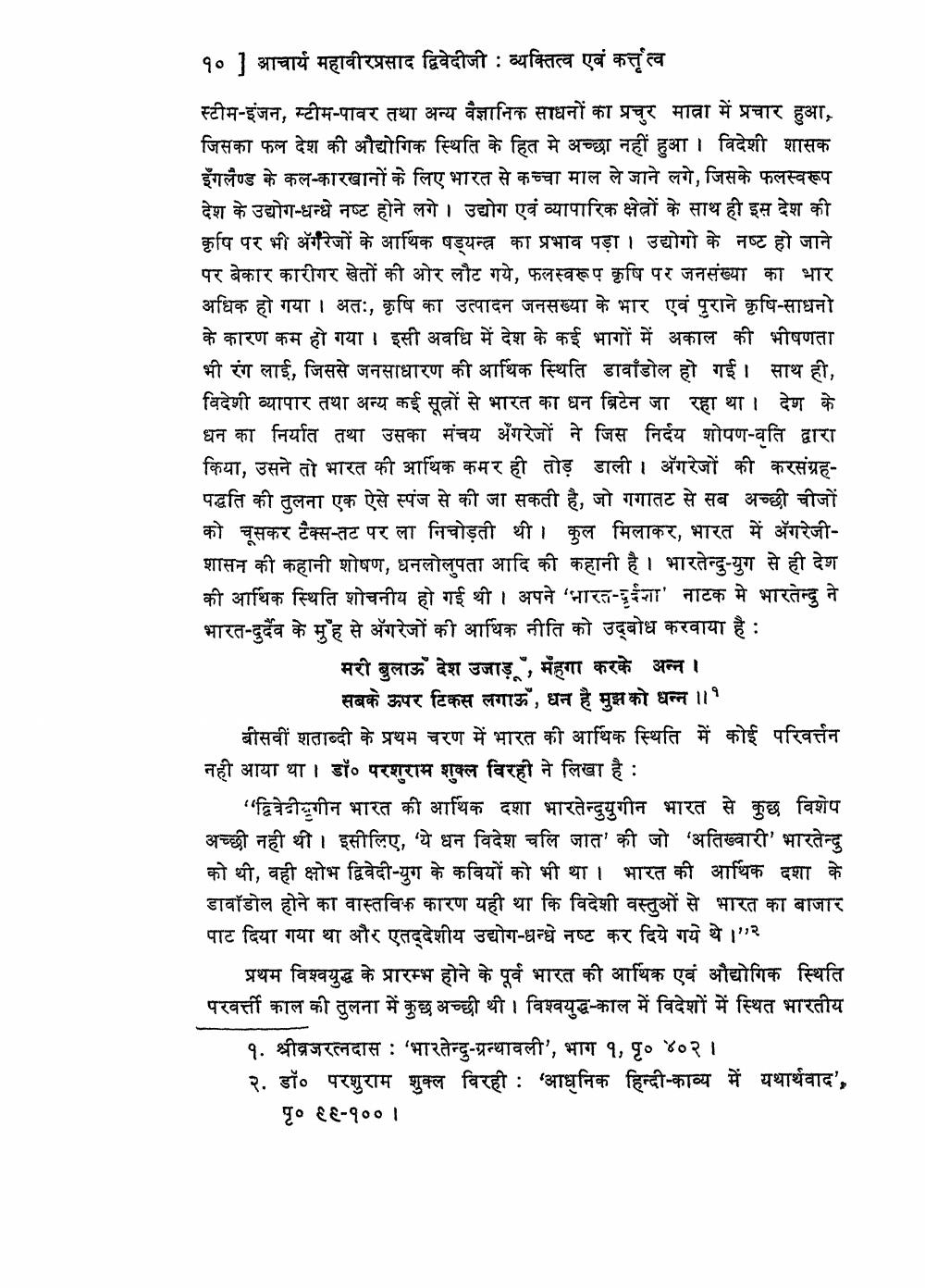________________
१० ] आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदीजी : व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व स्टीम-इंजन, स्टीम-पावर तथा अन्य वैज्ञानिक साधनों का प्रचुर मात्रा में प्रचार हुआ, जिसका फल देश की औद्योगिक स्थिति के हित मे अच्छा नहीं हुआ। विदेशी शासक इंगलैण्ड के कल-कारखानों के लिए भारत से कच्चा माल ले जाने लगे, जिसके फलस्वरूप देश के उद्योग-धन्धे नष्ट होने लगे। उद्योग एवं व्यापारिक क्षेत्रों के साथ ही इस देश की कृषि पर भी अगरेजों के आर्थिक षड्यन्त्र का प्रभाव पड़ा। उद्योगो के नष्ट हो जाने पर बेकार कारीगर खेतों की ओर लौट गये, फलस्वरूप कृषि पर जनसंख्या का भार अधिक हो गया। अतः, कृषि का उत्पादन जनसख्या के भार एवं पुराने कृषि-साधनो के कारण कम हो गया। इसी अवधि में देश के कई भागों में अकाल की भीषणता भी रंग लाई, जिससे जनसाधारण की आर्थिक स्थिति डावाँडोल हो गई। साथ ही, विदेशी व्यापार तथा अन्य कई सूत्रों से भारत का धन ब्रिटेन जा रहा था। देश के धन का निर्यात तथा उसका संचय अँगरेजों ने जिस निर्दय शोपण-वति द्वारा किया, उसने तो भारत की आर्थिक कमर ही तोड़ डाली। अगरेजों की करसंग्रहपद्धति की तुलना एक ऐसे स्पंज से की जा सकती है, जो गगातट से सब अच्छी चीजों को चूसकर टैक्स-तट पर ला निचोड़ती थी। कुल मिलाकर, भारत में अँगरेजीशासन की कहानी शोषण, धनलोलुपता आदि की कहानी है। भारतेन्दु-युग से ही देश की आर्थिक स्थिति शोचनीय हो गई थी। अपने 'भारत-बुर्दशा' नाटक मे भारतेन्दु ने भारत-दुर्दैव के मुह से अंगरेजों की आर्थिक नीति को उद्बोध करवाया है :
मरी बुलाऊँ देश उजाड़', महगा करके अन्न ।
सबके ऊपर टिकस लगाऊँ, धन है मुझ को धन्न ॥१ बीसवीं शताब्दी के प्रथम चरण में भारत की आर्थिक स्थिति में कोई परिवर्तन नही आया था। डॉ० परशुराम शुक्ल विरही ने लिखा है : __ "विवेढीबुगीन भारत की आर्थिक दशा भारतेन्दुयुगीन भारत से कुछ विशेष अच्छी नही थी। इसीलिए, 'ये धन विदेश चलि जात' की जो 'अतिख्वारी' भारतेन्दु को थी, वही क्षोभ द्विवेदी-युग के कवियों को भी था। भारत की आर्थिक दशा के डावॉडोल होने का वास्तविक कारण यही था कि विदेशी वस्तुओं से भारत का बाजार पाट दिया गया था और एतद्देशीय उद्योग-धन्धे नष्ट कर दिये गये थे।"२
प्रथम विश्वयुद्ध के प्रारम्भ होने के पूर्व भारत की आर्थिक एवं औद्योगिक स्थिति परवर्ती काल की तुलना में कुछ अच्छी थी। विश्वयुद्ध-काल में विदेशों में स्थित भारतीय
१. श्रीब्रजरत्नदास : 'भारतेन्दु-ग्रन्थावली', भाग १, पृ० ४०२।। २. डॉ० परशुराम शुक्ल विरही : 'आधुनिक हिन्दी-काव्य में यथार्थवाद',
पृ० ६६-१००।