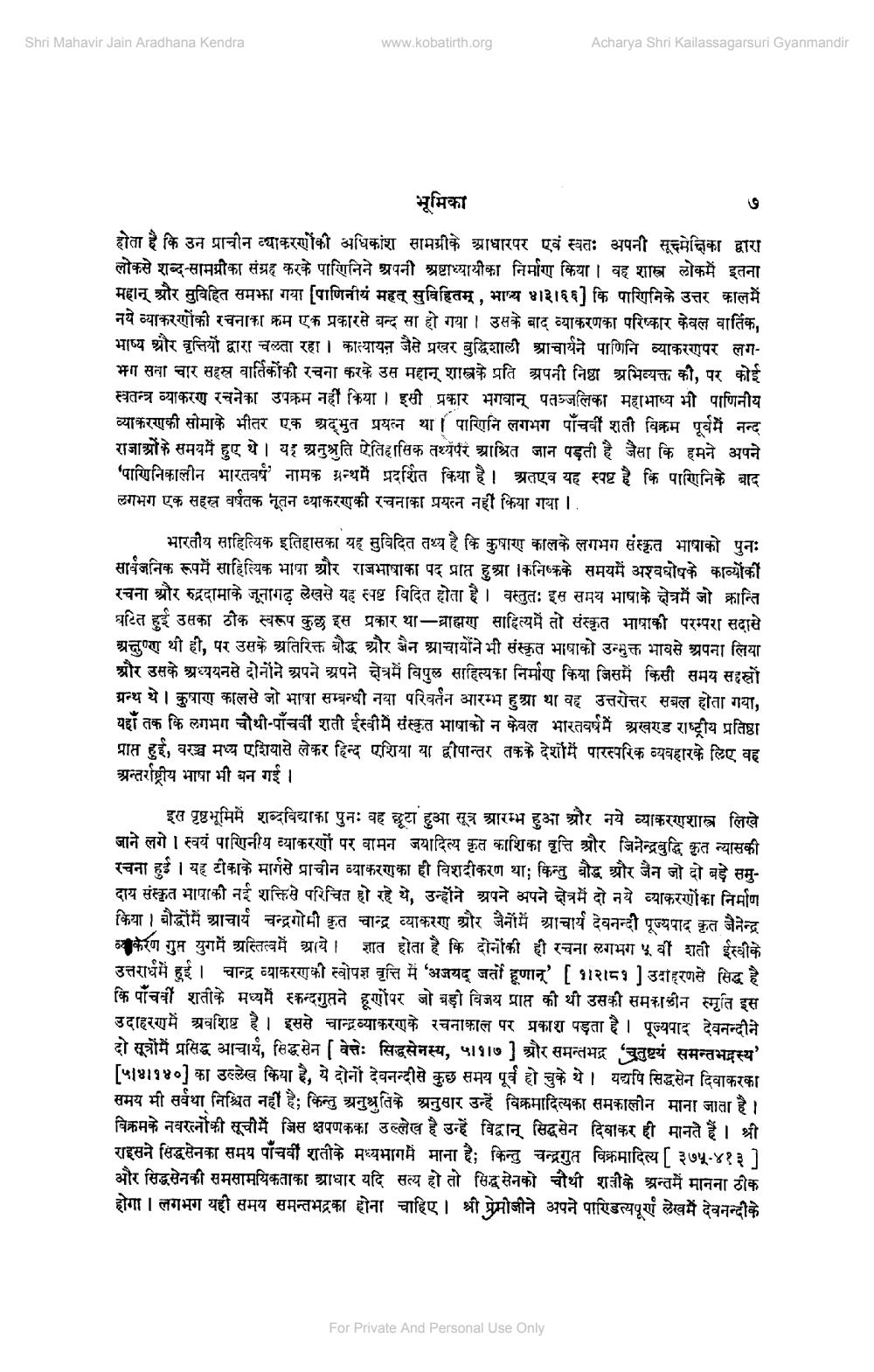________________
Shri Mahavir Jain Aradhana Kendra
www.kobatirth.org
Acharya Shri Kailassagarsuri Gyanmandir
भूमिका
होता है कि उन प्राचीन व्याकरणोंकी अधिकांश सामग्रीके आधारपर एवं स्वतः अपनी सूक्ष्मेक्षिका द्वारा लोकसे शब्द-सामग्रीका संग्रह करके पाणिनिने अपनी अष्टाध्यायीका निर्माण किया। वह शास्त्र लोकमें इतना महान् और सुविहित समझा गया [पाणिनीयं महत् सुविहितम् , भाष्य ४।३।६६] कि पाणिनिके उत्तर कालमें नये व्याकरणोंकी रचनाका क्रम एक प्रकारसे बन्द सा हो गया। उसके बाद व्याकरणका परिष्कार केवल वार्तिक, भाष्य और वृत्तियों द्वारा चलता रहा। कात्यायन जैसे प्रखर बुद्धिशाली प्राचार्यने पाणिनि व्याकरणपर लगमग सवा चार सहस्र वार्तिकोंकी रचना करके उस महान् शास्त्र के प्रति अपनी निष्ठा अभिव्यक्त की, पर कोई स्वतन्त्र व्याकरण रचनेका उपक्रम नहीं किया। इसी प्रकार भगवान् पतञ्जलिका महाभाष्य भी पाणिनीय व्याकरणकी सोमाके भीतर एक अद्भुत प्रयत्न था। पाणिनि लगभग पाँचवीं शती विक्रम पूर्वमें नन्द राजाओं के समयमै हुए थे। यह अनुश्रुति ऐतिहासिक तथ्यपर आश्रित जान पड़ती है जैसा कि हमने अपने 'पाणिनिकालीन भारतवर्ष' नामक ग्रन्थमें प्रदर्शित किया है। अतएव यह स्पष्ट है कि पाणिनिके बाद लगभग एक सहस्र वर्षतक नूतन व्याकरणकी रचनाका प्रयत्न नहीं किया गया ।
भारतीय साहित्यिक इतिहासका यह सुविदित तथ्य है कि कुषाण कालके लगभग संस्कृत भाषाको पुनः सार्वजनिक रूपमें साहित्यिक भाषा और राजभाषाका पद प्राप्त हुआ किनिष्कके समयमै अश्वघोषके काव्योंकी रचना और रुद्रदामाके जूनागढ़ लेखसे यह स्पष्ट विदित होता है। वस्तुतः इस समय भाषाके क्षेत्रमें जो क्रान्ति घटित हुई उसका ठीक स्वरूप कुछ इस प्रकार था-ब्राह्मण साहित्य में तो संस्कृत भाषाकी परम्परा सदासे अक्षुण्ण थी ही, पर उसके अतिरिक्त बौद्ध और जैन श्राचार्योंने भी संस्कृत भाषाको उन्मुक्त भावसे अपना लिया
और उसके अध्ययनसे दोनोने अपने अपने क्षेत्रमें विपुल साहित्यका निर्माण किया जिसमें किसी समय सहस्रों ग्रन्थ थे। कुषाण कालसे जो भाषा सम्बन्धी नया परिवर्तन आरम्भ हुआ था वह उत्तरोत्तर सबल होता गया, यहाँ तक कि लगभग चौथी-पाँचवीं शती ईस्वी में संस्कृत भाषाको न केवल भारतवर्ष में अखण्ड राष्ट्रीय प्रतिष्ठा प्राप्त हुई, वरञ्च मध्य एशियासे लेकर हिन्द एशिया या द्वीपान्तर तकके देशोंमें पारस्परिक व्यवहार के लिए वह अन्तर्राष्ट्रीय भाषा भी बन गई।
इस पृष्ठभूमिमें शब्दविद्याका पुनः वह छुटा हुआ सूत्र प्रारम्भ हुआ और नये व्याकरणशास्त्र लिखे जाने लगे। स्वयं पाणिनीय व्याकरणों पर वामन जयादित्य कृत काशिका वृत्ति और जिनेन्द्रबद्धि कृत न्यासकी रचना हुई । यह टीकाके मार्गसे प्राचीन व्याकरणका ही विशदीकरण था; किन्तु बौद्ध और जैन जो दो बड़े समुदाय संस्कृत भाषाकी नई शक्ति से परिचित हो रहे थे, उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में दो नये व्याकरणोंका निर्माण किया। बौद्धोंमें प्राचार्य चन्द्रगोमी कृत चान्द्र व्याकरण और जैनों में प्राचार्य देवनन्दी पूज्यपाद कृत जैनेन्द्र व्याकरण गुप्त युगमैं अस्तित्वमें आये। ज्ञात होता है कि दोनोंकी ही रचना लगभग ५ वीं शती ईस्वीके उत्तरार्धमें हुई। चान्द्र व्याकरणकी त्वोपज्ञ वृत्ति में 'अजयद् जर्ती हूणान्' [ १॥२॥८१ ] उदाहरणसे सिद्ध है कि पाँचवीं शतीके मध्य में स्कन्दगुप्तने हणोंपर जो बड़ी विजय प्राप्त की थी उसकी समकालीन स्मृति इस उदाहरणमें अवशिष्ट है। इससे चान्द्र व्याकरणके रचनाकाल पर प्रकाश पड़ता है। पूज्यपाद देवनन्दीने दो सूत्रोंमें प्रसिद्ध आचार्य, सिद्धसेन [ वेत्तेः सिद्धसेनस्य, ५।१७ ] और समन्तभद्र 'चतुष्टयं समन्तभद्रस्य' [५/१४०] का उल्लेख किया है, ये दोनों देवनन्दीसे कुछ समय पूर्व हो चुके थे। यद्यपि सिद्धसेन दिवाकरका समय भी सर्वथा निश्चित नहीं है; किन्तु अनुश्रतिके अनुसार उन्हें विक्रमादित्यका समकालीन माना जाता है। विक्रमके नवरत्नोंकी सूची में जिस क्षपणकका उल्लेख है उन्हें विद्वान् सिद्धसेन दिवाकर ही मानते हैं। श्री राइसने सिद्धसेनका समय पाँचवीं शतीके मध्यभागमैं माना है। किन्तु चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य [ ३७५.४१३ 1
और सिद्धसेनकी समसामयिकताका आधार यदि सत्य हो तो सिद्धसेनको चौथी शतीके अन्तमें मानना ठीक होगा । लगभग यही समय समन्तभद्रका होना चाहिए। श्री प्रेमीजीने अपने पाण्डित्यपूर्ण लेखमें देवनन्दीके
For Private And Personal Use Only