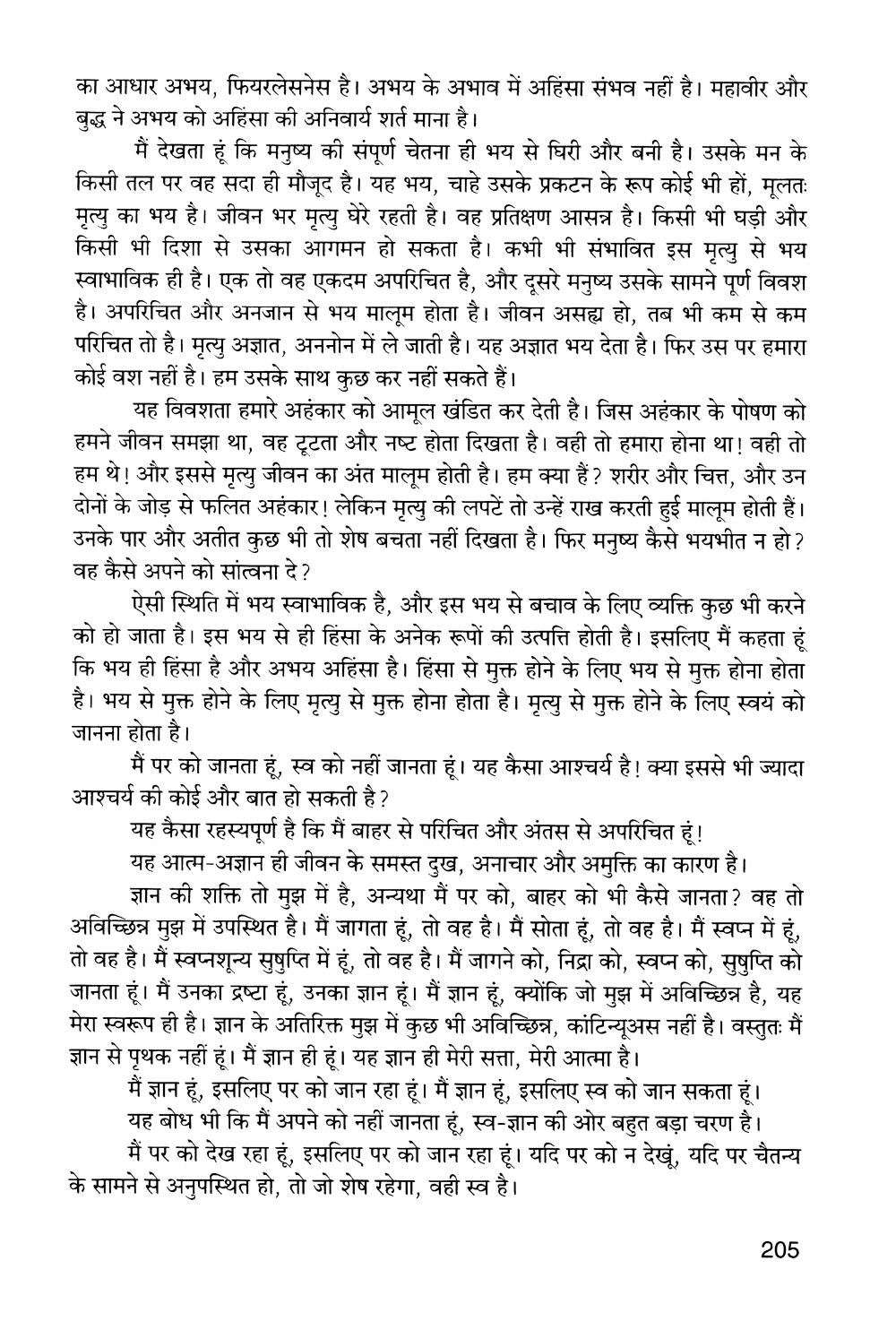________________
का आधार अभय, फियरलेसनेस है। अभय के अभाव में अहिंसा संभव नहीं है। महावीर और बुद्ध ने अभय को अहिंसा की अनिवार्य शर्त माना है।
मैं देखता हूं कि मनुष्य की संपूर्ण चेतना ही भय से घिरी और बनी है। उसके मन के किसी तल पर वह सदा ही मौजूद है। यह भय, चाहे उसके प्रकटन के रूप कोई भी हों, मूलतः मृत्यु का भय है। जीवन भर मृत्यु घेरे रहती है। वह प्रतिक्षण आसन्न है। किसी भी घड़ी और किसी भी दिशा से उसका आगमन हो सकता है। कभी भी संभावित इस मृत्यु से भय स्वाभाविक ही है। एक तो वह एकदम अपरिचित है, और दूसरे मनुष्य उसके सामने पूर्ण विवश है। अपरिचित और अनजान से भय मालूम होता है। जीवन असह्य हो, तब भी कम से कम परिचित तो है। मृत्यु अज्ञात, अननोन में ले जाती है। यह अज्ञात भय देता है। फिर उस पर हमारा कोई वश नहीं है। हम उसके साथ कुछ कर नहीं सकते हैं।
यह विवशता हमारे अहंकार को आमूल खंडित कर देती है। जिस अहंकार के पोषण को हमने जीवन समझा था, वह टूटता और नष्ट होता दिखता है। वही तो हमारा होना था। वही तो हम थे! और इससे मृत्यु जीवन का अंत मालूम होती है। हम क्या हैं? शरीर और चित्त, और उन दोनों के जोड़ से फलित अहंकार! लेकिन मृत्यु की लपटें तो उन्हें राख करती हई मालम होती हैं। उनके पार और अतीत कुछ भी तो शेष बचता नहीं दिखता है। फिर मनुष्य कैसे भयभीत न हो? वह कैसे अपने को सांत्वना दे?
ऐसी स्थिति में भय स्वाभाविक है, और इस भय से बचाव के लिए व्यक्ति कुछ भी करने को हो जाता है। इस भय से ही हिंसा के अनेक रूपों की उत्पत्ति होती है। इसलिए मैं कहता हूं कि भय ही हिंसा है और अभय अहिंसा है। हिंसा से मुक्त होने के लिए भय से मुक्त होना होता है। भय से मुक्त होने के लिए मृत्यु से मुक्त होना होता है। मृत्यु से मुक्त होने के लिए स्वयं को जानना होता है।
मैं पर को जानता हूं, स्व को नहीं जानता हूं। यह कैसा आश्चर्य है! क्या इससे भी ज्यादा आश्चर्य की कोई और बात हो सकती है?
यह कैसा रहस्यपूर्ण है कि मैं बाहर से परिचित और अंतस से अपरिचित हूं! यह आत्म-अज्ञान ही जीवन के समस्त दुख, अनाचार और अमुक्ति का कारण है।
ज्ञान की शक्ति तो मुझ में है, अन्यथा मैं पर को, बाहर को भी कैसे जानता? वह तो अविच्छिन्न मुझ में उपस्थित है। मैं जागता हूं, तो वह है। मैं सोता हूं, तो वह है। मैं स्वप्न में हूं, तो वह है। मैं स्वप्नशून्य सुषुप्ति में हूं, तो वह है। मैं जागने को, निद्रा को, स्वप्न को, सुषुप्ति को जानता हूं। मैं उनका द्रष्टा हूं, उनका ज्ञान हूं। मैं ज्ञान हूं, क्योंकि जो मुझ में अविच्छिन्न है, यह मेरा स्वरूप ही है। ज्ञान के अतिरिक्त मुझ में कुछ भी अविच्छिन्न, कांटिन्यूअस नहीं है। वस्तुतः मैं ज्ञान से पृथक नहीं हूं। मैं ज्ञान ही हूं। यह ज्ञान ही मेरी सत्ता, मेरी आत्मा है।
मैं ज्ञान हूं, इसलिए पर को जान रहा हूं। मैं ज्ञान हूं, इसलिए स्व को जान सकता हूं। यह बोध भी कि मैं अपने को नहीं जानता हूं, स्व-ज्ञान की ओर बहुत बड़ा चरण है।
मैं पर को देख रहा हूं, इसलिए पर को जान रहा हूं। यदि पर को न देखू, यदि पर चैतन्य के सामने से अनुपस्थित हो, तो जो शेष रहेगा, वही स्व है।
205