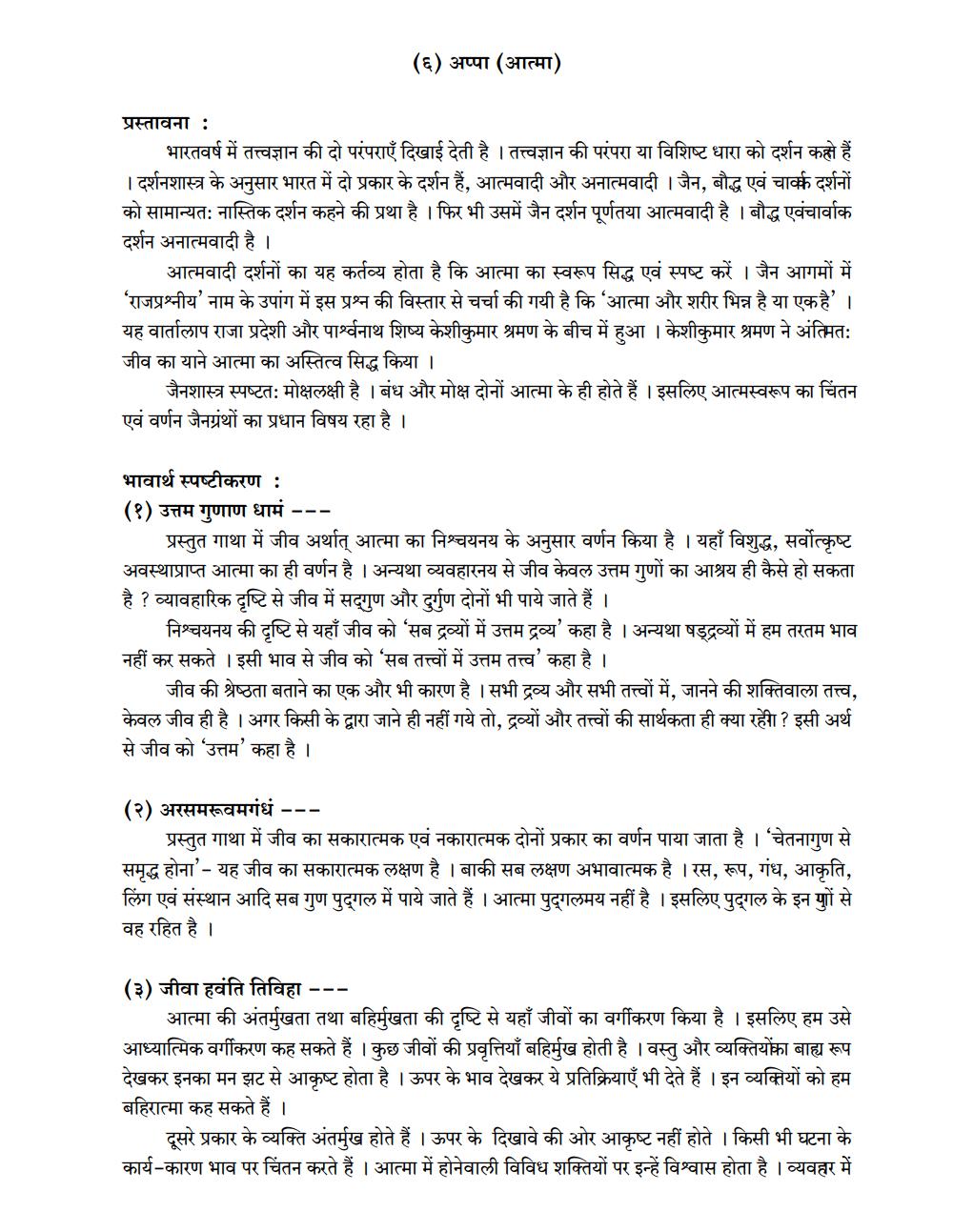________________
(६) अप्पा (आत्मा)
प्रस्तावना:
भारतवर्ष में तत्त्वज्ञान की दो परंपराएँ दिखाई देती है । तत्त्वज्ञान की परंपरा या विशिष्ट धारा को दर्शन कहते हैं । दर्शनशास्त्र के अनुसार भारत में दो प्रकार के दर्शन हैं, आत्मवादी और अनात्मवादी । जैन, बौद्ध एवं चार्क दर्शनों को सामान्यत: नास्तिक दर्शन कहने की प्रथा है । फिर भी उसमें जैन दर्शन पूर्णतया आत्मवादी है । बौद्ध एवंचार्वाक दर्शन अनात्मवादी है ।
आत्मवादी दर्शनों का यह कर्तव्य होता है कि आत्मा का स्वरूप सिद्ध एवं स्पष्ट करें । जैन आगमों में 'राजप्रश्नीय' नाम के उपांग में इस प्रश्न की विस्तार से चर्चा की गयी है कि आत्मा और शरीर भिन्न है या एकहै । यह वार्तालाप राजा प्रदेशी और पार्श्वनाथ शिष्य केशीकुमार श्रमण के बीच में हुआ । केशीकुमार श्रमण ने अंतिमतः जीव का याने आत्मा का अस्तित्व सिद्ध किया ।
जैनशास्त्र स्पष्टत: मोक्षलक्षी है । बंध और मोक्ष दोनों आत्मा के ही होते हैं । इसलिए आत्मस्वरूप का चिंतन एवं वर्णन जैनग्रंथों का प्रधान विषय रहा है ।
भावार्थ स्पष्टीकरण : (१) उत्तम गुणाण धामं ---
प्रस्तुत गाथा में जीव अर्थात् आत्मा का निश्चयनय के अनुसार वर्णन किया है । यहाँ विशुद्ध, सर्वोत्कृष्ट अवस्थाप्राप्त आत्मा का ही वर्णन है । अन्यथा व्यवहारनय से जीव केवल उत्तम गुणों का आश्रय ही कैसे हो सकता है ? व्यावहारिक दृष्टि से जीव में सद्गुण और दर्गण दोनों भी पाये जाते हैं।
निश्चयनय की दृष्टि से यहाँ जीव को ‘सब द्रव्यों में उत्तम द्रव्य' कहा है । अन्यथा षड्द्रव्यों में हम तरतम भाव नहीं कर सकते । इसी भाव से जीव को 'सब तत्त्वों में उत्तम तत्त्व' कहा है।
जीव की श्रेष्ठता बताने का एक और भी कारण है । सभी द्रव्य और सभी तत्त्वों में, जानने की शक्तिवाला तत्त्व, केवल जीव ही है । अगर किसी के द्वारा जाने ही नहीं गये तो, द्रव्यों और तत्त्वों की सार्थकता ही क्या रही? इसी अर्थ से जीव को 'उत्तम' कहा है ।।
(२) अरसमरूवमगंधं ---
प्रस्तुत गाथा में जीव का सकारात्मक एवं नकारात्मक दोनों प्रकार का वर्णन पाया जाता है । 'चेतनागुण से समृद्ध होना'- यह जीव का सकारात्मक लक्षण है । बाकी सब लक्षण अभावात्मक है । रस, रूप, गंध, आकृति, लिंग एवं संस्थान आदि सब गुण पुद्गल में पाये जाते हैं । आत्मा पुद्गलमय नहीं है । इसलिए पुद्गल के इन णों से वह रहित है।
(३) जीवा हवंति तिविहा ---
__ आत्मा की अंतर्मुखता तथा बहिर्मुखता की दृष्टि से यहाँ जीवों का वर्गीकरण किया है । इसलिए हम उसे आध्यात्मिक वर्गीकरण कह सकते हैं । कुछ जीवों की प्रवृत्तियाँ बहिर्मुख होती है । वस्तु और व्यक्तियोंका बाह्य रूप देखकर इनका मन झट से आकृष्ट होता है । ऊपर के भाव देखकर ये प्रतिक्रियाएँ भी देते हैं । इन व्यक्तियों को हम बहिरात्मा कह सकते हैं।
दूसरे प्रकार के व्यक्ति अंतर्मुख होते हैं । ऊपर के दिखावे की ओर आकृष्ट नहीं होते । किसी भी घटना के कार्य-कारण भाव पर चिंतन करते हैं । आत्मा में होनेवाली विविध शक्तियों पर इन्हें विश्वास होता है । व्यवहर में