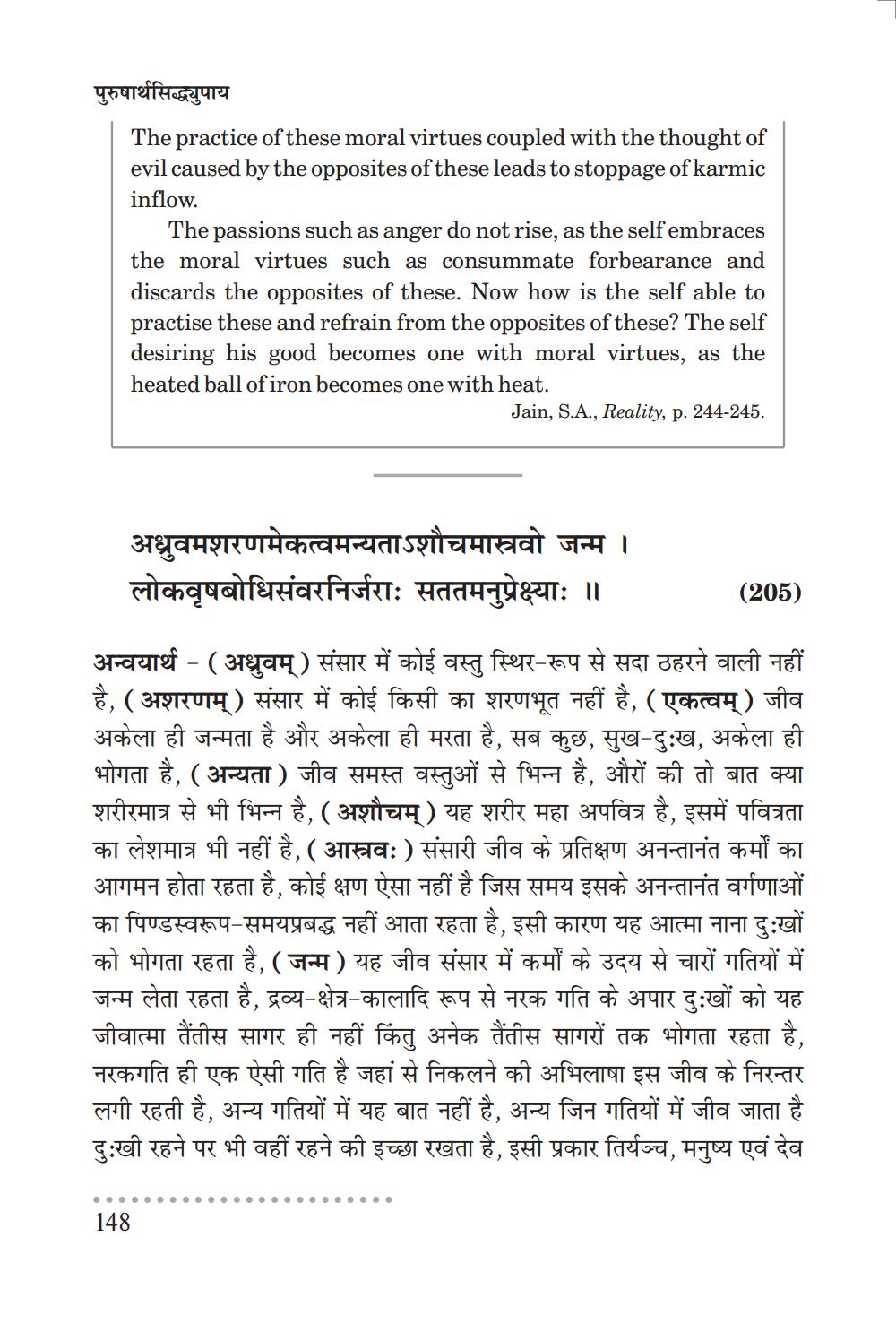________________
पुरुषार्थसिद्ध्युपाय
The practice of these moral virtues coupled with the thought of evil caused by the opposites of these leads to stoppage of karmic inflow.
The passions such as anger do not rise, as the self embraces the moral virtues such as consummate forbearance and discards the opposites of these. Now how is the self able to practise these and refrain from the opposites of these? The self desiring his good becomes one with moral virtues, as the heated ball of iron becomes one with heat.
Jain, S.A., Reality, p. 244-245.
अध्रुवमशरणमेकत्वमन्यताऽशौचमाञवो जन्म । लोकवृषबोधिसंवरनिर्जराः सततमनुप्रेक्ष्याः ॥
(205)
अन्वयार्थ - (अध्रुवम् ) संसार में कोई वस्तु स्थिर-रूप से सदा ठहरने वाली नहीं है, (अशरणम् ) संसार में कोई किसी का शरणभूत नहीं है, (एकत्वम् ) जीव अकेला ही जन्मता है और अकेला ही मरता है, सब कुछ, सुख-दु:ख, अकेला ही भोगता है, (अन्यता) जीव समस्त वस्तुओं से भिन्न है, औरों की तो बात क्या शरीरमात्र से भी भिन्न है, (अशौचम्) यह शरीर महा अपवित्र है, इसमें पवित्रता का लेशमात्र भी नहीं है, (आस्त्रवः) संसारी जीव के प्रतिक्षण अनन्तानंत कर्मों का आगमन होता रहता है, कोई क्षण ऐसा नहीं है जिस समय इसके अनन्तानंत वर्गणाओं का पिण्डस्वरूप-समयप्रबद्ध नहीं आता रहता है, इसी कारण यह आत्मा नाना दु:खों को भोगता रहता है, (जन्म) यह जीव संसार में कर्मों के उदय से चारों गतियों में जन्म लेता रहता है, द्रव्य-क्षेत्र-कालादि रूप से नरक गति के अपार दु:खों को यह जीवात्मा तैंतीस सागर ही नहीं किंतु अनेक तैंतीस सागरों तक भोगता रहता है, नरकगति ही एक ऐसी गति है जहां से निकलने की अभिलाषा इस जीव के निरन्तर लगी रहती है, अन्य गतियों में यह बात नहीं है, अन्य जिन गतियों में जीव जाता है दुःखी रहने पर भी वहीं रहने की इच्छा रखता है, इसी प्रकार तिर्यञ्च, मनुष्य एवं देव
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
148