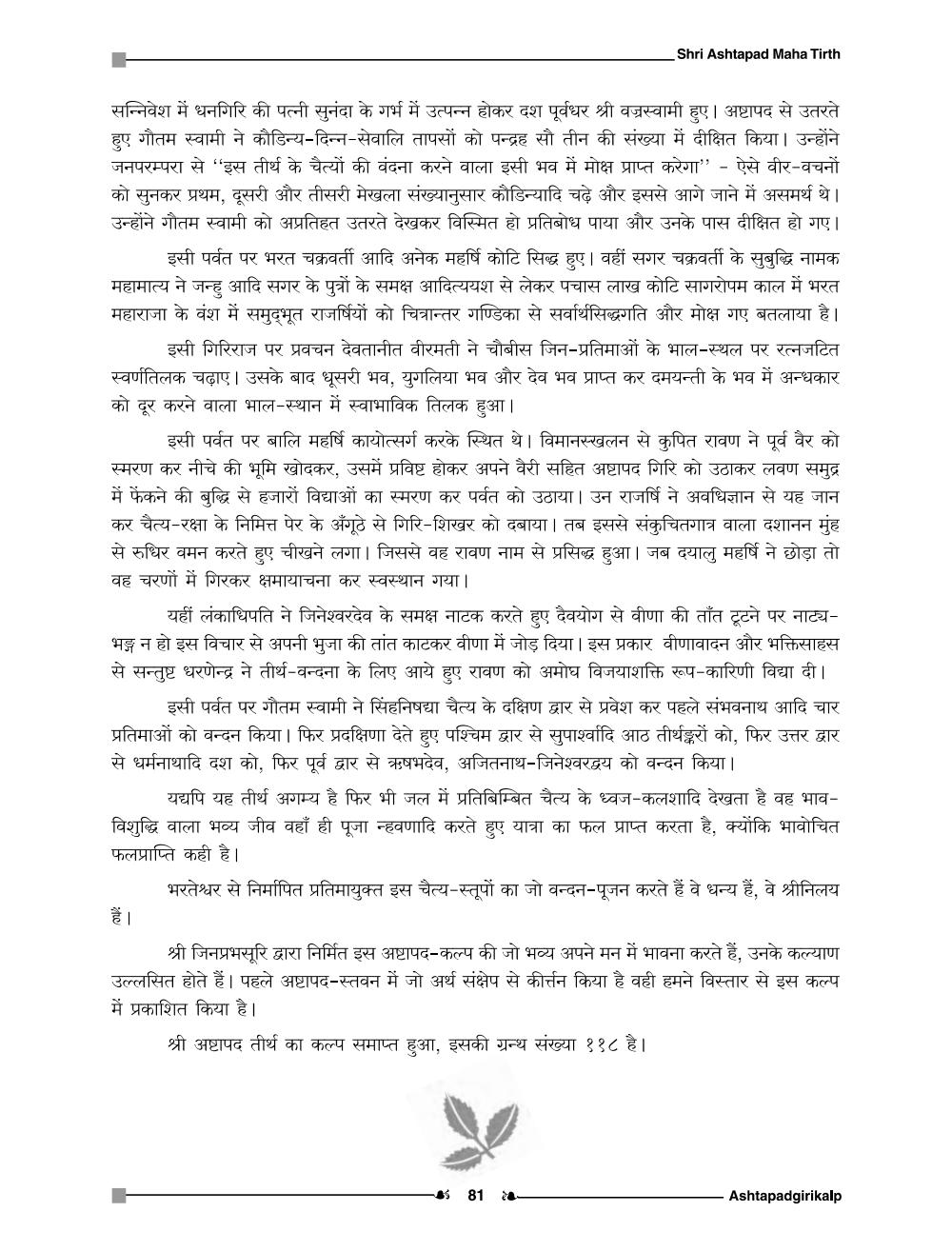________________
_Shri Ashtapad Maha Tirth
सन्निवेश में धनगिरि की पत्नी सुनंदा के गर्भ में उत्पन्न होकर दश पूर्वधर श्री वज्रस्वामी हुए। अष्टापद से उतरते हुए गौतम स्वामी ने कौडिन्य-दिन्न-सेवालि तापसों को पन्द्रह सौ तीन की संख्या में दीक्षित किया। उन्होंने जनपरम्परा से "इस तीर्थ के चैत्यों की वंदना करने वाला इसी भव में मोक्ष प्राप्त करेगा" - ऐसे वीर-वचनों को सुनकर प्रथम, दूसरी और तीसरी मेखला संख्यानुसार कौडिन्यादि चढ़े और इससे आगे जाने में असमर्थ थे। उन्होंने गौतम स्वामी को अप्रतिहत उतरते देखकर विस्मित हो प्रतिबोध पाया और उनके पास दीक्षित हो गए।
इसी पर्वत पर भरत चक्रवर्ती आदि अनेक महर्षि कोटि सिद्ध हुए। वहीं सगर चक्रवर्ती के सुबुद्धि नामक महामात्य ने जन्हु आदि सगर के पुत्रों के समक्ष आदित्ययश से लेकर पचास लाख कोटि सागरोपम काल में भरत महाराजा के वंश में समुद्भूत राजर्षियों को चित्रान्तर गण्डिका से सर्वार्थसिद्धगति और मोक्ष गए बतलाया है।
इसी गिरिराज पर प्रवचन देवतानीत वीरमती ने चौबीस जिन-प्रतिमाओं के भाल-स्थल पर रत्नजटित स्वर्णतिलक चढ़ाए। उसके बाद धूसरी भव, युगलिया भव और देव भव प्राप्त कर दमयन्ती के भव में अन्धकार को दूर करने वाला भाल-स्थान में स्वाभाविक तिलक हुआ।
इसी पर्वत पर बालि महर्षि कायोत्सर्ग करके स्थित थे। विमानस्खलन से कुपित रावण ने पूर्व वैर को स्मरण कर नीचे की भूमि खोदकर, उसमें प्रविष्ट होकर अपने वैरी सहित अष्टापद गिरि को उठाकर लवण समुद्र में फेंकने की बुद्धि से हजारों विद्याओं का स्मरण कर पर्वत को उठाया। उन राजर्षि ने अवधिज्ञान से यह जान कर चैत्य-रक्षा के निमित्त पेर के अंगूठे से गिरि-शिखर को दबाया । तब इससे संकुचितगात्र वाला दशानन मुंह से रुधिर वमन करते हुए चीखने लगा। जिससे वह रावण नाम से प्रसिद्ध हुआ। जब दयालु महर्षि ने छोड़ा तो वह चरणों में गिरकर क्षमायाचना कर स्वस्थान गया।
यहीं लंकाधिपति ने जिनेश्वरदेव के समक्ष नाटक करते हुए दैवयोग से वीणा की ताँत टूटने पर नाट्यभङ्ग न हो इस विचार से अपनी भुजा की तांत काटकर वीणा में जोड़ दिया। इस प्रकार वीणावादन और भक्तिसाहस से सन्तुष्ट धरणेन्द्र ने तीर्थ-वन्दना के लिए आये हुए रावण को अमोघ विजयाशक्ति रूप-कारिणी विद्या दी।
इसी पर्वत पर गौतम स्वामी ने सिंहनिषद्या चैत्य के दक्षिण द्वार से प्रवेश कर पहले संभवनाथ आदि चार प्रतिमाओं को वन्दन किया। फिर प्रदक्षिणा देते हुए पश्चिम द्वार से सुपा दि आठ तीर्थङ्करों को, फिर उत्तर द्वार से धर्मनाथादि दश को, फिर पूर्व द्वार से ऋषभदेव, अजितनाथ-जिनेश्वरद्वय को वन्दन किया।
यद्यपि यह तीर्थ अगम्य है फिर भी जल में प्रतिबिम्बित चैत्य के ध्वज-कलशादि देखता है वह भावविशुद्धि वाला भव्य जीव वहाँ ही पूजा न्हवणादि करते हुए यात्रा का फल प्राप्त करता है, क्योंकि भावोचित फलप्राप्ति कही है।
भरतेश्वर से निर्मापित प्रतिमायुक्त इस चैत्य-स्तूपों का जो वन्दन-पूजन करते हैं वे धन्य हैं, वे श्रीनिलय
श्री जिनप्रभसूरि द्वारा निर्मित इस अष्टापद-कल्प की जो भव्य अपने मन में भावना करते हैं, उनके कल्याण उल्लसित होते हैं। पहले अष्टापद-स्तवन में जो अर्थ संक्षेप से कीर्तन किया है वही हमने विस्तार से इस कल्प में प्रकाशित किया है।
श्री अष्टापद तीर्थ का कल्प समाप्त हुआ, इसकी ग्रन्थ संख्या ११८ है।
-681
Ashtapadgirikalp