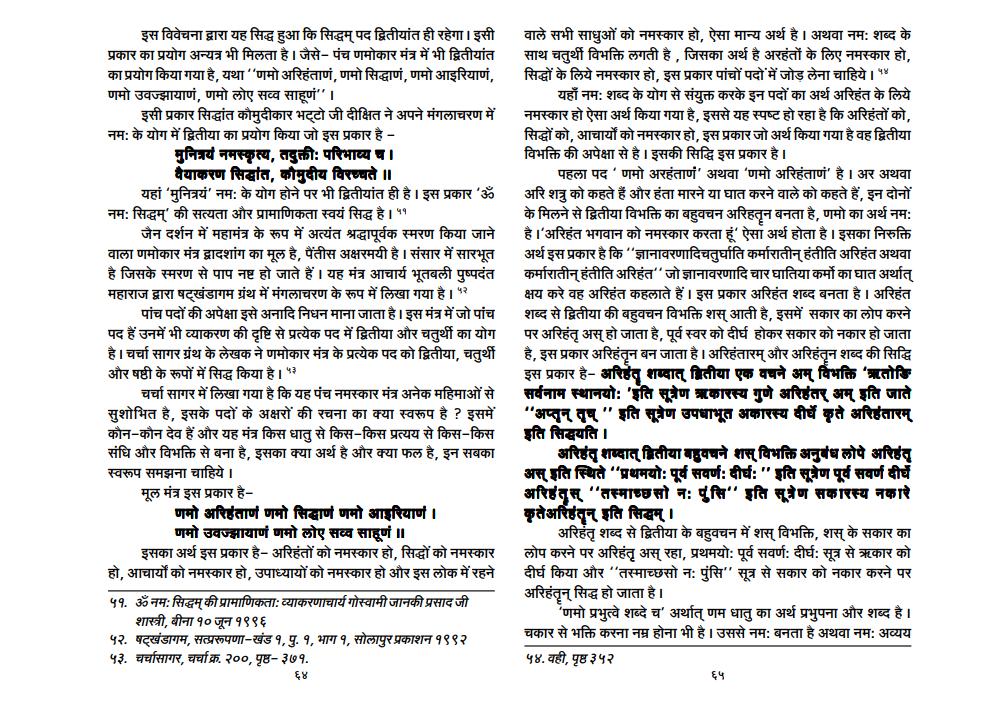________________
इस विवेचना द्वारा यह सिद्ध हुआ कि सिद्धम् पद द्वितीयांत ही रहेगा। इसी वाले सभी साधुओं को नमस्कार हो, ऐसा मान्य अर्थ है। अथवा नम: शब्द के प्रकार का प्रयोग अन्यत्र भी मिलता है। जैसे- पंच णमोकार मंत्र में भी द्वितीयांत साथ चतुर्थी विभक्ति लगती है, जिसका अर्थ है अरहंतों के लिए नमस्कार हो, का प्रयोग किया गया है, यथा"णमो अरिहंताणं,णमो सिद्धाणं,णमो आइरियाणं, सिद्धों के लिये नमस्कार हो, इस प्रकार पांचों पदों में जोड़ लेना चाहिये। ५४ णमो उवज्झायाणं, णमो लोए सव्व साहूणं"।
यहाँ नमः शब्द के योग से संयुक्त करके इन पदों का अर्थ अरिहंत के लिये इसी प्रकार सिद्धांत कौमुदीकार भट्टो जी दीक्षित ने अपने मंगलाचरण में नमस्कार हो ऐसा अर्थ किया गया है, इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि अरिहंतों को, नम: के योग में द्वितीया का प्रयोग किया जो इस प्रकार है -
सिद्धों को, आचार्यों को नमस्कार हो, इस प्रकार जो अर्थ किया गया है वह द्वितीया मुनित्रयं नमस्कृत्य, तदुक्ती: परिभाष्यप।
विभक्ति की अपेक्षा से है। इसकी सिद्धि इस प्रकार है। वैयाकरण सिद्धांत, कौमुदीय विरच्यते ॥
पहला पद णमो अरहताणं' अथवा 'णमो अरिहंताणं' है । अर अथवा यहां 'मुनित्रयं' नम: के योग होने पर भी द्वितीयांत ही है। इस प्रकार 'ॐ अरि शत्रु को कहते हैं और हंता मारने या घात करने वाले को कहते हैं, इन दोनों नम: सिद्धम्' की सत्यता और प्रामाणिकता स्वयं सिद्ध है। ५५
के मिलने से द्वितीया विभक्ति का बहुवचन अरिहतृन बनता है, णमो का अर्थ नमः जैन दर्शन में महामंत्र के रूप में अत्यंत श्रद्धापूर्वक स्मरण किया जाने । है। अरिहंत भगवान को नमस्कार करता हूं' ऐसा अर्थ होता है। इसका निरुक्ति वाला णमोकार मंत्र द्वादशांग का मूल है, पैंतीस अक्षरमयी है। संसार में सारभूत अर्थ इस प्रकार है कि "ज्ञानावरणादिचतुर्घाति कर्मारातीन हंतीति अरिहंत अथवा है जिसके स्मरण से पाप नष्ट हो जाते हैं। यह मंत्र आचार्य भूतबली पुष्पदंत कारातीन हंतीति अरिहंत"जोज्ञानावरणादिचार घातिया कर्मो का घात अर्थात् महाराज द्वारा षट्खंडागम ग्रंथ में मंगलाचरण के रूप में लिखा गया है। ५२ क्षय करे वह अरिहंत कहलाते हैं। इस प्रकार अरिहंत शब्द बनता है। अरिहंत
पांच पदों की अपेक्षा इसे अनादि निधन माना जाता है। इस मंत्र में जो पांच । शब्द से द्वितीया की बहुवचन विभक्ति शस् आती है, इसमें सकार का लोप करने पद हैं उनमें भी व्याकरण की दृष्टि से प्रत्येक पद में द्वितीया और चतुर्थी का योग पर अरिहंतृ अस् हो जाता है, पूर्व स्वर को दीर्घ होकर सकार को नकार हो जाता है। चर्चा सागर ग्रंथ के लेखक ने णमोकार मंत्र के प्रत्येक पद को द्वितीया, चतुर्थी है, इस प्रकार अरिहंतृन बन जाता है। अरिहंतारम् और अरिहंतृन शब्द की सिद्धि और षष्ठी के रूपों में सिद्ध किया है। ५३
इस प्रकार है- अरिहंत शब्दात् द्वितीया एक वचने अम् विभक्ति 'बातोडि चर्चा सागर में लिखा गया है कि यह पंच नमस्कार मंत्र अनेक महिमाओं से सर्वनाम स्थानयोः 'इति सत्रेण ऋकारस्य गुणे अरिहंतर अम् इति जाते सुशोभित है, इसके पदों के अक्षरों की रचना का क्या स्वरूप है ? इसमें "अप्तन तप"इति सूत्रेण उपधाभूत अकारस्य वीर्वंकते अरिहंतारम कौन-कौन देव हैं और यह मंत्र किस धातु से किस-किस प्रत्यय से किस-किस इति सिद्धयति। संधि और विभक्ति से बना है, इसका क्या अर्थ है और क्या फल है, इन सबका अरिहंत शब्दात द्वितीया बहुवचने शस् विभक्ति अनुबंध लोपे अरिहंत स्वरूप समझना चाहिये।
अस् इति स्थिते "प्रथमयोः पूर्व सवर्ण: दीर्घः" इति सूत्रेण पूर्व सवर्ण दीर्घ मूल मंत्र इस प्रकार है
अरिहंतुस् "तस्माच्छ सो नः सि"इति सण सकारस्य नकारे णमो अरिहंताणं णमो सिद्धाणं णमो आइरियाणं ।
कृतेअरिहंतन इति सिद्धम्। णमो उवज्झायाणं णमो लोए सव्व साहूणं॥
अरिहंत शब्द से द्वितीया के बहुवचन में शस विभक्ति, शस् के सकार का इसका अर्थ इस प्रकार है- अरिहंतों को नमस्कार हो, सिद्धों को नमस्कार लोप करने पर अरिहंत अस् रहा, प्रथमयो: पूर्व सवर्ण: दीर्घ: सूत्र से ऋकार को हो, आचार्यों को नमस्कार हो, उपाध्यायों को नमस्कार हो और इस लोक में रहने दीर्घ किया और "तस्माच्छसो नः पुंसि" सूत्र से सकार को नकार करने पर ५१. ॐ नम: सिद्धम् की प्रामाणिकता: व्याकरणाचार्य गोस्वामी जानकी प्रसाद जी
अरिहंतृन् सिद्ध हो जाता है। शास्त्री, बीना १० जून १९९६
'णमो प्रभुत्वे शब्दे च' अर्थात् णम धातु का अर्थ प्रभुपना और शब्द है। ५२. षट्खंडागम, सत्प्ररूपणा-खंड १,पु.१, भाग १, सोलापुर प्रकाशन १९९२
चकार से भक्ति करना नम्र होना भी है। उससे नम: बनता है अथवा नम: अव्यय ५३. चर्चासागर, चर्चा क्र.२००, पृष्ठ-३७१.
५४. वही, पृष्ठ ३५२