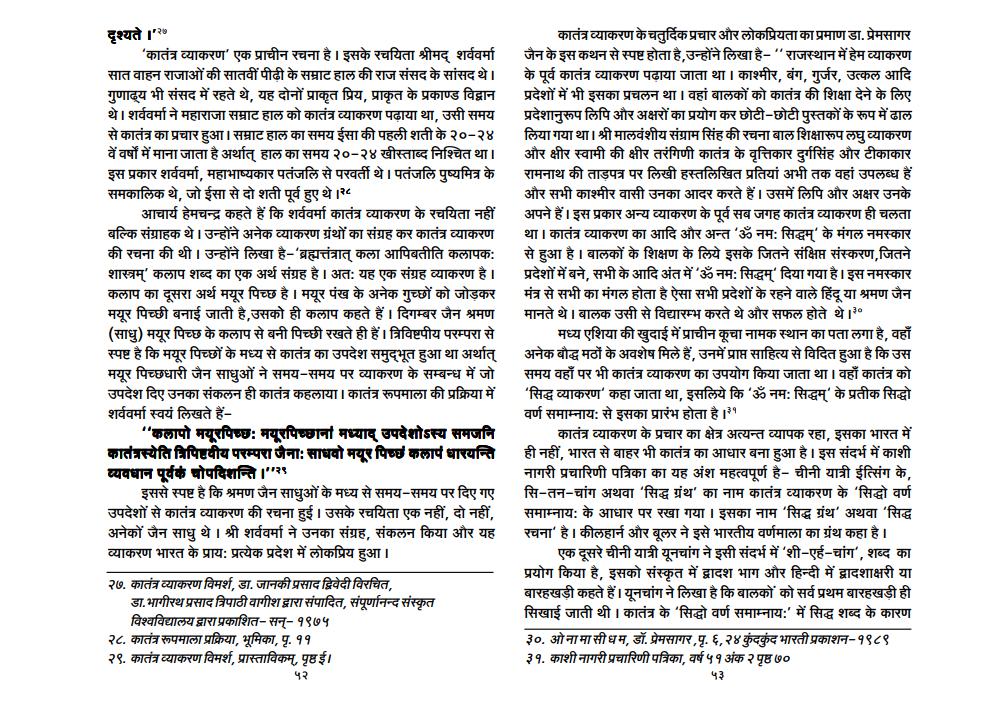________________
दृश्यते ॥२७
'कातंत्र व्याकरण' एक प्राचीन रचना है। इसके रचयिता श्रीमद् शर्ववर्मा सातवाहन राजाओं की सातवीं पीढ़ी के सम्राट हाल की राज संसद के सांसद थे। गुणाढ्य भी संसद में रहते थे, यह दोनों प्राकृत प्रिय, प्राकृत के प्रकाण्ड विद्वान थे। शर्ववर्मा ने महाराजा सम्राट हाल को कातंत्र व्याकरण पढ़ाया था, उसी समय से कातंत्र का प्रचार हुआ। सम्राट हाल का समय ईसा की पहली शती के २०-२४ वें वर्षों में माना जाता है अर्थात् हाल का समय २० - २४ खीस्ताब्द निश्चित था । इस प्रकार शर्ववर्मा, महाभाष्यकार पतंजलि से परवर्ती थे। पतंजलि पुष्यमित्र के समकालिक थे, जो ईसा से दो शती पूर्व हुए थे । २८
आचार्य हेमचन्द्र कहते हैं कि शर्ववर्मा कातंत्र व्याकरण के रचयिता नहीं बल्कि संग्राहक थे। उन्होंने अनेक व्याकरण ग्रंथों का संग्रह कर कातंत्र व्याकरण की रचना की थी। उन्होंने लिखा है- 'ब्रह्मत्तंत्रात् कला आपिबतीति कलापक: शास्त्रम्' कलाप शब्द का एक अर्थ संग्रह है। अत: यह एक संग्रह व्याकरण है। कलाप का दूसरा अर्थ मयूर पिच्छ है। मयूर पंख के अनेक गुच्छों को जोड़कर मयूरपिच्छी बनाई जाती है, उसको ही कलाप कहते हैं । दिगम्बर जैन श्रमण (साधु) मयूर पिच्छ के कलाप से बनी पिच्छी रखते ही हैं। त्रिविष्टपीय परम्परा से स्पष्ट है कि मयूरपिच्छों के मध्य से कातंत्र का उपदेश समुद्भूत हुआ था अर्थात् मयूरपिच्छधारी जैन साधुओं ने समय-समय पर व्याकरण के सम्बन्ध में जो उपदेश दिए उनका संकलन ही कातंत्र कहलाया। कातंत्र रूपमाला की प्रक्रिया में शर्ववर्मा स्वयं लिखते हैं
"कलापो मयूरपिच्छः मयूरपिच्छानां मध्याद् उपवेशोऽस्य समजनि कातंत्रस्येति त्रिपिष्टवीय परम्परा जैना: साधवो मयूर पिच्छं कलापं धारयन्ति व्यवधान पूर्वकं चोपदिशन्ति । २९
इससे स्पष्ट है कि श्रमण जैन साधुओं के मध्य से समय-समय पर दिए गए उपदेशों से कातंत्र व्याकरण की रचना हुई। उसके रचयिता एक नहीं, दो नहीं, अनेकों जैन साधु थे। श्री शर्ववर्मा ने उनका संग्रह, संकलन किया और यह व्याकरण भारत के प्राय: प्रत्येक प्रदेश में लोकप्रिय हुआ ।
२७. कातंत्र व्याकरण विमर्श, डा. जानकी प्रसाद द्विवेदी विरचित,
डा. भागीरथ प्रसाद त्रिपाठी वागीश द्वारा संपादित, संपूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित- सन् १९७५
२८. कातंत्र रूपमाला प्रक्रिया, भूमिका, पृ. ११
२९. कातंत्र व्याकरण विमर्श, प्रास्ताविकम्, पृष्ठ ई ।
५२
कातंत्र व्याकरण के चतुर्दिक प्रचार और लोकप्रियता का प्रमाण डा. प्रेमसागर जैन के इस कथन से स्पष्ट होता है, उन्होंने लिखा है- " राजस्थान में हेम व्याकरण के पूर्व कातंत्र व्याकरण पढ़ाया जाता था। काश्मीर, बंग, गुर्जर, उत्कल आदि प्रदेशों में भी इसका प्रचलन था। वहां बालकों को कातंत्र की शिक्षा देने के लिए प्रदेशानुरूप लिपि और अक्षरों का प्रयोग कर छोटी-छोटी पुस्तकों के रूप में ढाल लिया गया था। श्री मालवंशीय संग्राम सिंह की रचना बाल शिक्षारूप लघु व्याकरण और क्षीर स्वामी की क्षीर तरंगिणी कातंत्र के वृत्तिकार दुर्गसिंह और टीकाकार रामनाथ की ताड़पत्र पर लिखी हस्तलिखित प्रतियां अभी तक वहां उपलब्ध हैं। और सभी काश्मीर वासी उनका आदर करते हैं। उसमें लिपि और अक्षर उनके अपने हैं। इस प्रकार अन्य व्याकरण के पूर्व सब जगह कातंत्र व्याकरण ही चलता था। कातंत्र व्याकरण का आदि और अन्त 'ॐ नमः सिद्धम्' के मंगल नमस्कार से हुआ है। बालकों के शिक्षण के लिये इसके जितने संक्षिप्त संस्करण, जितने प्रदेशों में बने, सभी के आदि अंत में 'ॐ नमः सिद्धम्' दिया गया है। इस नमस्कार मंत्र से सभी का मंगल होता है ऐसा सभी प्रदेशों के रहने वाले हिंदू या श्रमण जैन • मानते थे। बालक उसी से विद्यारम्भ करते थे और सफल होते थे । ३०
मध्य एशिया की खुदाई में प्राचीन कूचा नामक स्थान का पता लगा है, वहाँ अनेक बौद्ध मठों के अवशेष मिले हैं, उनमें प्राप्त साहित्य से विदित हुआ है कि उस समय वहाँ पर भी कातंत्र व्याकरण का उपयोग किया जाता था। वहाँ कातंत्र को 'सिद्ध व्याकरण' कहा जाता था, इसलिये कि 'ॐ नमः सिद्धम्' के प्रतीक सिद्धो वर्ण समाम्नाय से इसका प्रारंभ होता है । ३१
कातंत्र व्याकरण के प्रचार का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक रहा, इसका भारत में ही नहीं, भारत से बाहर भी कातंत्र का आधार बना हुआ है। इस संदर्भ में काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका का यह अंश महत्वपूर्ण है- चीनी यात्री इत्सिंग के, सि-तन चांग अथवा 'सिद्ध ग्रंथ' का नाम कातंत्र व्याकरण के 'सिद्धो वर्ण समाम्नाय: के आधार पर रखा गया। इसका नाम 'सिद्ध ग्रंथ' अथवा 'सिद्ध रचना' है। कीलहार्न और बूलर ने इसे भारतीय वर्णमाला का ग्रंथ कहा है।
एक दूसरे चीनी यात्री यूनचांग ने इसी संदर्भ में 'शी- एर्ह चांग', शब्द का प्रयोग किया है, इसको संस्कृत में द्वादश भाग और हिन्दी में द्वादशाक्षरी या बारहखड़ी कहते हैं। यूनचांग ने लिखा है कि बालकों को सर्व प्रथम बारहखड़ी ही सिखाई जाती थी । कातंत्र के 'सिद्धो वर्ण समाम्नाय : ' में सिद्ध शब्द के कारण ३०. ओनामा सीधम, डॉ. प्रेमसागर, पृ. ६, २४ कुंदकुंद भारती प्रकाशन - १९८९ ३१. काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका, वर्ष ५१ अंक २ पृष्ठ ७०
५३