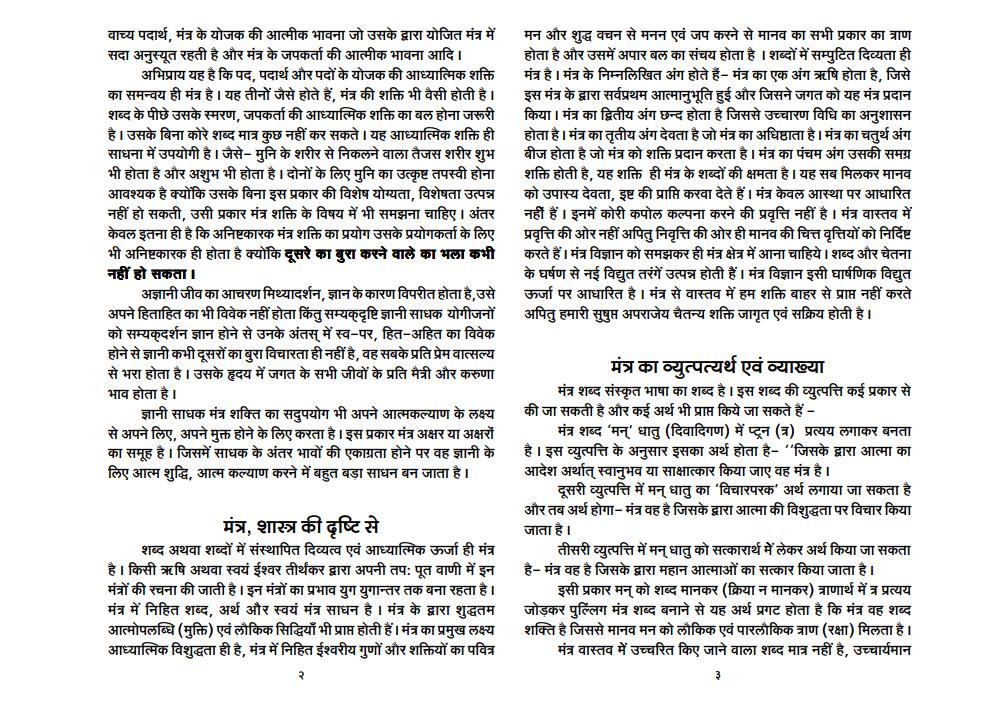________________
वाच्य पदार्थ, मंत्र के योजक की आत्मीक भावना जो उसके द्वारा योजित मंत्र में सदा अनुस्यूत रहती है और मंत्र के जपकर्ता की आत्मीक भावना आदि ।
अभिप्राय यह है कि पद, पदार्थ और पदों के योजक की आध्यात्मिक शक्ति का समन्वय ही मंत्र है। यह तीनों जैसे होते हैं, मंत्र की शक्ति भी वैसी होती है। शब्द के पीछे उसके स्मरण, जपकर्ता की आध्यात्मिक शक्ति का बल होना जरूरी है। उसके बिना कोरे शब्द मात्र कुछ नहीं कर सकते। यह आध्यात्मिक शक्ति ही साधना में उपयोगी है। जैसे- मुनि के शरीर से निकलने वाला तैजस शरीर शुभ भी होता है और अशुभ भी होता है। दोनों के लिए मुनि का उत्कृष्ट तपस्वी होना आवश्यक है क्योंकि उसके बिना इस प्रकार की विशेष योग्यता, विशेषता उत्पन्न नहीं हो सकती, उसी प्रकार मंत्र शक्ति के विषय में भी समझना चाहिए। अंतर केवल इतना ही है कि अनिष्टकारक मंत्र शक्ति का प्रयोग उसके प्रयोगकर्ता के लिए भी अनिष्टकारक ही होता है क्योंकि दूसरे का बुरा करने वाले का भला कभी नहीं हो सकता।
अज्ञानी जीव का आचरण मिथ्यादर्शन, ज्ञान के कारण विपरीत होता है, उसे अपने हिताहित का भी विवेक नहीं होता किंतु सम्यक्दृष्टि ज्ञानी साधक योगीजनों को सम्यक्दर्शन ज्ञान होने से उनके अंतस् में स्व-पर, हित-अहित का विवेक होने से ज्ञानी कभी दूसरों का बुरा विचारता ही नहीं है, वह सबके प्रति प्रेम वात्सल्य से भरा होता है। उसके हृदय में जगत के सभी जीवों के प्रति मैत्री और करुणा भाव होता है।
ज्ञानी साधक मंत्र शक्ति का सदुपयोग भी अपने आत्मकल्याण के लक्ष्य से अपने लिए, अपने मुक्त होने के लिए करता है। इस प्रकार मंत्र अक्षर या अक्षरों का समूह है। जिसमें साधक के अंतर भावों की एकाग्रता होने पर वह ज्ञानी के लिए आत्म शुद्धि, आत्म कल्याण करने में बहुत बड़ा साधन बन जाता है।
मंत्र शास्त्र की दृष्टि से
शब्द अथवा शब्दों में संस्थापित दिव्यत्व एवं आध्यात्मिक ऊर्जा ही मंत्र है। किसी ऋषि अथवा स्वयं ईश्वर तीर्थंकर द्वारा अपनी तपः पूत वाणी में इन मंत्रों की रचना की जाती है। इन मंत्रों का प्रभाव युग युगान्तर तक बना रहता है। मंत्र में निहित शब्द, अर्थ और स्वयं मंत्र साधन है। मंत्र के द्वारा शुद्धतम आत्मोपलब्धि (मुक्ति) एवं लौकिक सिद्धियाँ भी प्राप्त होती हैं। मंत्र का प्रमुख लक्ष्य आध्यात्मिक विशुद्धता ही है, मंत्र में निहित ईश्वरीय गुणों और शक्तियों का पवित्र
२
मन और शुद्ध वचन से मनन एवं जप करने से मानव का सभी प्रकार का त्राण होता है और उसमें अपार बल का संचय होता है । शब्दों में सम्पुटित दिव्यता ही मंत्र है। मंत्र के निम्नलिखित अंग होते हैं- मंत्र का एक अंग ऋषि होता है, जिसे इस मंत्र के द्वारा सर्वप्रथम आत्मानुभूति हुई और जिसने जगत को यह मंत्र प्रदान किया। मंत्र का द्वितीय अंग छन्द होता है जिससे उच्चारण विधि का अनुशासन होता है। मंत्र का तृतीय अंग देवता है जो मंत्र का अधिष्ठाता है। मंत्र का चतुर्थ अंग बीज होता है जो मंत्र को शक्ति प्रदान करता है। मंत्र का पंचम अंग उसकी समग्र शक्ति होती है, यह शक्ति ही मंत्र के शब्दों की क्षमता है। यह सब मिलकर मानव को उपास्य देवता, इष्ट की प्राप्ति करवा देते हैं। मंत्र केवल आस्था पर आधारित नहीं हैं। इनमें कोरी कपोल कल्पना करने की प्रवृत्ति नहीं है। मंत्र वास्तव में प्रवृत्ति की ओर नहीं अपितु निवृत्ति की ओर ही मानव की चित्त वृत्तियों को निर्दिष्ट करते हैं। मंत्र विज्ञान को समझकर ही मंत्र क्षेत्र में आना चाहिये। शब्द और चेतना के घर्षण से नई विद्युत तरंगें उत्पन्न होती हैं। मंत्र विज्ञान इसी घार्षणिक विद्युत ऊर्जा पर आधारित है। मंत्र से वास्तव में हम शक्ति बाहर से प्राप्त नहीं करते अपितु हमारी सुषुप्त अपराजेय चैतन्य शक्ति जागृत एवं सक्रिय होती है।
मंत्र का व्युत्पत्यर्थ एवं व्याख्या
मंत्र शब्द संस्कृत भाषा का शब्द है। इस शब्द की व्युत्पत्ति कई प्रकार से की जा सकती है और कई अर्थ भी प्राप्त किये जा सकते हैं -
मंत्र शब्द 'मन्' धातु (दिवादिगण) में प्टून (त्र) प्रत्यय लगाकर बनता है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार इसका अर्थ होता है- "जिसके द्वारा आत्मा का आदेश अर्थात् स्वानुभव या साक्षात्कार किया जाए वह मंत्र है।
दूसरी व्युत्पत्ति में मन् धातु का 'विचारपरक' अर्थ लगाया जा सकता है और तब अर्थ होगा- मंत्र वह है जिसके द्वारा आत्मा की विशुद्धता पर विचार किया जाता है।
तीसरी व्युत्पत्ति में मन् धातु को सत्कारार्थ में लेकर अर्थ किया जा सकता है- मंत्र वह है जिसके द्वारा महान आत्माओं का सत्कार किया जाता है।
इसी प्रकार मन् को शब्द मानकर (क्रिया न मानकर) त्राणार्थ में त्र प्रत्यय जोड़कर पुल्लिंग मंत्र शब्द बनाने से यह अर्थ प्रगट होता है कि मंत्र वह शब्द शक्ति है जिससे मानव मन को लौकिक एवं पारलौकिक त्राण (रक्षा) मिलता है। मंत्र वास्तव में उच्चरित किए जाने वाला शब्द मात्र नहीं है, उच्चार्यमान
३