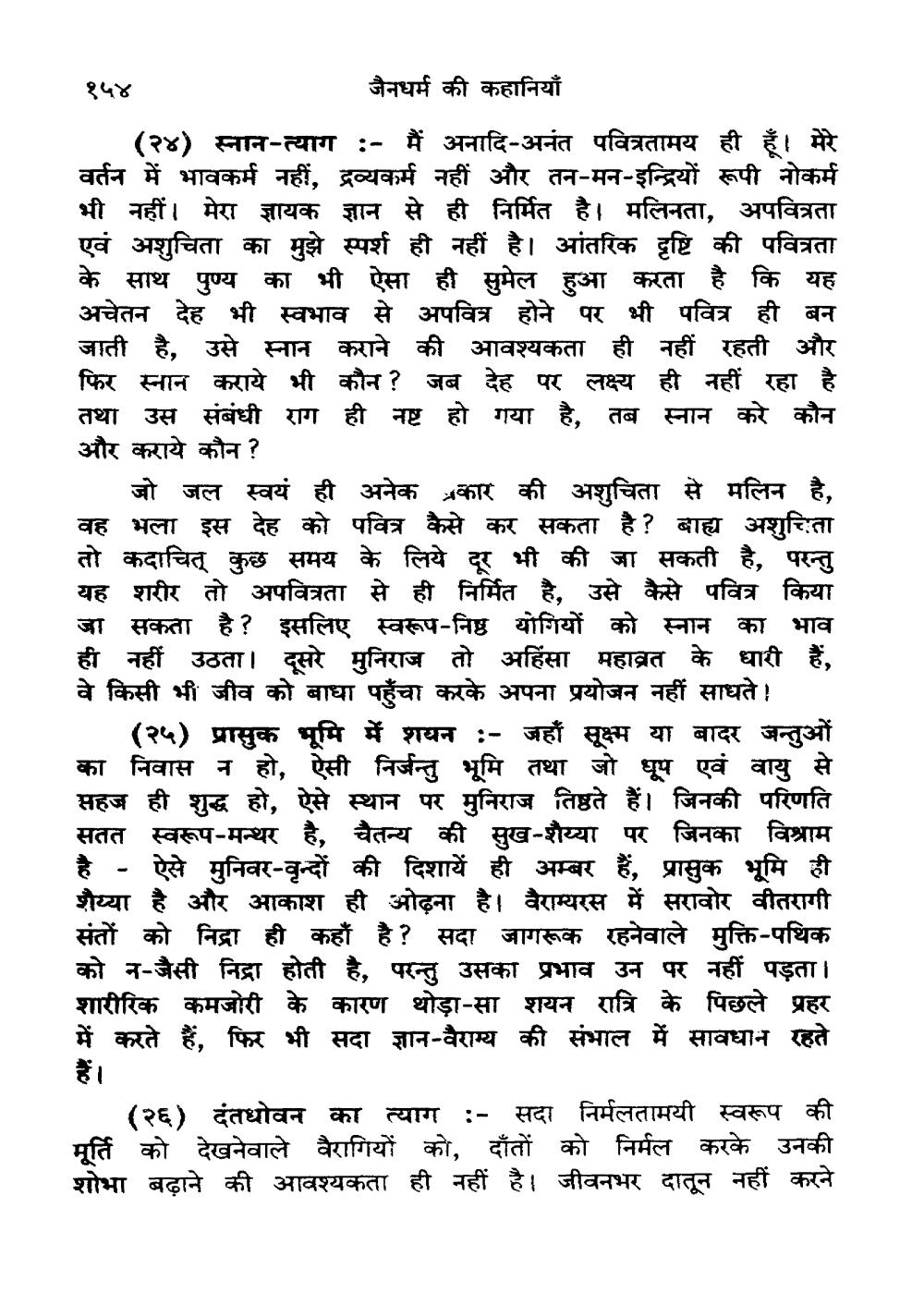________________
१५४
जैनधर्म की कहानियाँ (२४) स्नान-त्याग :- मैं अनादि-अनंत पवित्रतामय ही हूँ। मेरे वर्तन में भावकर्म नहीं, द्रव्यकर्म नहीं और तन-मन-इन्द्रियों रूपी नोकर्म भी नहीं। मेरा ज्ञायक ज्ञान से ही निर्मित है। मलिनता, अपवित्रता एवं अशुचिता का मुझे स्पर्श ही नहीं है। आंतरिक दृष्टि की पवित्रता के साथ पुण्य का भी ऐसा ही सुमेल हुआ करता है कि यह अचेतन देह भी स्वभाव से अपवित्र होने पर भी पवित्र ही बन जाती है, उसे स्नान कराने की आवश्यकता ही नहीं रहती और फिर स्नान कराये भी कौन? जब देह पर लक्ष्य ही नहीं रहा है तथा उस संबंधी राग ही नष्ट हो गया है, तब स्नान करे कौन और कराये कौन ? ___ जो जल स्वयं ही अनेक प्रकार की अशुचिता से मलिन है, वह भला इस देह को पवित्र कैसे कर सकता है? बाह्य अशुचिता तो कदाचित् कुछ समय के लिये दूर भी की जा सकती है, परन्तु यह शरीर तो अपवित्रता से ही निर्मित है, उसे कैसे पवित्र किया जा सकता है? इसलिए स्वरूप-निष्ठ योगियों को स्नान का भाव ही नहीं उठता। दूसरे मुनिराज तो अहिंसा महाव्रत के धारी हैं, वे किसी भी जीव को बाधा पहुँचा करके अपना प्रयोजन नहीं साधते।
(२५) प्रासुक भूमि में शयन :- जहाँ सूक्ष्म या बादर जन्तुओं का निवास न हो, ऐसी निर्जन्तु भूमि तथा जो धूप एवं वायु से सहज ही शुद्ध हो, ऐसे स्थान पर मुनिराज तिष्ठते हैं। जिनकी परिणति सतत स्वरूप-मन्थर है, चैतन्य की सुख-शैय्या पर जिनका विश्राम है - ऐसे मुनिवर-वृन्दों की दिशायें ही अम्बर हैं, प्रासुक भूमि ही शैय्या है और आकाश ही ओढ़ना है। वैराम्यरस में सरावोर वीतरागी संतों को निद्रा ही कहाँ है? सदा जागरूक रहनेवाले मुक्ति-पथिक को न-जैसी निद्रा होती है, परन्तु उसका प्रभाव उन पर नहीं पड़ता। शारीरिक कमजोरी के कारण थोड़ा-सा शयन रात्रि के पिछले प्रहर में करते हैं, फिर भी सदा ज्ञान-वैराग्य की संभाल में सावधान रहते
(२६) दंतधोवन का त्याग :- सदा निर्मलतामयी स्वरूप की मूर्ति को देखनेवाले वैरागियों को, दाँतों को निर्मल करके उनकी शोभा बढ़ाने की आवश्यकता ही नहीं है। जीवनभर दातून नहीं करने