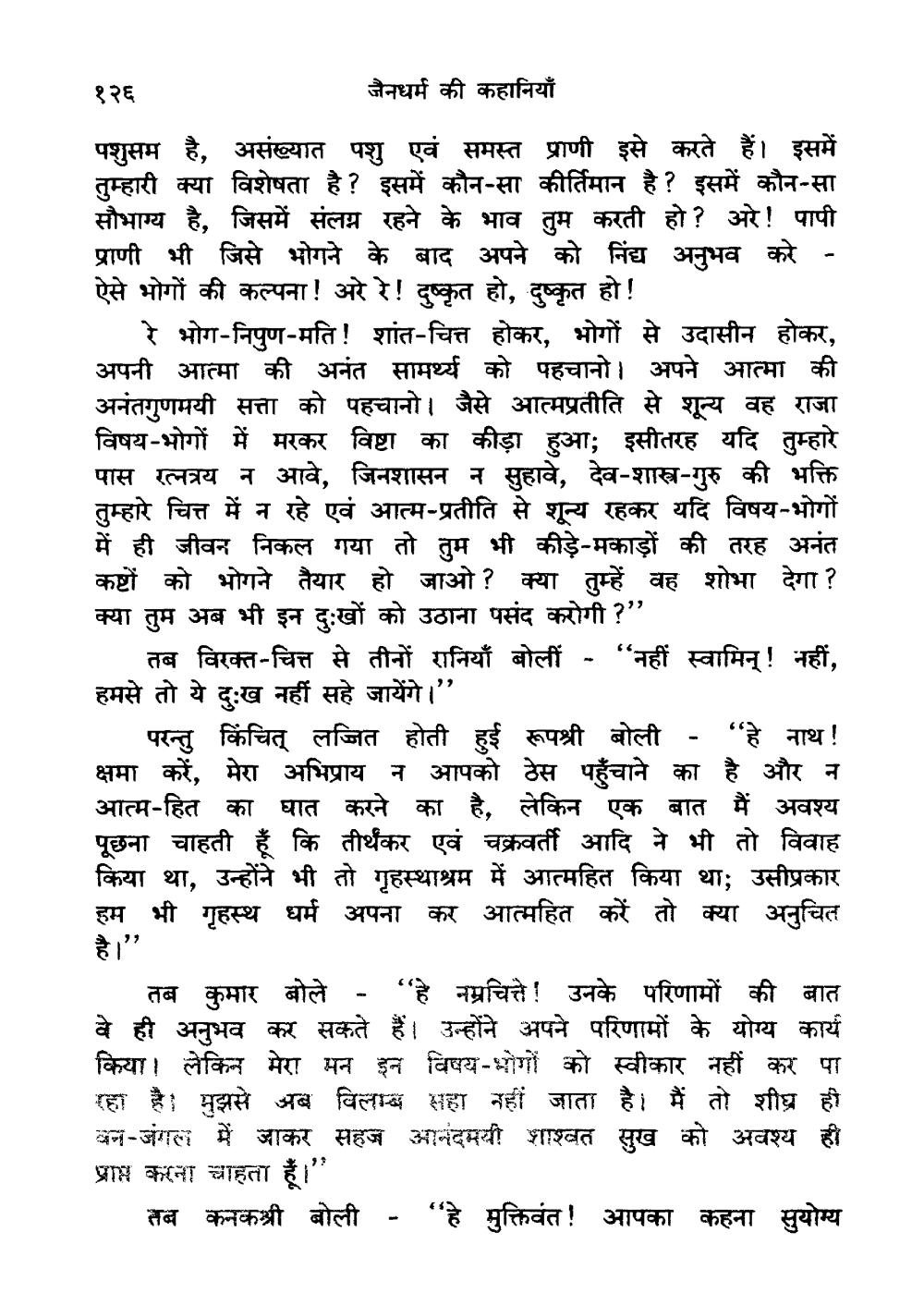________________
१२६
जैनधर्म की कहानियाँ पशुसम है, असंख्यात पशु एवं समस्त प्राणी इसे करते हैं। इसमें तुम्हारी क्या विशेषता है? इसमें कौन-सा कीर्तिमान है ? इसमें कौन-सा सौभाग्य है, जिसमें संलग्न रहने के भाव तुम करती हो? अरे! पापी प्राणी भी जिसे भोगने के बाद अपने को निंद्य अनुभव करे - ऐसे भोगों की कल्पना! अरे रे! दुष्कृत हो, दुष्कृत हो!
रे भोग-निपुण-मति! शांत-चित्त होकर, भोगों से उदासीन होकर, अपनी आत्मा की अनंत सामर्थ्य को पहचानो। अपने आत्मा की अनंतगुणमयी सत्ता को पहचानो। जैसे आत्मप्रतीति से शून्य वह राजा विषय-भोगों में मरकर विष्टा का कीड़ा हुआ; इसीतरह यदि तुम्हारे पास रत्नत्रय न आवे, जिनशासन न सुहावे, देव-शास्त्र-गुरु की भक्ति तुम्हारे चित्त में न रहे एवं आत्म-प्रतीति से शून्य रहकर यदि विषय-भोगों में ही जीवन निकल गया तो तुम भी कीड़े-मकाड़ों की तरह अनंत कष्टों को भोगने तैयार हो जाओ? क्या तुम्हें वह शोभा देगा? क्या तुम अब भी इन दुःखों को उठाना पसंद करोगी?"
तब विरक्त-चित्त से तीनों रानियाँ बोलीं - “नहीं स्वामिन् ! नहीं, हमसे तो ये दुःख नहीं सहे जायेंगे।"
परन्तु किंचित् लज्जित होती हुई रूपश्री बोली - "हे नाथ! क्षमा करें, मेरा अभिप्राय न आपको ठेस पहुँचाने का है और न आत्म-हित का घात करने का है, लेकिन एक बात मैं अवश्य पूछना चाहती हूँ कि तीर्थंकर एवं चक्रवर्ती आदि ने भी तो विवाह किया था, उन्होंने भी तो गृहस्थाश्रम में आत्महित किया था; उसीप्रकार हम भी गृहस्थ धर्म अपना कर आत्महित करें तो क्या अनुचित है।"
तब कुमार बोले - “हे नम्रचित्ते! उनके परिणामों की बात वे ही अनुभव कर सकते हैं। उन्होंने अपने परिणामों के योग्य कार्य किया। लेकिन मेरा मन इन विषय-भोगों को स्वीकार नहीं कर पा रहा है। मझसे अब विलाब सहा नहीं जाता है। मैं तो शीघ्र ही बन-जंगल में जाकर सहज आनंदमयी शाश्वत सुख को अवश्य ही प्राप्त करना चाहता हूँ।"
सब कनकश्री बोली - "हे मुक्तिवंत! आपका कहना सुयोग्य