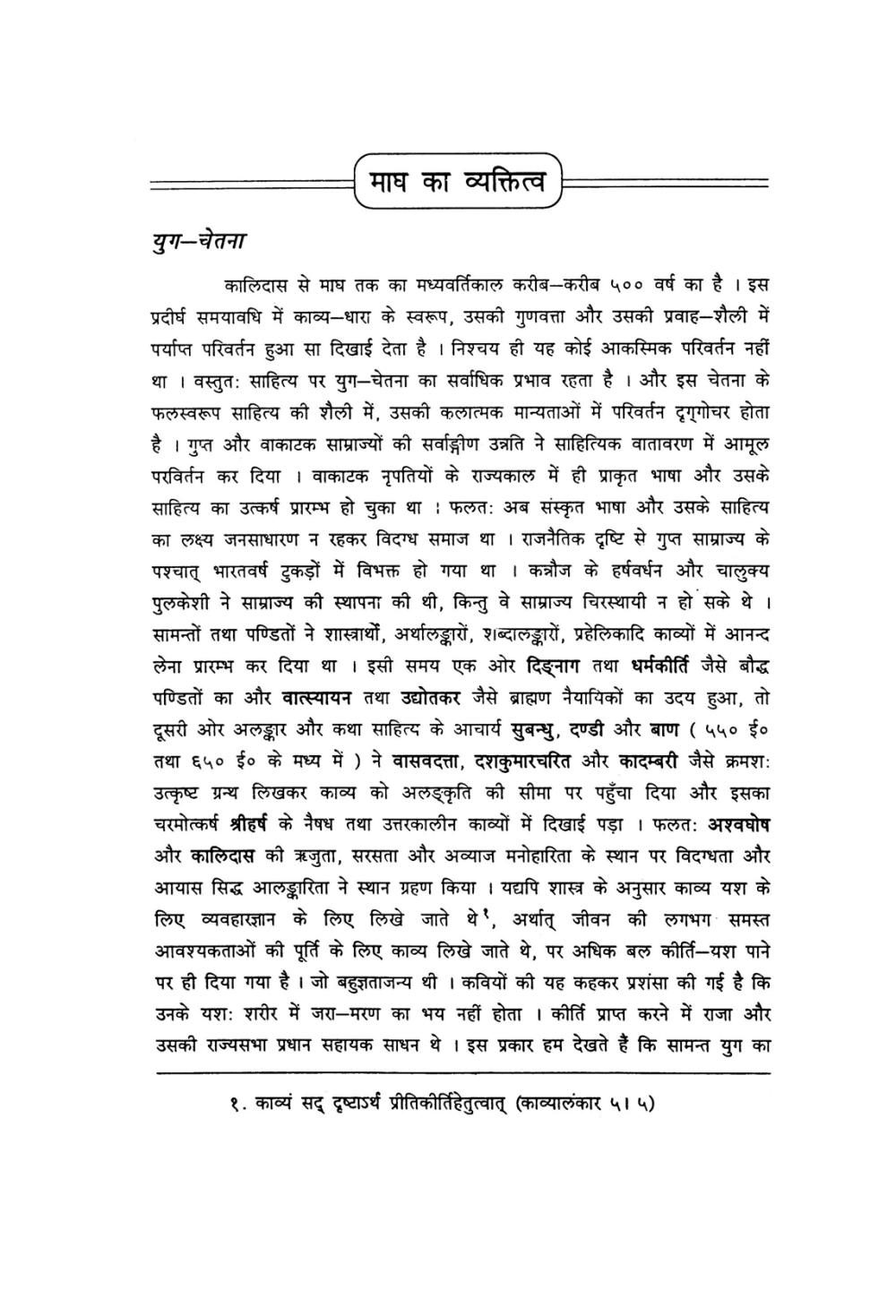________________
माघ का व्यक्तित्व
युग-चेतना
कालिदास से माघ तक का मध्यवर्तिकाल करीब-करीब ५०० वर्ष का है । इस प्रदीर्घ समयावधि में काव्य-धारा के स्वरूप, उसकी गुणवत्ता और उसकी प्रवाह-शैली में पर्याप्त परिवर्तन हुआ सा दिखाई देता है । निश्चय ही यह कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं था । वस्तुतः साहित्य पर युग-चेतना का सर्वाधिक प्रभाव रहता है । और इस चेतना के फलस्वरूप साहित्य की शैली में, उसकी कलात्मक मान्यताओं में परिवर्तन दृग्गोचर होता है । गुप्त और वाकाटक साम्राज्यों की सर्वाङ्गीण उन्नति ने साहित्यिक वातावरण में आमल परविर्तन कर दिया । वाकाटक नृपतियों के राज्यकाल में ही प्राकृत भाषा और उसके साहित्य का उत्कर्ष प्रारम्भ हो चुका था । फलतः अब संस्कृत भाषा और उसके साहित्य का लक्ष्य जनसाधारण न रहकर विदग्ध समाज था । राजनैतिक दृष्टि से गुप्त साम्राज्य के पश्चात् भारतवर्ष टुकड़ों में विभक्त हो गया था । कनौज के हर्षवर्धन और चालुक्य पुलकेशी ने साम्राज्य की स्थापना की थी, किन्तु वे साम्राज्य चिरस्थायी न हो सके थे । सामन्तों तथा पण्डितों ने शास्त्रार्थों, अर्थालङ्कारों, शब्दालङ्कारों, प्रहेलिकादि काव्यों में आनन्द लेना प्रारम्भ कर दिया था । इसी समय एक ओर दिङ्नाग तथा धर्मकीर्ति जैसे बौद्ध पण्डितों का और वात्स्यायन तथा उद्योतकर जैसे ब्राह्मण नैयायिकों का उदय हुआ, तो दूसरी ओर अलङ्कार और कथा साहित्य के आचार्य सुबन्धु, दण्डी और बाण ( ५५० ई० तथा ६५० ई० के मध्य में ) ने वासवदत्ता, दशकुमारचरित और कादम्बरी जैसे क्रमश: उत्कृष्ट ग्रन्थ लिखकर काव्य को अलङ्कृति की सीमा पर पहुंचा दिया और इसका चरमोत्कर्ष श्रीहर्ष के नैषध तथा उत्तरकालीन काव्यों में दिखाई पडा । फलतः अश्वघोष और कालिदास की ऋजुता, सरसता और अव्याज मनोहारिता के स्थान पर विदग्धता और आयास सिद्ध आलङ्कारिता ने स्थान ग्रहण किया । यद्यपि शास्त्र के अनुसार काव्य यश के लिए व्यवहारज्ञान के लिए लिखे जाते थे', अर्थात् जीवन की लगभग समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए काव्य लिखे जाते थे, पर अधिक बल कीर्ति-यश पाने पर ही दिया गया है। जो बहज्ञताजन्य थी । कवियों की यह कहकर प्रशंसा की गई है कि उनके यश: शरीर में जरा-मरण का भय नहीं होता । कीर्ति प्राप्त करने में राजा और उसकी राज्यसभा प्रधान सहायक साधन थे । इस प्रकार हम देखते हैं कि सामन्त युग का
१. काव्यं सद् दृष्टाऽर्थ प्रीतिकीर्तिहेतुत्वात् (काव्यालंकार ५। ५)