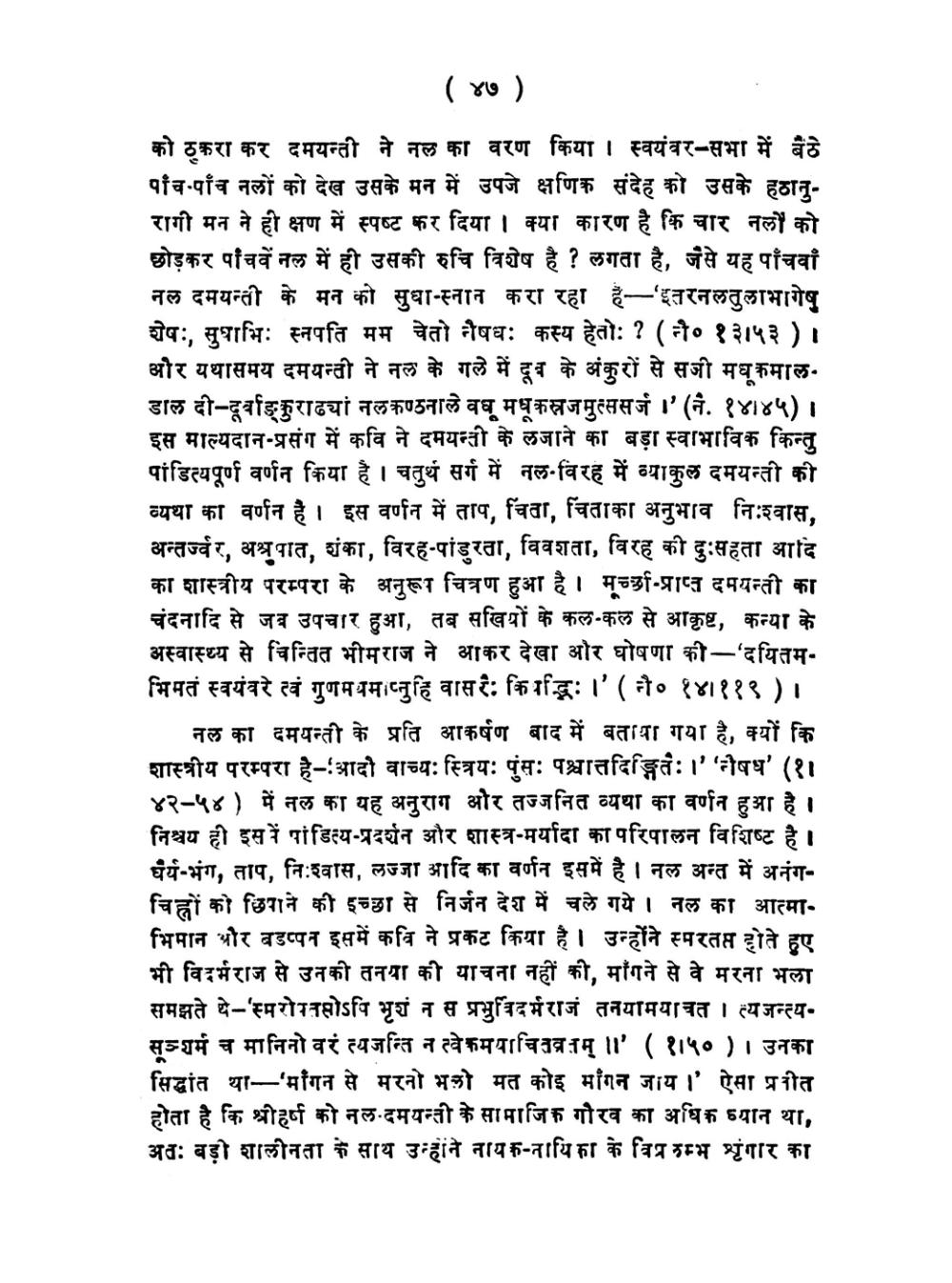________________
( ४७ ) को ठुकरा कर दमयन्ती ने नल का वरण किया। स्वयंवर-सभा में बैठे पांच-पाँच नलों को देख उसके मन में उपजे क्षणिक संदेह को उसके हठानुरागी मन ने ही क्षण में स्पष्ट कर दिया। क्या कारण है कि चार नलों को छोड़कर पांचवें नल में ही उसकी रुचि विशेष है ? लगता है, जैसे यह पाँचवाँ नल दमयन्ती के मन को सुधा-स्नान करा रहा है-'इतरनलतुलाभागेषु शेषः, सुधाभिः स्नपति मम चेतो नैषधः कस्य हेतोः ? (नै० १३१५३ )। और यथासमय दमयन्ती ने नल के गले में दूब के अंकुरों से सजी मधूकमाल. डाल दी-दूर्वाङ्कुराढयां नलकण्ठनाले वधू मधुकरजमुत्ससर्ज ।' (नं. १४।४५) । इस माल्यदान-प्रसंग में कवि ने दमयन्ती के लजाने का बड़ा स्वाभाविक किन्तु पांडित्यपूर्ण वर्णन किया है । चतुर्थ सर्ग में नल-विरह में व्याकुल दमयन्ती की व्यथा का वर्णन है। इस वर्णन में ताप, चिंता, चिताका अनुभाव निःश्वास, अन्तर्वर, अश्रुपात, शंका, विरह-पांडुरता, विवशता, विरह की दुःसहता आदि का शास्त्रीय परम्परा के अनुरूप चित्रण हुआ है। मूर्छा-प्राप्त दमयन्ती का चंदनादि से जब उपचार हुआ, तब सखियों के कल-कल से आकृष्ट, कन्या के अस्वास्थ्य से चिन्तित भीमराज ने आकर देखा और घोषणा की-'दयितमभिमतं स्वयंवरे त्वं गुणमयमाप्नुहि वासरः किद्भिः ।' (नै० १४।११९ )।
नल का दमयन्ती के प्रति आकर्षण बाद में बताया गया है, क्यों कि शास्त्रीय परम्परा है-:आदी वाच्यः स्त्रियः पुंसः पश्चात्तदिङ्गितः।' 'नैषध' (१॥ ४२-५४) में नल का यह अनुराग और तज्जनित व्यथा का वर्णन हुआ है। निश्चय ही इसमें पांडित्य-प्रदर्शन और शास्त्र-मर्यादा का परिपालन विशिष्ट है। घंर्य-भंग, ताप, नि:श्वास, लज्जा आदि का वर्णन इसमें है । नल अन्त में अनंगचिह्नों को छिपाने की इच्छा से निर्जन देश में चले गये। नल का आत्मा. भिमान और बडप्पन इसमें कवि ने प्रकट किया है। उन्होंने स्मरतप्त होते हए भी विदर्भराज से उनकी तनया की याचना नहीं की, मांगने से वे मरना भला समझते थे-'स्मरोग्ततोऽपि भृशं न स प्रभुविदर्भराजं तनयामयाचत । त्यजन्त्य. सञ्चर्म च मानिनो वरं त्यजन्ति न त्वेकमयाचितवतम् ।।' (११५०) । उनका सिद्धांत था-'मांगन से मरनो भलो मत कोइ मांगन जाय ।' ऐसा प्रतीत होता है कि श्रीहर्ष को नल-दमयन्ती के सामाजिक गौरव का अधिक ध्यान था, अतः बड़ो शालीनता के साथ उन्होंने नायक-नायिका के विप्र उम्भ शृंगार का