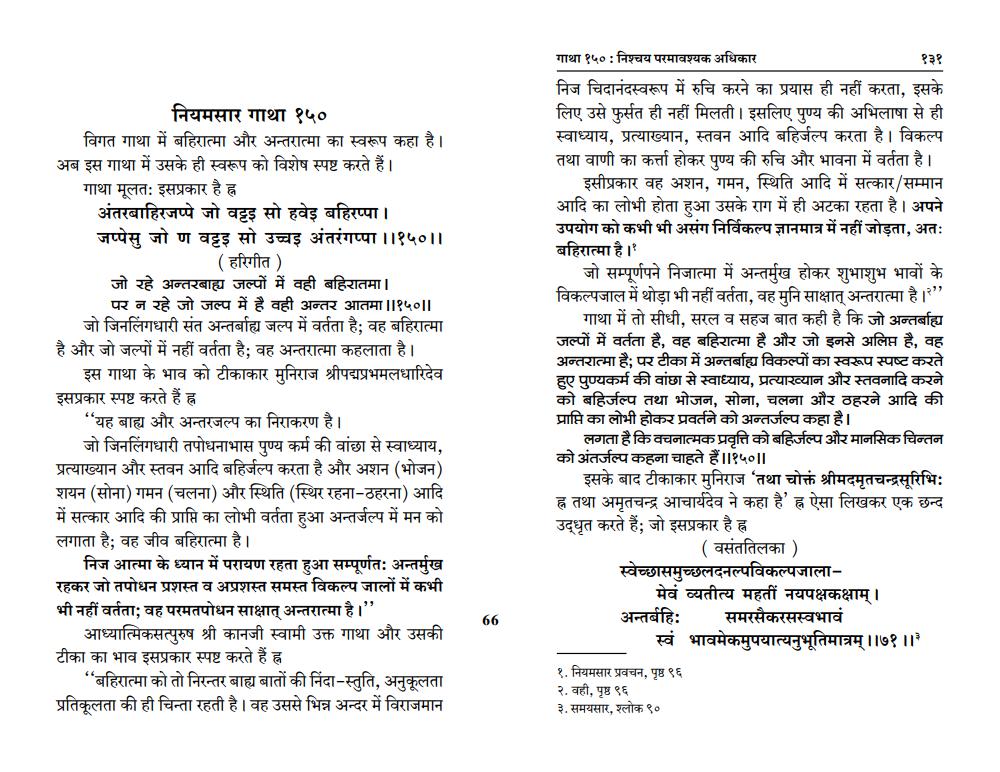________________
नियमसार गाथा १५०
विगत गाथा में बहिरात्मा और अन्तरात्मा का स्वरूप कहा है। अब इस गाथा में उसके ही स्वरूप को विशेष स्पष्ट करते हैं। गाथा मूलतः इसप्रकार है ह्र
अंतरबाहिरजप्पे जो वट्टइ सो हवेइ बहिरप्पा । जप्पे जो ण वट्टइ सो उच्चड़ अंतरंगप्पा ।। १५० ।। ( हरिगीत )
जो रहे अन्तरबाह्य जल्पों में वही बहिरातमा ।
पर न रहे जो जल्प में है वही अन्तर आतमा ||१५०|| जो जिनलिंगधारी संत अन्तर्बाह्य जल्प में वर्तता है; वह बहिरात्मा है और जो जल्पों में नहीं वर्तता है; वह अन्तरात्मा कहलाता है। इस गाथा के भाव को टीकाकार मुनिराज श्रीपद्मप्रभमलधारिदेव इसप्रकार स्पष्ट करते हैं ह्र
'यह बाह्य और अन्तरजल्प का निराकरण है।
जो जिनलिंगधारी तपोधनाभास पुण्य कर्म की वांछा से स्वाध्याय, प्रत्याख्यान और स्तवन आदि बहिर्जल्प करता है और अशन (भोजन) शयन (सोना) गमन (चलना) और स्थिति (स्थिर रहना - ठहरना) आदि में सत्कार आदि की प्राप्ति का लोभी वर्तता हुआ अन्तर्जल्प में मन को लगाता है; वह जीव बहिरात्मा है ।
निज आत्मा के ध्यान में परायण रहता हुआ सम्पूर्णत: अन्तर्मुख रहकर जो तपोधन प्रशस्त व अप्रशस्त समस्त विकल्प जालों में कभी भी नहीं वर्तता; वह परमतपोधन साक्षात् अन्तरात्मा है ।"
आध्यात्मिकसत्पुरुष श्री कानजी स्वामी उक्त गाथा और उसकी टीका का भाव इसप्रकार स्पष्ट करते हैं ह्र
"बहिरात्मा को तो निरन्तर बाह्य बातों की निंदा-स्तुति, अनुकूलता प्रतिकूलता की ही चिन्ता रहती है। वह उससे भिन्न अन्दर में विराजमान
66
गाथा १५० : निश्चय परमावश्यक अधिकार
१३१
निज चिदानंदस्वरूप में रुचि करने का प्रयास ही नहीं करता, इसके लिए उसे फुर्सत ही नहीं मिलती। इसलिए पुण्य की अभिलाषा से ही स्वाध्याय, प्रत्याख्यान, स्तवन आदि बहिर्जल्प करता है। विकल्प तथा वाणी का कर्त्ता होकर पुण्य की रुचि और भावना में वर्तता है।
इसीप्रकार वह अशन, गमन, स्थिति आदि में सत्कार / सम्मान आदि का लोभी होता हुआ उसके राग में ही अटका रहता है। अपने उपयोग को कभी भी असंग निर्विकल्प ज्ञानमात्र में नहीं जोड़ता, अतः बहिरात्मा है ।
जो सम्पूर्णपने निजात्मा में अन्तर्मुख होकर शुभाशुभ भावों के विकल्पजाल में थोड़ा भी नहीं वर्तता, वह मुनि साक्षात् अन्तरात्मा है। २"
गाथा में तो सीधी, सरल व सहज बात कही है कि जो अन्तर्बाह्य जल्पों में वर्तता है, वह बहिरात्मा है और जो इनसे अलिप्त है, वह अन्तरात्मा है; पर टीका में अन्तर्बाह्य विकल्पों का स्वरूप स्पष्ट करते हुए पुण्यकर्म की वांछा से स्वाध्याय, प्रत्याख्यान और स्तवनादि करने को बहिर्जल्प तथा भोजन, सोना, चलना और ठहरने आदि की प्राप्ति का लोभी होकर प्रवर्तने को अन्तर्जल्प कहा है।
लगता है कि वचनात्मक प्रवृत्ति को बहिर्जल्प और मानसिक चिन्तन को अंतर्जल्प कहना चाहते हैं ।। १५० ।।
इसके बाद टीकाकार मुनिराज 'तथा चोक्तं श्रीमदमृतचन्द्रसूरिभिः ह्न तथा अमृतचन्द्र आचार्यदेव ने कहा है' ह्र ऐसा लिखकर एक छन्द उद्धृत करते हैं; जो इसप्रकार है ह्र
( वसंततिलका ) स्वेच्छासमुच्छलदनल्पविकल्पजाला
मेवं व्यतीत्य महतीं नयपक्षकक्षाम् । अन्तर्बहिः समरसैकरसस्वभावं
स्वं भावमेकमुपयात्यनुभूतिमात्रम् ।। ७१ ।। *
१. नियमसार प्रवचन, पृष्ठ ९६
२. वही, पृष्ठ ९६
३. समयसार, श्लोक ९०