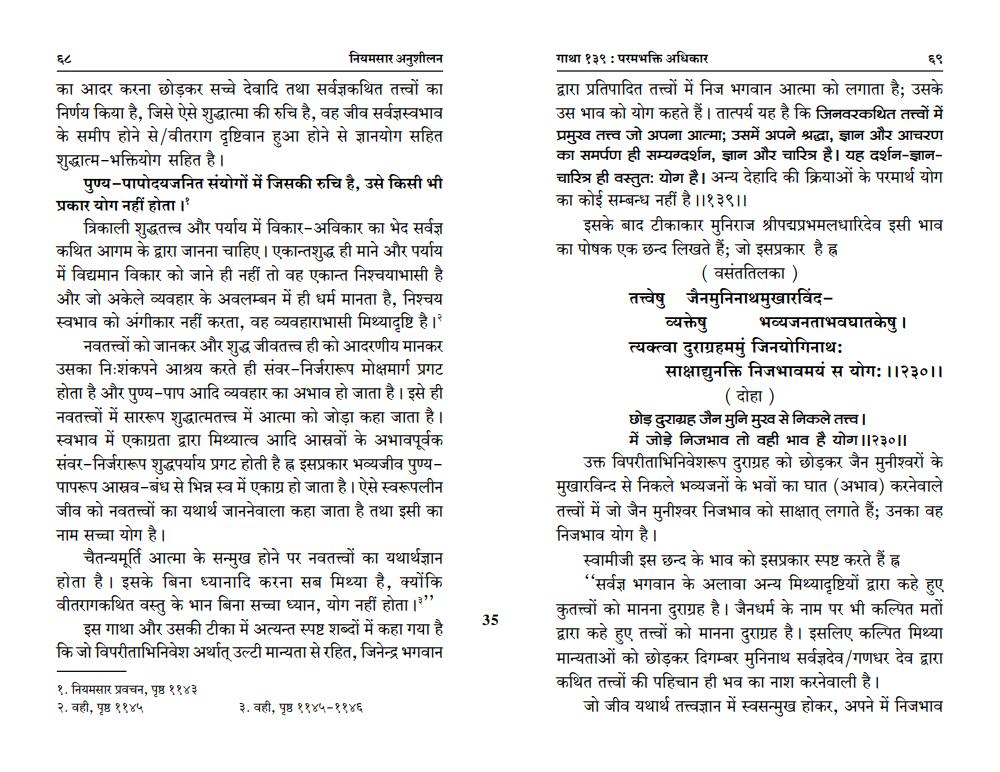________________
६८
नियमसार अनुशीलन का आदर करना छोड़कर सच्चे देवादि तथा सर्वज्ञकथित तत्त्वों का निर्णय किया है, जिसे ऐसे शुद्धात्मा की रुचि है, वह जीव सर्वज्ञस्वभाव के समीप होने से/वीतराग दृष्टिवान हुआ होने से ज्ञानयोग सहित शुद्धात्म-भक्तियोग सहित है।
पुण्य-पापोदयजनित संयोगों में जिसकी रुचि है, उसे किसी भी प्रकार योग नहीं होता
त्रिकाली शुद्धतत्त्व और पर्याय में विकार - अविकार का भेद सर्वज्ञ कथित आगम के द्वारा जानना चाहिए। एकान्तशुद्ध ही माने और पर्याय विद्यमान विकार को जाने ही नहीं तो वह एकान्त निश्चयाभासी है। और जो अकेले व्यवहार के अवलम्बन में ही धर्म मानता है, निश्चय स्वभाव को अंगीकार नहीं करता, वह व्यवहाराभासी मिथ्यादृष्टि है।
नवतत्त्वों को जानकर और शुद्ध जीवतत्त्व ही को आदरणीय मानकर उसका नि:शंकपने आश्रय करते ही संवर निर्जरारूप मोक्षमार्ग प्रगट होता है और पुण्य-पाप आदि व्यवहार का अभाव हो जाता है। इसे ही नवतत्त्वों में साररूप शुद्धात्मतत्त्व में आत्मा को जोड़ा कहा जाता है। स्वभाव में एकाग्रता द्वारा मिथ्यात्व आदि आस्रवों के अभावपूर्वक संवर-निर्जरारूप शुद्धपर्याय प्रगट होती है ह्र इसप्रकार भव्यजीव पुण्यपापरूप आस्रव-बंध से भिन्न स्व में एकाग्र हो जाता है। ऐसे स्वरूपलीन जीव को नवतत्त्वों का यथार्थ जाननेवाला कहा जाता है तथा इसी का नाम सच्चा योग है।
चैतन्यमूर्ति आत्मा के सन्मुख होने पर नवतत्त्वों का यथार्थज्ञान होता है । इसके बिना ध्यानादि करना सब मिथ्या है, क्योंकि वीतरागकथित वस्तु के भान बिना सच्चा ध्यान, योग नहीं होता । ३"
इस गाथा और उसकी टीका में अत्यन्त स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि जो विपरीताभिनिवेश अर्थात् उल्टी मान्यता से रहित, जिनेन्द्र भगवान
१. नियमसार प्रवचन, पृष्ठ ११४३ २. वही, पृष्ठ १९४५
३. वही, पृष्ठ १९४५-११४६
35
गाथा १३९ : परमभक्ति अधिकार
६९
द्वारा प्रतिपादित तत्त्वों में निज भगवान आत्मा को लगाता है; उसके उस भाव को योग कहते हैं। तात्पर्य यह है कि जिनवरकथित तत्त्वों में प्रमुख तत्त्व जो अपना आत्मा; उसमें अपने श्रद्धा, ज्ञान और आचरण का समर्पण ही सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र है । यह दर्शन-ज्ञानचारित्र ही वस्तुतः योग है। अन्य देहादि की क्रियाओं के परमार्थ योग का कोई सम्बन्ध नहीं है ।। १३९ ।।
इसके बाद टीकाकार मुनिराज श्रीपद्मप्रभमलधारिदेव इसी भाव का पोषक एक छन्द लिखते हैं; जो इसप्रकार है
(वसंततिलका) तत्त्वेषु जैनमुनिनाथमुखारविंद
व्यक्तेषु भव्यजनताभवघातकेषु । त्यक्त्वा दुराग्रहममुं जिनयोगिनाथ:
साक्षाद्युनक्ति निजभावमयं स योगः ।।२३० ।। (दोहा)
छोड़ दुराग्रह जैन मुनि मुख से निकले तत्त्व | में जोड़े निजभाव तो वही भाव है योग ||२३० ॥ उक्त विपरीताभिनिवेशरूप दुराग्रह को छोड़कर जैन मुनीश्वरों के मुखारविन्द से निकले भव्यजनों के भवों का घात (अभाव) करनेवाले तत्त्वों में जो जैन मुनीश्वर निजभाव को साक्षात् लगाते हैं; उनका वह निजभाव योग है।
स्वामीजी इस छन्द के भाव को इसप्रकार स्पष्ट करते हैं ह्र
"सर्वज्ञ भगवान के अलावा अन्य मिथ्यादृष्टियों द्वारा कहे हुए कुतत्त्वों को मानना दुराग्रह है। जैनधर्म के नाम पर भी कल्पित मतों द्वारा कहे हुए तत्त्वों को मानना दुराग्रह है । इसलिए कल्पित मिथ्या मान्यताओं को छोड़कर दिगम्बर मुनिनाथ सर्वज्ञदेव / गणधर देव द्वारा कथित तत्त्वों की पहिचान ही भव का नाश करनेवाली है।
जो जीव यथार्थ तत्त्वज्ञान में स्वसन्मुख होकर, अपने में निजभाव