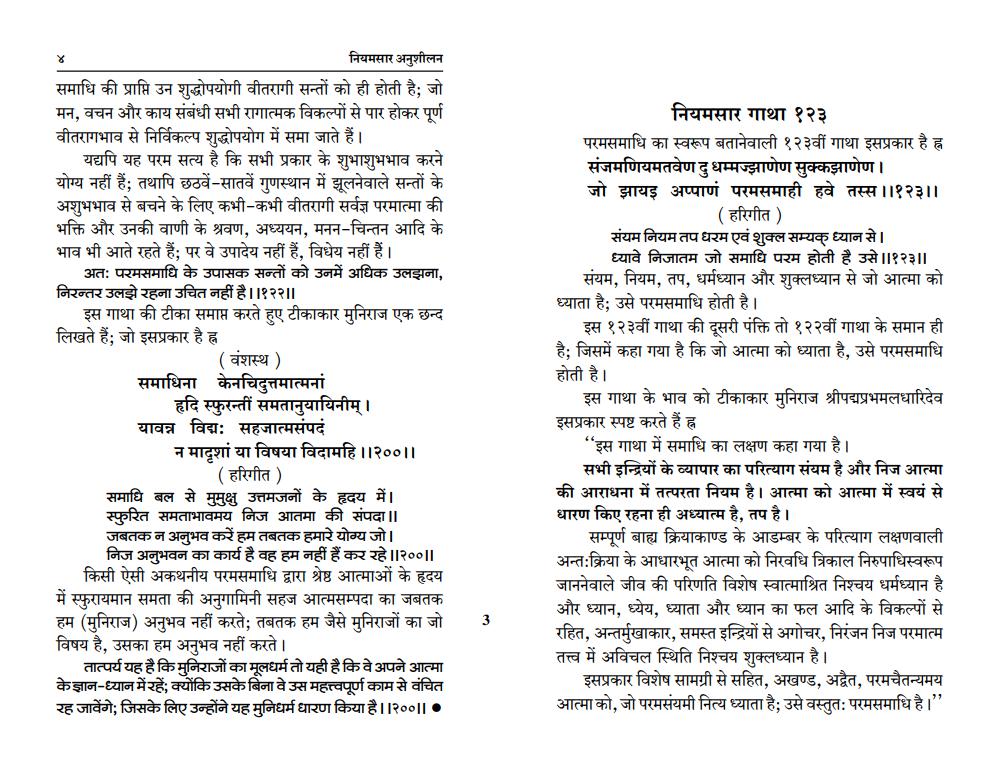________________
नियमसार अनुशीलन समाधि की प्राप्ति उन शुद्धोपयोगी वीतरागी सन्तों को ही होती है; जो मन, वचन और काय संबंधी सभी रागात्मक विकल्पों से पार होकर पूर्ण वीतरागभाव से निर्विकल्प शुद्धोपयोग में समा जाते हैं।
यद्यपि यह परम सत्य है कि सभी प्रकार के शुभाशुभभाव करने योग्य नहीं हैं; तथापि छठवें सातवें गुणस्थान में झूलनेवाले सन्तों के शुभभाव से बचने के लिए कभी-कभी वीतरागी सर्वज्ञ परमात्मा की भक्ति और उनकी वाणी के श्रवण, अध्ययन, मनन- चिन्तन आदि के भाव भी आते रहते हैं; पर वे उपादेय नहीं हैं, विधेय नहीं हैं।
४
अतः परमसमाधि के उपासक सन्तों को उनमें अधिक उलझना, निरन्तर उलझे रहना उचित नहीं है । । १२२ ।।
इस गाथा की टीका समाप्त करते हुए टीकाकार मुनिराज एक छन्द लिखते हैं; जो इसप्रकार है ह्र
( वंशस्थ ) समाधिना केनचिदुत्तमात्मनां हृदि स्फुरन्तीं समतानुयायिनीम् । यावन्न विद्मः सहजात्मसंपदं
न मादृशां या विषया विदामहि ।। २०० ।। ( हरिगीत )
समाधि बल से मुमुक्षु उत्तमजनों के हृदय में । स्फुरित समताभावमय निज आतमा की संपदा || जबतक न अनुभव करें हम तबतक हमारे योग्य जो।
निज अनुभवन का कार्य है वह हम नहीं हैं कर रहे ॥ २००॥
किसी ऐसी अकथनीय परमसमाधि द्वारा श्रेष्ठ आत्माओं के हृदय में स्फुरायमान समता की अनुगामिनी सहज आत्मसम्पदा का जबतक हम (मुनिराज ) अनुभव नहीं करते; तबतक हम जैसे मुनिराजों का जो विषय है, उसका हम अनुभव नहीं करते ।
तात्पर्य यह है कि मुनिराजों का मूलधर्म तो यही है कि वे अपने म के ज्ञान-ध्यान में रहें; क्योंकि उसके बिना वे उस महत्त्वपूर्ण काम रह जायेंगे; जिसके लिए उन्होंने यह मुनिधर्म धारण किया है । । २०० ॥ •
3
नियमसार गाथा १२३
परमसमाधि का स्वरूप बतानेवाली १२३वीं गाथा इसप्रकार है ह्र संजमणियमतवेण दु धम्मज्झाणेण सुक्कझाणेण ।
जो झायइ अप्पाणं परमसमाही हवे तस्स ।। १२३ ।। ( हरिगीत )
संयम नियम तप धरम एवं शुक्ल सम्यक् ध्यान से ।
ध्यावे निजातम जो समाधि परम होती है उसे ।। १२३ ।। संयम, नियम, तप, धर्मध्यान और शुक्लध्यान से जो आत्मा को ध्याता है; उसे परमसमाधि होती है।
इस १२३वीं गाथा की दूसरी पंक्ति तो १२२वीं गाथा के समान ही है; जिसमें कहा गया है कि जो आत्मा को ध्याता है, उसे परमसमाधि होती है।
इस गाथा के भाव को टीकाकार मुनिराज श्रीपद्मप्रभमलधारिदेव इसप्रकार स्पष्ट करते हैं
" इस गाथा में समाधि का लक्षण कहा गया है।
सभी इन्द्रियों के व्यापार का परित्याग संयम है और निज आत्मा की आराधना में तत्परता नियम है। आत्मा को आत्मा में स्वयं से धारण किए रहना ही अध्यात्म है, तप है ।
सम्पूर्ण बाह्य क्रियाकाण्ड के आडम्बर के परित्याग लक्षणवाली अन्तःक्रिया के आधारभूत आत्मा को निरवधि त्रिकाल निरुपाधिस्वरूप जाननेवाले जीव की परिणति विशेष स्वात्माश्रित निश्चय धर्मध्यान है और ध्यान, ध्येय, ध्याता और ध्यान का फल आदि के विकल्पों से रहित, अन्तर्मुखाकार, समस्त इन्द्रियों से अगोचर, निरंजन निज परमात्म तत्त्व में अविचल स्थिति निश्चय शुक्लध्यान है।
इसप्रकार विशेष सामग्री से सहित, अखण्ड, अद्वैत, परमचैतन्यमय आत्मा को, जो परमसंयमी नित्य ध्याता है; उसे वस्तुतः परमसमाधि है।”