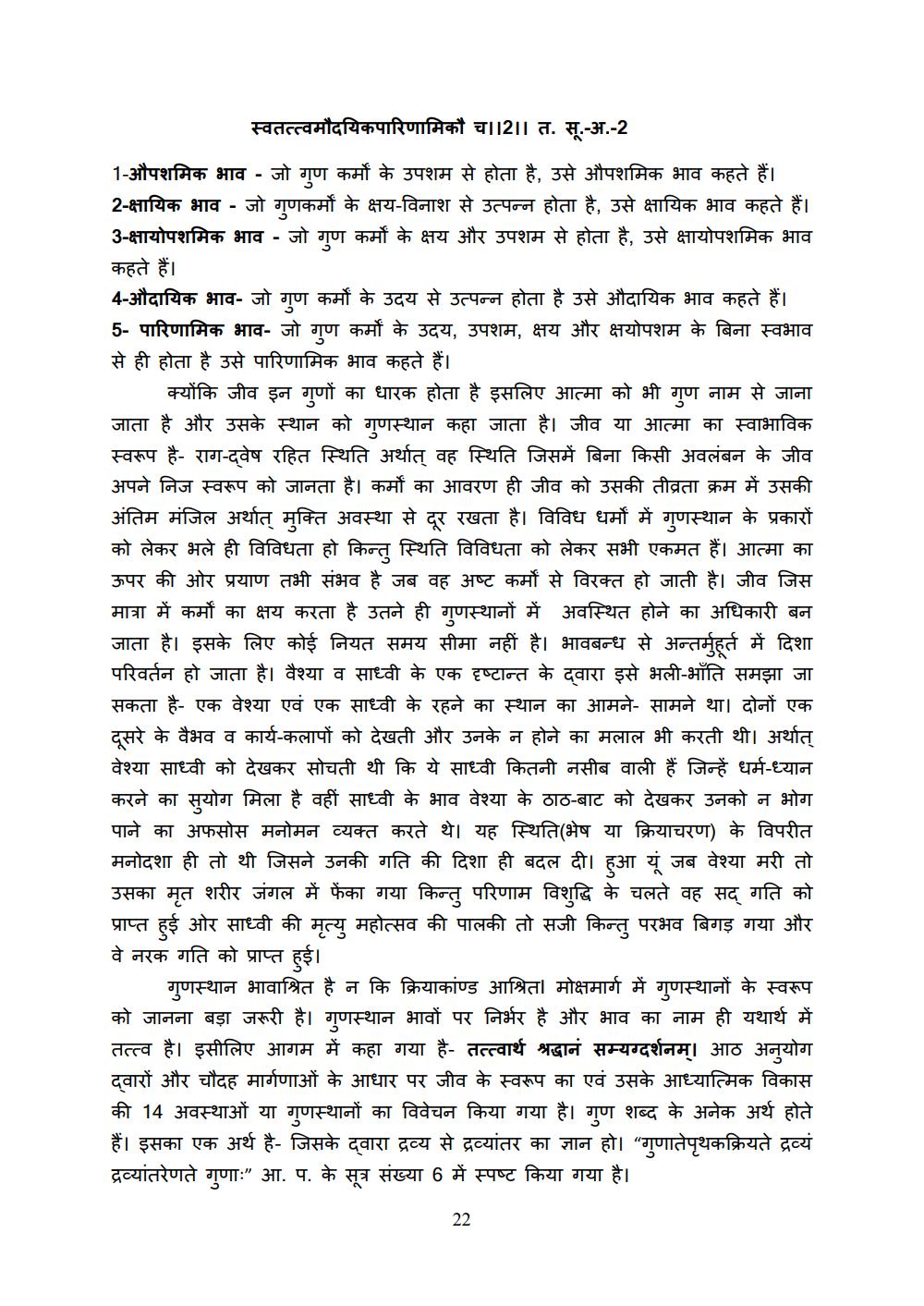________________
स्वतत्त्वमौदयिकपारिणामिको च।।2।। त. सू.-अ.-2 1-औपशमिक भाव - जो गुण कर्मों के उपशम से होता है, उसे औपशमिक भाव कहते हैं। 2-क्षायिक भाव - जो गुणकर्मों के क्षय-विनाश से उत्पन्न होता है, उसे क्षायिक भाव कहते हैं। 3-क्षायोपशमिक भाव - जो गुण कर्मों के क्षय और उपशम से होता है, उसे क्षायोपशमिक भाव कहते हैं। 4-औदायिक भाव- जो गुण कर्मों के उदय से उत्पन्न होता है उसे औदायिक भाव कहते हैं। 5- पारिणामिक भाव- जो गुण कर्मों के उदय, उपशम, क्षय और क्षयोपशम के बिना स्वभाव से ही होता है उसे पारिणामिक भाव कहते हैं।
क्योंकि जीव इन गुणों का धारक होता है इसलिए आत्मा को भी गुण नाम से जाना जाता है और उसके स्थान को गुणस्थान कहा जाता है। जीव या आत्मा का स्वाभाविक स्वरूप है- राग-दवेष रहित स्थिति अर्थात् वह स्थिति जिसमें बिना किसी अवलंबन के जीव अपने निज स्वरूप को जानता है। कर्मों का आवरण ही जीव को उसकी तीव्रता क्रम में उसकी अंतिम मंजिल अर्थात् मुक्ति अवस्था से दूर रखता है। विविध धर्मों में गुणस्थान के प्रकारों को लेकर भले ही विविधता हो किन्तु स्थिति विविधता को लेकर सभी एकमत हैं। आत्मा का
की ओर प्रयाण तभी संभव है जब वह अष्ट कर्मों से विरक्त हो जाती है। जीव जिस मात्रा में कर्मों का क्षय करता है उतने ही गुणस्थानों में अवस्थित होने का अधिकारी बन
है। इसके लिए कोई नियत समय सीमा नहीं है। भावबन्ध से अन्तर्महर्त में दिशा परिवर्तन हो जाता है। वैश्या व साध्वी के एक दृष्टान्त के द्वारा इसे भली-भाँति समझा जा सकता है- एक वेश्या एवं एक साध्वी के रहने का स्थान का आमने- सामने था। दोनों एक दुसरे के वैभव व कार्य-कलापों को देखती और उनके न होने का मलाल भी करती थी। अर्थात वेश्या साध्वी को देखकर सोचती थी कि ये साध्वी कितनी नसीब वाली हैं जिन्हें धर्म-ध्यान करने का सुयोग मिला है वहीं साध्वी के भाव वेश्या के ठाठ-बाट को देखकर उनको न भोग पाने का अफसोस मनोमन व्यक्त करते थे। यह स्थिति(भेष या क्रियाचरण) के विपरीत मनोदशा ही तो थी जिसने उनकी गति की दिशा ही बदल दी। हआ यं जब वेश्या मरी तो उसका मृत शरीर जंगल में फेंका गया किन्तु परिणाम विशुद्धि के चलते वह सद् गति को प्राप्त हुई ओर साध्वी की मृत्यु महोत्सव की पालकी तो सजी किन्तु परभव बिगड़ गया और वे नरक गति को प्राप्त हुई।
____ गुणस्थान भावाश्रित है न कि क्रियाकांण्ड आश्रित| मोक्षमार्ग में गुणस्थानों के स्वरूप को जानना बड़ा जरूरी है। गुणस्थान भावों पर निर्भर है और भाव का नाम ही यथार्थ में तत्त्व है। इसीलिए आगम में कहा गया है- तत्त्वार्थ श्रद्धानं सम्यग्दर्शनम्। आठ अनुयोग द्वारों और चौदह मार्गणाओं के आधार पर जीव के स्वरूप का एवं उसके आध्यात्मिक विकास की 14 अवस्थाओं या गुणस्थानों का विवेचन किया गया है। गुण शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। इसका एक अर्थ है- जिसके द्वारा द्रव्य से द्रव्यांतर का ज्ञान हो। “गुणातेपृथकक्रियते द्रव्यं द्रव्यांतरेणते गुणाः” आ. प. के सूत्र संख्या 6 में स्पष्ट किया गया है।
22