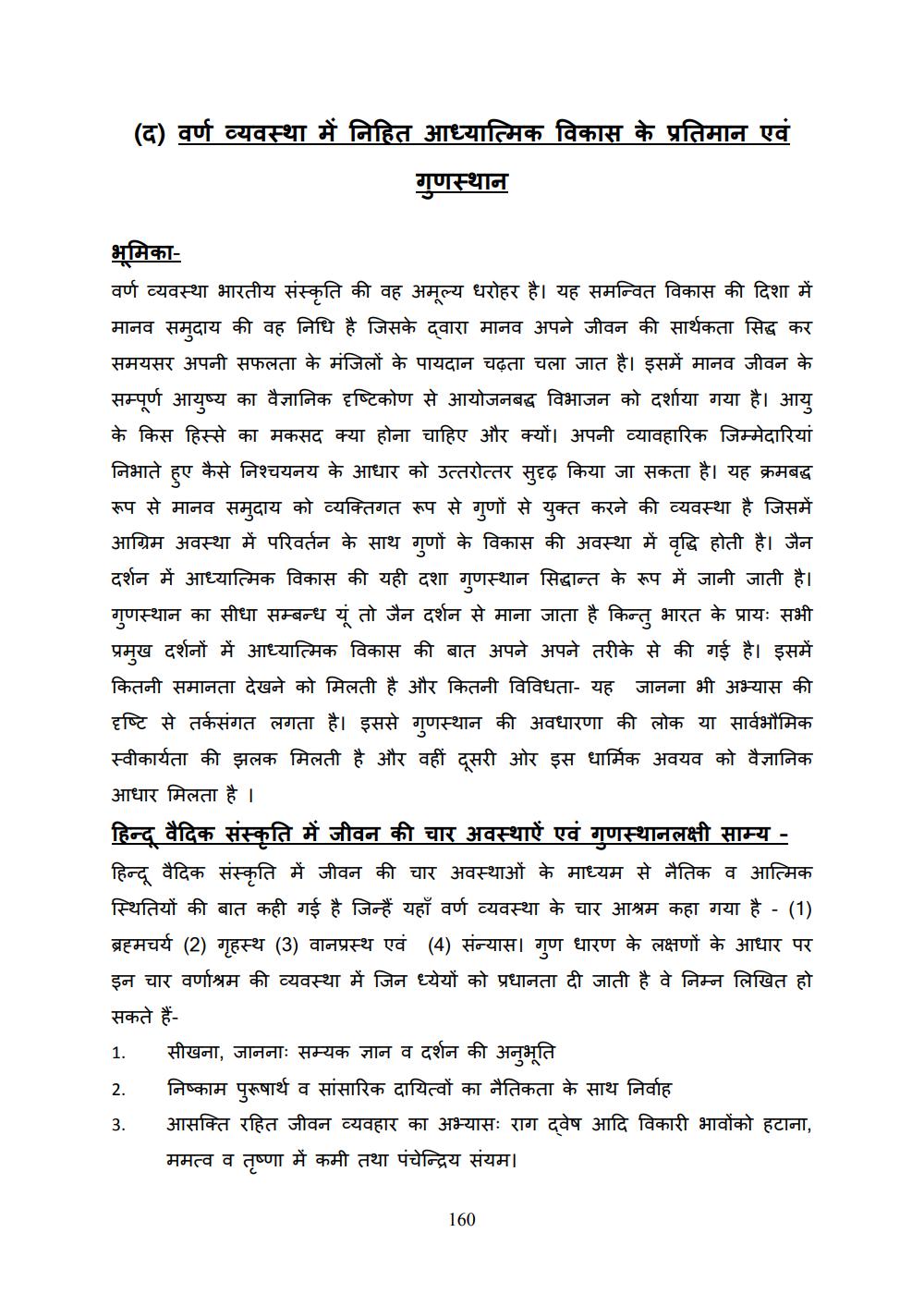________________
(द) वर्ण व्यवस्था में निहित आध्यात्मिक विकास के प्रतिमान एवं
गुणस्थान
भमिकावर्ण व्यवस्था भारतीय संस्कृति की वह अमूल्य धरोहर है। यह समन्वित विकास की दिशा में मानव समुदाय की वह निधि है जिसके द्वारा मानव अपने जीवन की सार्थकता सिद्ध कर समयसर अपनी सफलता के मंजिलों के पायदान चढ़ता चला जात है। इसमें मानव जीवन के सम्पूर्ण आयुष्य का वैज्ञानिक दृष्टिकोण से आयोजनबद्ध विभाजन को दर्शाया गया है। आयु के किस हिस्से का मकसद क्या होना चाहिए और क्यों। अपनी व्यावहारिक जिम्मेदारियां निभाते हुए कैसे निश्चयनय के आधार को उत्तरोत्तर सुदृढ़ किया जा सकता है। यह क्रमबद्ध रूप से मानव समुदाय को व्यक्तिगत रूप से गुणों से युक्त करने की व्यवस्था है जिसमें आग्रिम अवस्था में परिवर्तन के साथ गुणों के विकास की अवस्था में वृद्धि होती है। जैन दर्शन में आध्यात्मिक विकास की यही दशा गुणस्थान सिद्धान्त के रूप में जानी जाती है। गुणस्थान का सीधा सम्बन्ध यूं तो जैन दर्शन से माना जाता है किन्तु भारत के प्रायः सभी प्रमुख दर्शनों में आध्यात्मिक विकास की बात अपने अपने तरीके से की गई है। इसमें कितनी समानता देखने को मिलती है और कितनी विविधता- यह जानना भी अभ्यास की दृष्टि से तर्कसंगत लगता है। इससे गुणस्थान की अवधारणा की लोक या सार्वभौमिक स्वीकार्यता की झलक मिलती है और वहीं दूसरी ओर इस धार्मिक अवयव को वैज्ञानिक आधार मिलता है । हिन्दू वैदिक संस्कृति में जीवन की चार अवस्थाएं एवं गणस्थानलक्षी साम्य - हिन्दू वैदिक संस्कृति में जीवन की चार अवस्थाओं के माध्यम से नैतिक व आत्मिक स्थितियों की बात कही गई है जिन्हें यहाँ वर्ण व्यवस्था के चार आश्रम कहा गया है - (1) ब्रह्मचर्य (2) गृहस्थ (3) वानप्रस्थ एवं (4) संन्यास। गुण धारण के लक्षणों के आधार पर इन चार वर्णाश्रम की व्यवस्था में जिन ध्येयों को प्रधानता दी जाती है वे निम्न लिखित हो सकते हैं1. सीखना, जाननाः सम्यक ज्ञान व दर्शन की अनुभूति 2. निष्काम पुरूषार्थ व सांसारिक दायित्वों का नैतिकता के साथ निर्वाह
आसक्ति रहित जीवन व्यवहार का अभ्यासः राग दवेष आदि विकारी भावोंको हटाना, ममत्व व तृष्णा में कमी तथा पंचेन्द्रिय संयम।
ल
160