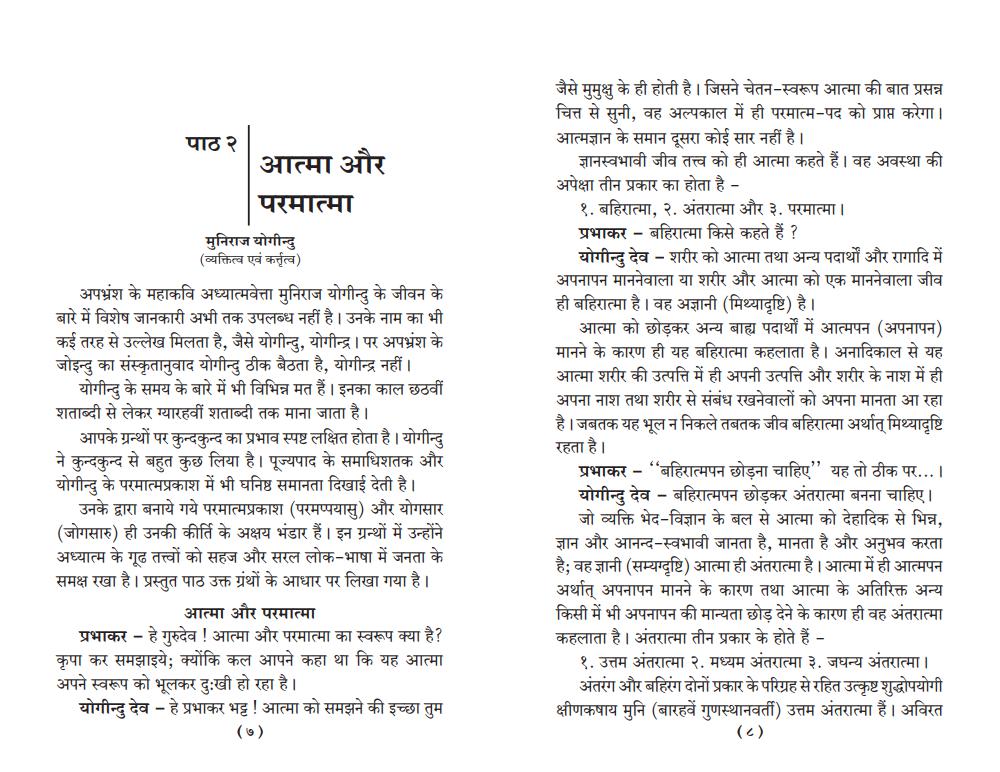________________
पाठ २
आत्मा और परमात्मा
मुनिराज योगीन्दु (व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व)
अपभ्रंश के महाकवि अध्यात्मवेत्ता मुनिराज योगीन्दु के जीवन के बारे में विशेष जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं है। उनके नाम का भी कई तरह से उल्लेख मिलता है, जैसे योगीन्दु, योगीन्द्र । पर अपभ्रंश के जोइन्दु का संस्कृतानुवाद योगीन्दु ठीक बैठता है, योगीन्द्र नहीं।
योगीन्दु के समय के बारे में भी विभिन्न मत हैं। इनका काल छठवीं शताब्दी से लेकर ग्यारहवीं शताब्दी तक माना जाता है।
आपके ग्रन्थों पर कुन्दकुन्द का प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता है। योगीन्दु ने कुन्दकुन्द से बहुत कुछ लिया है। पूज्यपाद के समाधिशतक और योगीन्दु के परमात्मप्रकाश में भी घनिष्ठ समानता दिखाई देती है।
उनके द्वारा बनाये गये परमात्मप्रकाश (परमप्पयासु) और योगसार (जोगसारु) ही उनकी कीर्ति के अक्षय भंडार हैं। इन ग्रन्थों में उन्होंने अध्यात्म के गूढ तत्त्वों को सहज और सरल लोक-भाषा में जनता के समक्ष रखा है। प्रस्तुत पाठ उक्त ग्रंथों के आधार पर लिखा गया है।
आत्मा और परमात्मा प्रभाकर - हे गुरुदेव ! आत्मा और परमात्मा का स्वरूप क्या है? कृपा कर समझाइये; क्योंकि कल आपने कहा था कि यह आत्मा अपने स्वरूप को भूलकर दुःखी हो रहा है। योगीन्दु देव - हे प्रभाकर भट्ट ! आत्मा को समझने की इच्छा तुम
जैसे मुमुक्षु के ही होती है। जिसने चेतन-स्वरूप आत्मा की बात प्रसन्न चित्त से सुनी, वह अल्पकाल में ही परमात्म-पद को प्राप्त करेगा। आत्मज्ञान के समान दूसरा कोई सार नहीं है।
ज्ञानस्वभावी जीव तत्त्व को ही आत्मा कहते हैं। वह अवस्था की अपेक्षा तीन प्रकार का होता है -
१. बहिरात्मा, २. अंतरात्मा और ३. परमात्मा । प्रभाकर - बहिरात्मा किसे कहते हैं ?
योगीन्दु देव - शरीर को आत्मा तथा अन्य पदार्थों और रागादि में अपनापन माननेवाला या शरीर और आत्मा को एक माननेवाला जीव ही बहिरात्मा है। वह अज्ञानी (मिथ्यादृष्टि) है। ___ आत्मा को छोड़कर अन्य बाह्य पदार्थों में आत्मपन (अपनापन) मानने के कारण ही यह बहिरात्मा कहलाता है। अनादिकाल से यह आत्मा शरीर की उत्पत्ति में ही अपनी उत्पत्ति और शरीर के नाश में ही अपना नाश तथा शरीर से संबंध रखनेवालों को अपना मानता आ रहा है। जबतक यह भूल न निकले तबतक जीव बहिरात्मा अर्थात् मिथ्यादृष्टि रहता है।
प्रभाकर - "बहिरात्मपन छोड़ना चाहिए" यह तो ठीक पर...। योगीन्दु देव - बहिरात्मपन छोड़कर अंतरात्मा बनना चाहिए।
जो व्यक्ति भेद-विज्ञान के बल से आत्मा को देहादिक से भिन्न, ज्ञान और आनन्द-स्वभावी जानता है, मानता है और अनुभव करता है; वह ज्ञानी (सम्यग्दृष्टि) आत्मा ही अंतरात्मा है। आत्मा में ही आत्मपन अर्थात् अपनापन मानने के कारण तथा आत्मा के अतिरिक्त अन्य किसी में भी अपनापन की मान्यता छोड़ देने के कारण ही वह अंतरात्मा कहलाता है। अंतरात्मा तीन प्रकार के होते हैं -
१. उत्तम अंतरात्मा २. मध्यम अंतरात्मा ३. जघन्य अंतरात्मा।
अंतरंग और बहिरंग दोनों प्रकार के परिग्रह से रहित उत्कृष्ट शुद्धोपयोगी क्षीणकषाय मुनि (बारहवें गुणस्थानवर्ती) उत्तम अंतरात्मा हैं। अविरत
(८)