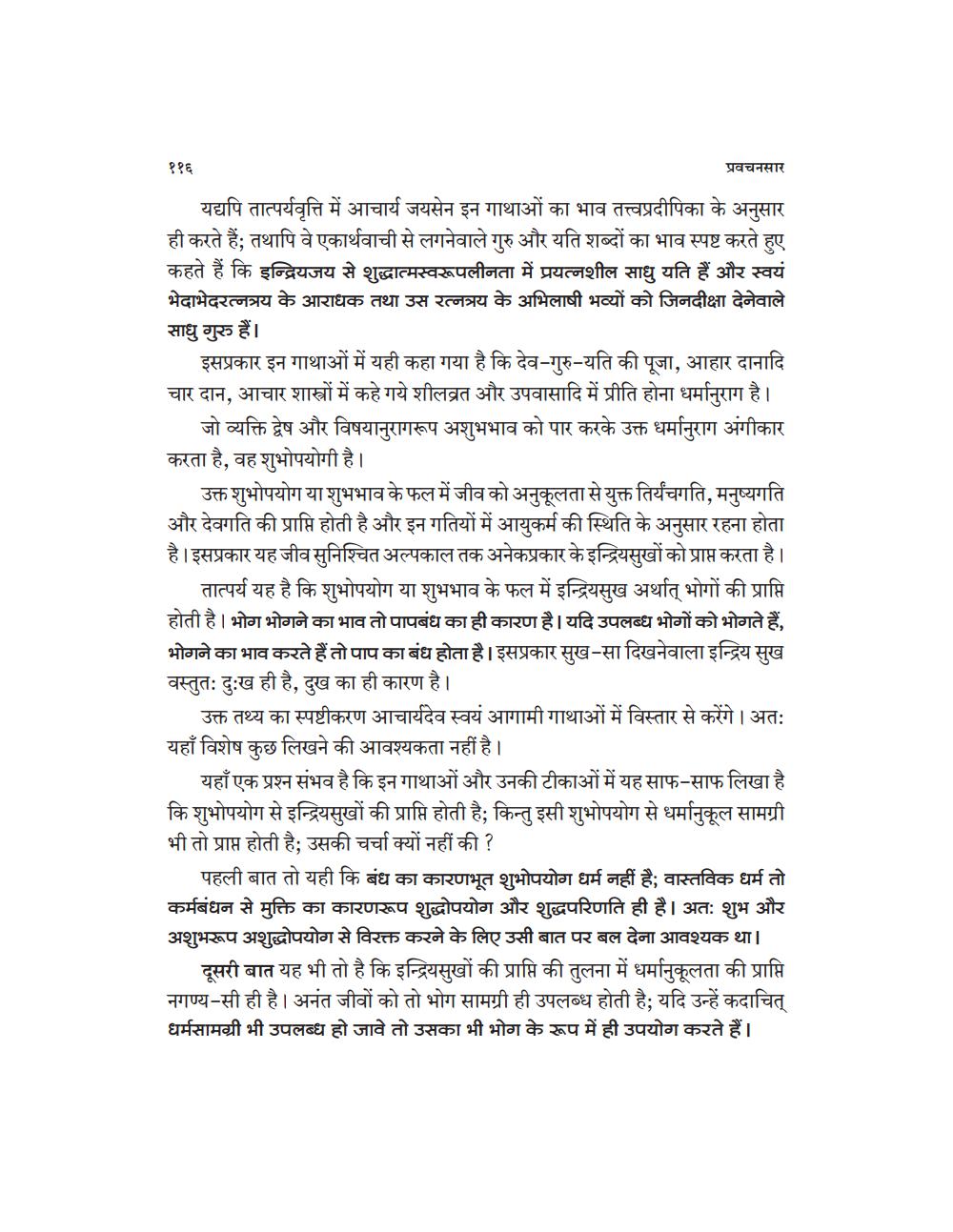________________
११६
प्रवचनसार
यद्यपि तात्पर्यवृत्ति में आचार्य जयसेन इन गाथाओं का भाव तत्त्वप्रदीपिका के अनुसार ही करते हैं; तथापि वे एकार्थवाची से लगनेवाले गुरु और यति शब्दों का भाव स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि इन्द्रियजय से शुद्धात्मस्वरूपलीनता में प्रयत्नशील साधु यति हैं और स्वयं भेदाभेदरत्नत्रय के आराधक तथा उस रत्नत्रय के अभिलाषी भव्यों को जिनदीक्षा देनेवाले साधु गुरु हैं।
इसप्रकार इन गाथाओं में यही कहा गया है कि देव-गुरु-यति की पूजा, आहार दानादि चार दान, आचार शास्त्रों में कहे गये शीलव्रत और उपवासादि में प्रीति होना धर्मानुराग है। जो व्यक्ति द्वेष और विषयानुरागरूप अशुभभाव को पार करके उक्त धर्मानुराग अंगीकार करता है, वह शुभोपयोगी है।
उक्त शुभोपयोग या शुभभाव के फल में जीव को अनुकूलता से युक्त तिर्यंचगति, मनुष्यगति और देवगति की प्राप्ति होती है और इन गतियों में आयुकर्म की स्थिति के अनुसार रहना होता । इसप्रकार यह जीव सुनिश्चित अल्पकाल तक अनेकप्रकार के इन्द्रियसुखों को प्राप्त करता है।
तात्पर्य यह है कि शुभोपयोग या शुभभाव के फल में इन्द्रियसुख अर्थात् भोगों की प्राप्ति होती है । भोग भोगने का भाव तो पापबंध का ही कारण है। यदि उपलब्ध भोगों को भोगते हैं, भोगने का भाव करते हैं तो पाप का बंध होता है। इसप्रकार सुख-सा दिखनेवाला इन्द्रिय सुख वस्तुतः दुःख ही है, दुख का ही कारण है।
उक्त तथ्य का स्पष्टीकरण आचार्यदेव स्वयं आगामी गाथाओं में विस्तार से करेंगे । अतः यहाँ विशेष कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है ।
यहाँ एक प्रश्न संभव है कि इन गाथाओं और उनकी टीकाओं में यह साफ-साफ लिखा है कि शुभोपयोग से इन्द्रियसुखों की प्राप्ति होती है; किन्तु इसी शुभोपयोग से धर्मानुकूल सामग्री भी तो प्राप्त होती है; उसकी चर्चा क्यों नहीं की ?
पहली बात तो यही कि बंध का कारणभूत शुभोपयोग धर्म नहीं है; वास्तविक धर्म तो कर्मबंधन से मुक्ति का कारणरूप शुद्धोपयोग और शुद्धपरिणति ही है । अतः शुभ और अशुभरूप अशुद्धोपयोग से विरक्त करने के लिए उसी बात पर बल देना आवश्यक था।
दूसरी बात यह भी तो है कि इन्द्रियसुखों की प्राप्ति की तुलना में धर्मानुकूलता की प्राप्ति नगण्य -सी ही है। अनंत जीवों को तो भोग सामग्री ही उपलब्ध होती है; यदि उन्हें कदाचित् धर्मसामग्री भी उपलब्ध हो जावे तो उसका भी भोग के रूप में ही उपयोग करते हैं।