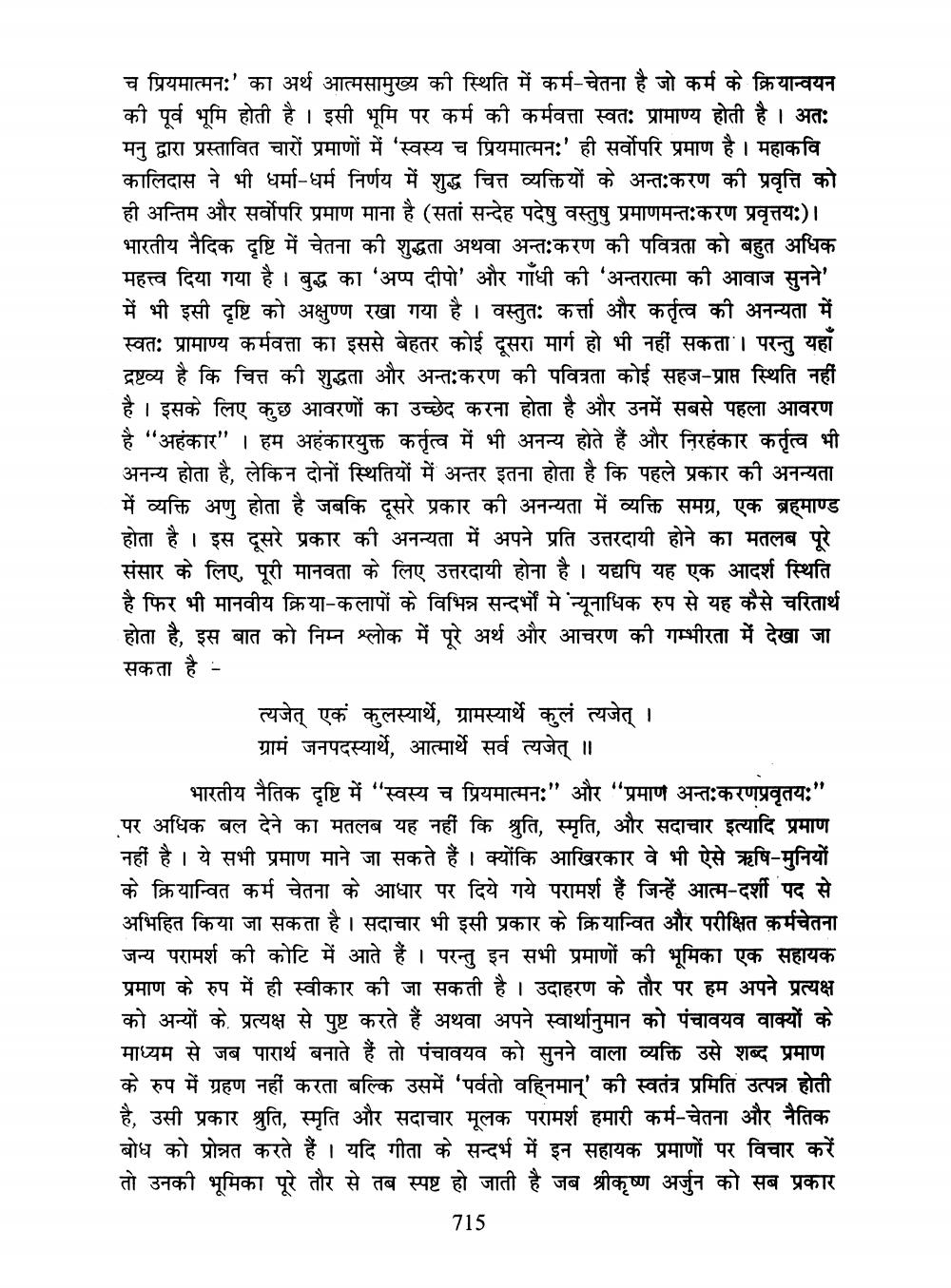________________
च प्रियमात्मनः' का अर्थ आत्मसामुख्य की स्थिति में कर्म-चेतना है जो कर्म के क्रियान्वयन की पूर्व भूमि होती है । इसी भूमि पर कर्म की कर्मवत्ता स्वतः प्रामाण्य होती है । अतः मनु द्वारा प्रस्तावित चारों प्रमाणों में 'स्वस्य च प्रियमात्मनः' ही सर्वोपरि प्रमाण है। महाकवि कालिदास ने भी धर्मा-धर्म निर्णय में शुद्ध चित्त व्यक्तियों के अन्तःकरण की प्रवृत्ति को ही अन्तिम और सर्वोपरि प्रमाण माना है (सतां सन्देह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरण प्रवृत्तयः)। भारतीय नैदिक दृष्टि में चेतना की शुद्धता अथवा अन्तःकरण की पवित्रता को बहुत अधिक महत्त्व दिया गया है । बुद्ध का 'अप्प दीपो' और गाँधी की 'अन्तरात्मा की आवाज सुनने' में भी इसी दृष्टि को अक्षुण्ण रखा गया है । वस्तुतः कर्ता और कर्तृत्व की अनन्यता में स्वतः प्रामाण्य कर्मवत्ता का इससे बेहतर कोई दूसरा मार्ग हो भी नहीं सकता। परन्तु यहाँ द्रष्टव्य है कि चित्त की शुद्धता और अन्तःकरण की पवित्रता कोई सहज-प्राप्त स्थिति नहीं है । इसके लिए कुछ आवरणों का उच्छेद करना होता है और उनमें सबसे पहला आवरण है "अहंकार" । हम अहंकारयुक्त कर्तृत्व में भी अनन्य होते हैं और निरहंकार कर्तृत्व भी अनन्य होता है, लेकिन दोनों स्थितियों में अन्तर इतना होता है कि पहले प्रकार की अनन्यता में व्यक्ति अणु होता है जबकि दूसरे प्रकार की अनन्यता में व्यक्ति समग्र, एक ब्रह्माण्ड होता है । इस दूसरे प्रकार की अनन्यता में अपने प्रति उत्तरदायी होने का मतलब पूरे संसार के लिए, पूरी मानवता के लिए उत्तरदायी होना है । यद्यपि यह एक आदर्श स्थिति है फिर भी मानवीय क्रिया-कलापों के विभिन्न सन्दर्भो में न्यूनाधिक रुप से यह कैसे चरितार्थ होता है, इस बात को निम्न श्लोक में पूरे अर्थ और आचरण की गम्भीरता में देखा जा सकता है -
त्यजेत् एकं कुलस्यार्थे, ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत् ।
ग्रामं जनपदस्यार्थे, आत्मार्थे सर्व त्यजेत् ॥ भारतीय नैतिक दृष्टि में "स्वस्य च प्रियमात्मनः" और "प्रमाण अन्तःकरणप्रवृतयः" पर अधिक बल देने का मतलब यह नहीं कि श्रुति, स्मृति, और सदाचार इत्यादि प्रमाण नहीं है। ये सभी प्रमाण माने जा सकते हैं। क्योंकि आखिरकार वे भी ऐसे ऋषि-मुनियों के क्रियान्वित कर्म चेतना के आधार पर दिये गये परामर्श हैं जिन्हें आत्म-दर्शी पद से अभिहित किया जा सकता है । सदाचार भी इसी प्रकार के क्रियान्वित और परीक्षित कर्मचेतना जन्य परामर्श की कोटि में आते हैं । परन्तु इन सभी प्रमाणों की भूमिका एक सहायक प्रमाण के रुप में ही स्वीकार की जा सकती है। उदाहरण के तौर पर हम अपने प्रत्यक्ष को अन्यों के प्रत्यक्ष से पुष्ट करते हैं अथवा अपने स्वार्थानुमान को पंचावयव वाक्यों के माध्यम से जब पारार्थ बनाते हैं तो पंचावयव को सुनने वाला व्यक्ति उसे शब्द प्रमाण के रुप में ग्रहण नहीं करता बल्कि उसमें 'पर्वतो वह्निमान्' की स्वतंत्र प्रमिति उत्पन्न होती है, उसी प्रकार श्रुति, स्मृति और सदाचार मूलक परामर्श हमारी कर्म-चेतना और नैतिक बोध को प्रोन्नत करते हैं । यदि गीता के सन्दर्भ में इन सहायक प्रमाणों पर विचार करें तो उनकी भूमिका पूरे तौर से तब स्पष्ट हो जाती है जब श्रीकृष्ण अर्जुन को सब प्रकार
715