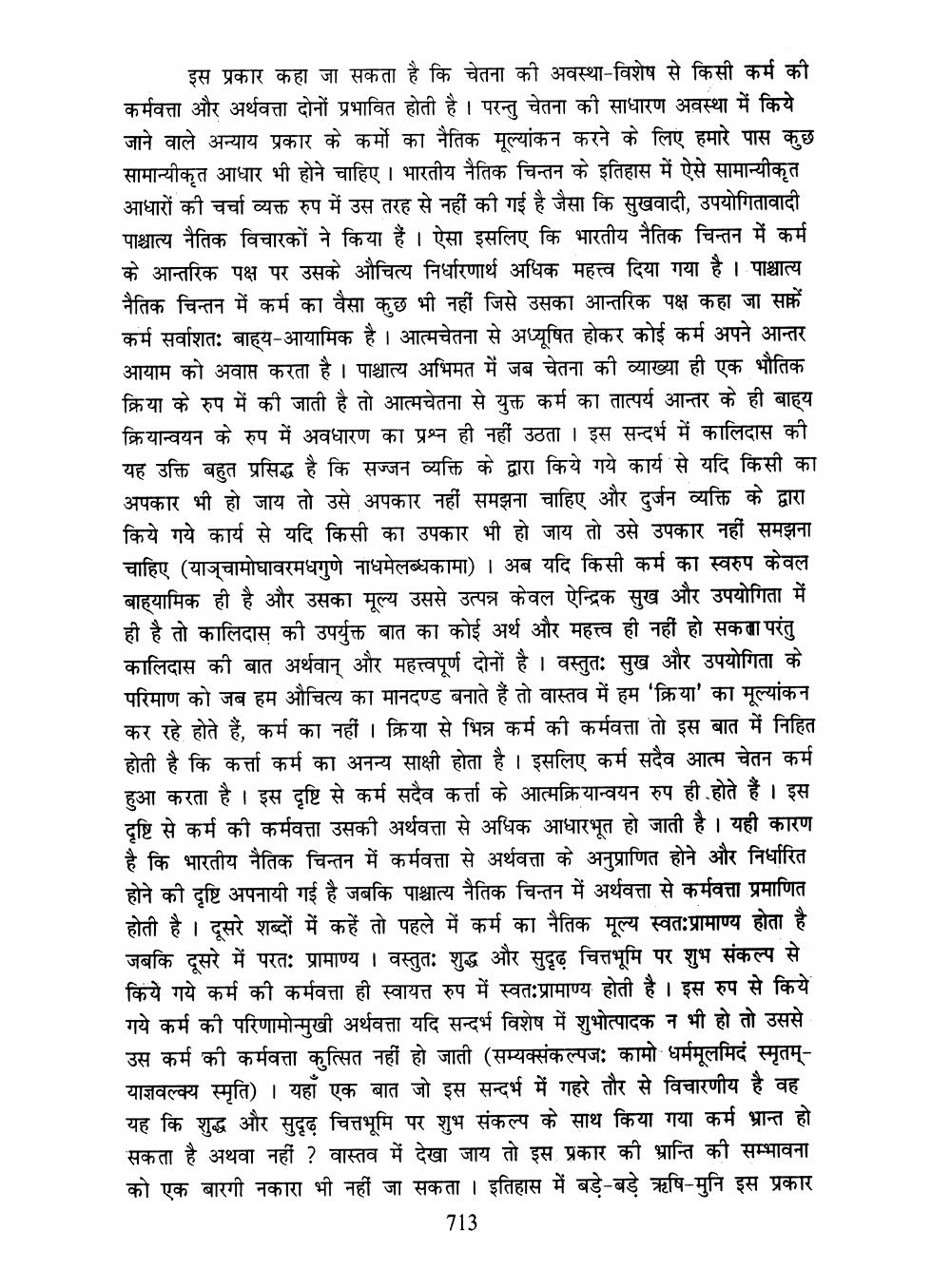________________
इस प्रकार कहा जा सकता है कि चेतना की अवस्था-विशेष से किसी कर्म की कर्मवत्ता और अर्थवत्ता दोनों प्रभावित होती है । परन्तु चेतना की साधारण अवस्था में किये जाने वाले अन्याय प्रकार के कर्मों का नैतिक मूल्यांकन करने के लिए हमारे पास कुछ सामान्यीकृत आधार भी होने चाहिए । भारतीय नैतिक चिन्तन के इतिहास में ऐसे सामान्यीकृत आधारों की चर्चा व्यक्त रुप में उस तरह से नहीं की गई है जैसा कि सुखवादी, उपयोगितावादी पाश्चात्य नैतिक विचारकों ने किया हैं । ऐसा इसलिए कि भारतीय नैतिक चिन्तन में कर्म के आन्तरिक पक्ष पर उसके औचित्य निर्धारणार्थ अधिक महत्त्व दिया गया है । पाश्चात्य नैतिक चिन्तन में कर्म का वैसा कुछ भी नहीं जिसे उसका आन्तरिक पक्ष कहा जा सकें कर्म सर्वाशतः बाह्य-आयामिक है। आत्मचेतना से अध्यूषित होकर कोई कर्म अपने आन्तर
आयाम को अवाप्त करता है । पाश्चात्य अभिमत में जब चेतना की व्याख्या ही एक भौतिक क्रिया के रुप में की जाती है तो आत्मचेतना से युक्त कर्म का तात्पर्य आन्तर के ही बाह्य क्रियान्वयन के रुप में अवधारण का प्रश्न ही नहीं उठता । इस सन्दर्भ में कालिदास की यह उक्ति बहुत प्रसिद्ध है कि सज्जन व्यक्ति के द्वारा किये गये कार्य से यदि किसी का अपकार भी हो जाय तो उसे अपकार नहीं समझना चाहिए और दुर्जन व्यक्ति के द्वारा किये गये कार्य से यदि किसी का उपकार भी हो जाय तो उसे उपकार नहीं समझना चाहिए (याञ्चामोघावरमधगुणे नाधमेलब्धकामा) । अब यदि किसी कर्म का स्वरुप केवल बाह्यामिक ही है और उसका मूल्य उससे उत्पन्न केवल ऐन्द्रिक सुख और उपयोगिता में ही है तो कालिदास की उपर्युक्त बात का कोई अर्थ और महत्त्व ही नहीं हो सकता परंतु कालिदास की बात अर्थवान् और महत्त्वपूर्ण दोनों है । वस्तुतः सुख और उपयोगिता के परिमाण को जब हम औचित्य का मानदण्ड बनाते हैं तो वास्तव में हम 'क्रिया' का मल्यांकन कर रहे होते हैं, कर्म का नहीं । क्रिया से भिन्न कर्म की कर्मवत्ता तो इस बात में निहित होती है कि कर्ता कर्म का अनन्य साक्षी होता है। इसलिए कर्म सदैव आत्म चेतन कर्म हुआ करता है । इस दृष्टि से कर्म सदैव कर्ता के आत्मक्रियान्वयन रुप ही होते हैं । इस दृष्टि से कर्म की कर्मवत्ता उसकी अर्थवत्ता से अधिक आधारभूत हो जाती है। यही कारण है कि भारतीय नैतिक चिन्तन में कर्मवत्ता से अर्थवत्ता के अनुप्राणित होने और निर्धारित होने की दृष्टि अपनायी गई है जबकि पाश्चात्य नैतिक चिन्तन में अर्थवत्ता से कर्मवत्ता प्रमाणित होती है । दूसरे शब्दों में कहें तो पहले में कर्म का नैतिक मूल्य स्वतःप्रामाण्य होता है जबकि दूसरे में परतः प्रामाण्य । वस्तुतः शुद्ध और सुदृढ़ चित्तभूमि पर शुभ संकल्प से किये गये कर्म की कर्मवत्ता ही स्वायत्त रुप में स्वतःप्रामाण्य होती है। इस रुप से किये गये कर्म की परिणामोन्मुखी अर्थवत्ता यदि सन्दर्भ विशेष में शुभोत्पादक न भी हो तो उससे उस कर्म की कर्मवत्ता कुत्सित नहीं हो जाती (सम्यक्संकल्पजः कामो धर्ममूलमिदं स्मृतम्याज्ञवल्क्य स्मृति) । यहाँ एक बात जो इस सन्दर्भ में गहरे तौर से विचारणीय है वह यह कि शुद्ध और सुदृढ़ चित्तभूमि पर शुभ संकल्प के साथ किया गया कर्म भ्रान्त हो सकता है अथवा नहीं ? वास्तव में देखा जाय तो इस प्रकार की भ्रान्ति की सम्भावना को एक बारगी नकारा भी नहीं जा सकता । इतिहास में बड़े-बड़े ऋषि-मुनि इस प्रकार
713