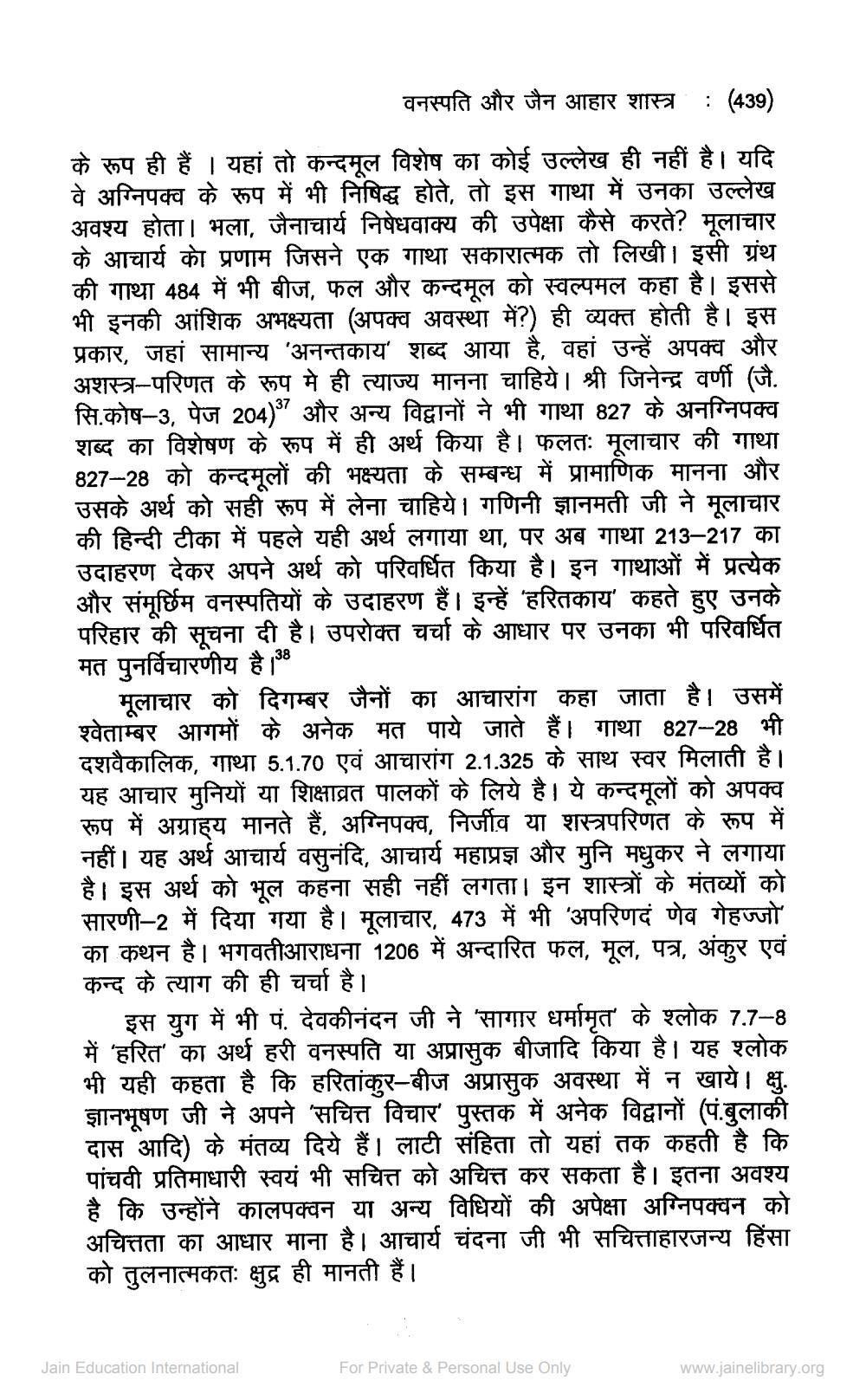________________
वनस्पति और जैन आहार शास्त्र : (439)
के रूप ही हैं । यहां तो कन्दमूल विशेष का कोई उल्लेख ही नहीं है। यदि वे अग्निपक्व के रूप में भी निषिद्ध होते, तो इस गाथा में उनका उल्लेख अवश्य होता । भला, जैनाचार्य निषेधवाक्य की उपेक्षा कैसे करते? मूलाचार के आचार्य को प्रणाम जिसने एक गाथा सकारात्मक तो लिखी । इसी ग्रंथ की गाथा 484 में भी बीज, फल और कन्दमूल को स्वल्पमल कहा है। इससे भी इनकी आंशिक अभक्ष्यता ( अपक्व अवस्था में ? ) ही व्यक्त होती है। इस प्रकार, जहां सामान्य 'अनन्तकाय' शब्द आया है, वहां उन्हें अपक्व और अशस्त्र - परिणत के रूप मे ही त्याज्य मानना चाहिये । श्री जिनेन्द्र वर्णी (जै. सि.कोष - 3, पेज 204 ) 27 और अन्य विद्वानों ने भी गाथा 827 के अनग्निपक्व शब्द का विशेषण के रूप में ही अर्थ किया है। फलतः मूलाचार की गाथा 827-28 को कन्दमूलों की भक्ष्यता के सम्बन्ध में प्रामाणिक मानना और उसके अर्थ को सही रूप में लेना चाहिये । गणिनी ज्ञानमती जी ने मूलाचार की हिन्दी टीका में पहले यही अर्थ लगाया था, पर अब गाथा 213-217 का उदाहरण देकर अपने अर्थ को परिवर्धित किया है। इन गाथाओं में प्रत्येक और संमूर्छिम वनस्पतियों के उदाहरण हैं। इन्हें 'हरितकाय' कहते हुए उनके परिहार की सूचना दी है। उपरोक्त चर्चा के आधार पर उनका भी परिवर्धित मत पुनर्विचारणीय है। 38
मूलाचार को दिगम्बर जैनों का आचारांग कहा जाता है । उसमें श्वेताम्बर आगमों के अनेक मत पाये जाते हैं। गाथा 827-28 भी दशवैकालिक, गाथा 5.1.70 एवं आचारांग 2.1.325 के साथ स्वर मिलाती है । यह आचार मुनियों या शिक्षाव्रत पालकों के लिये है । ये कन्दमूलों को अपक्व रूप में अग्राह्य मानते हैं, अग्निपक्व, निर्जीव या शस्त्रपरिणत के रूप में नहीं । यह अर्थ आचार्य वसुनंदि, आचार्य महाप्रज्ञ और मुनि मधुकर ने लगाया है । इस अर्थ को भूल कहना सही नहीं लगता । इन शास्त्रों के मंतव्यों को सारणी-2 में दिया गया है। मूलाचार, 473 में भी 'अपरिणदं णेव गेहज्जो' का कथन है। भगवती आराधना 1206 में अन्दारित फल, मूल, पत्र, अंकुर एवं कन्द के त्याग की ही चर्चा है ।
इस युग में भी पं. देवकीनंदन जी ने 'सागार धर्मामृत के श्लोक 7.7-8 में 'हरित' का अर्थ हरी वनस्पति या अप्रासुक बीजादि किया है। यह श्लोक भी यही कहता है कि हरितांकुर - बीज अप्रासुक अवस्था में न खाये । क्षु. ज्ञानभूषण जी ने अपने 'सचित्त विचार' पुस्तक में अनेक विद्वानों (पं. बुलाकी दास आदि) के मंतव्य दिये हैं। लाटी संहिता तो यहां तक कहती है कि पांचवी प्रतिमाधारी स्वयं भी सचित्त को अचित्त कर सकता है। इतना अवश्य है कि उन्होंने कालपक्वन या अन्य विधियों की अपेक्षा अग्निपक्वन को अचित्तता का आधार माना है। आचार्य चंदना जी भी सचित्ताहारजन्य हिंसा को तुलनात्मकतः क्षुद्र ही मानती हैं।
Jain Education International
For Private & Personal Use Only
www.jainelibrary.org