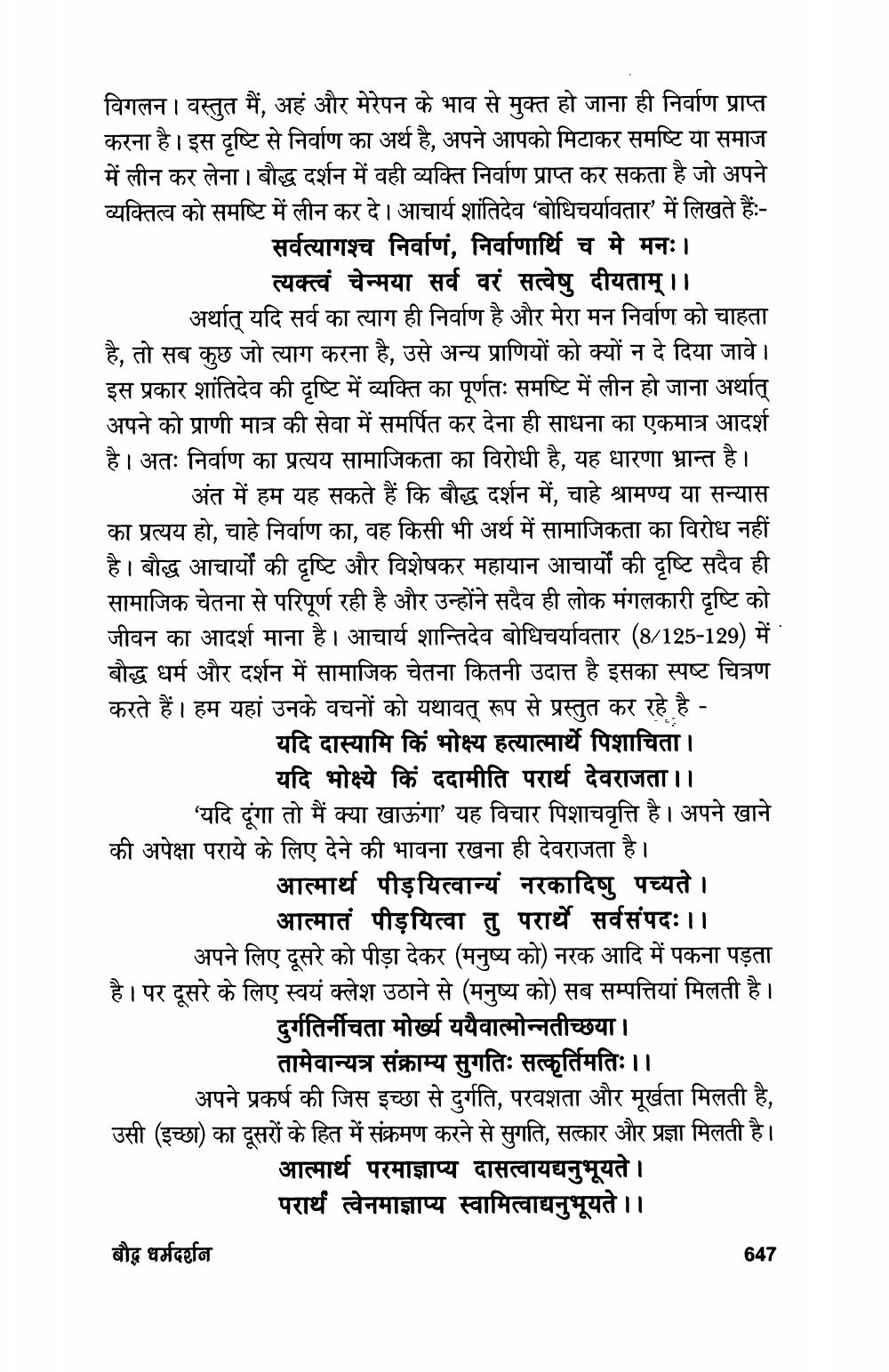________________
विगलन। वस्तुत मैं, अहं और मेरेपन के भाव से मुक्त हो जाना ही निर्वाण प्राप्त करना है। इस दृष्टि से निर्वाण का अर्थ है, अपने आपको मिटाकर समष्टि या समाज में लीन कर लेना। बौद्ध दर्शन में वही व्यक्ति निर्वाण प्राप्त कर सकता है जो अपने व्यक्तित्व को समष्टि में लीन कर दे। आचार्य शांतिदेव ‘बोधिचर्यावतार' में लिखते हैं:
सर्वत्यागश्च निर्वाणं, निर्वाणार्थि च मे मनः।
त्यक्त्वं चेन्मया सर्व वरं सत्वेषु दीयताम् ।। अर्थात् यदि सर्व का त्याग ही निर्वाण है और मेरा मन निर्वाण को चाहता है, तो सब कुछ जो त्याग करना है, उसे अन्य प्राणियों को क्यों न दे दिया जावे। इस प्रकार शांतिदेव की दृष्टि में व्यक्ति का पूर्णतः समष्टि में लीन हो जाना अर्थात् अपने को प्राणी मात्र की सेवा में समर्पित कर देना ही साधना का एकमात्र आदर्श है। अतः निर्वाण का प्रत्यय सामाजिकता का विरोधी है, यह धारणा भ्रान्त है।
___ अंत में हम यह सकते हैं कि बौद्ध दर्शन में, चाहे श्रामण्य या सन्यास का प्रत्यय हो, चाहे निर्वाण का, वह किसी भी अर्थ में सामाजिकता का विरोध नहीं है। बौद्ध आचार्यों की दृष्टि और विशेषकर महायान आचार्यों की दृष्टि सदैव ही सामाजिक चेतना से परिपूर्ण रही है और उन्होंने सदैव ही लोक मंगलकारी दृष्टि को जीवन का आदर्श माना है। आचार्य शान्तिदेव बोधिचर्यावतार (8/125-129) में बौद्ध धर्म और दर्शन में सामाजिक चेतना कितनी उदात्त है इसका स्पष्ट चित्रण करते हैं। हम यहां उनके वचनों को यथावत् रूप से प्रस्तुत कर रहे है -
यदि दास्यामि किं भोक्ष्य हत्यात्मार्थे पिशाचिता।
यदि भोक्ष्ये किं ददामीति परार्थ देवराजता।। 'यदि दूंगा तो मैं क्या खाऊंगा' यह विचार पिशाचवृत्ति है। अपने खाने की अपेक्षा पराये के लिए देने की भावना रखना ही देवराजता है।
आत्मार्थ पीड़यित्वान्यं नरकादिषु पच्यते ।
आत्मातं पीड़यित्वा तु परार्थे सर्वसंपदः।। __ अपने लिए दूसरे को पीड़ा देकर (मनुष्य को) नरक आदि में पकना पड़ता है। पर दूसरे के लिए स्वयं क्लेश उठाने से (मनुष्य को) सब सम्पत्तियां मिलती है।
दुर्गतिर्नीचता मोर्खा ययैवात्मोन्नतीच्छया।
तामेवान्यत्र संक्राम्य सुगतिः सत्कृर्तिमतिः।। ___ अपने प्रकर्ष की जिस इच्छा से दुर्गति, परवशता और मूर्खता मिलती है, उसी (इच्छा) का दूसरों के हित में संक्रमण करने से सुगति, सत्कार और प्रज्ञा मिलती है।
आत्मार्थ परमाज्ञाप्य दासत्वायद्यनुभूयते।
परार्थं त्वेनमाज्ञाप्य स्वामित्वाद्यनुभूयते।। बौद्ध धर्मदर्शन
647