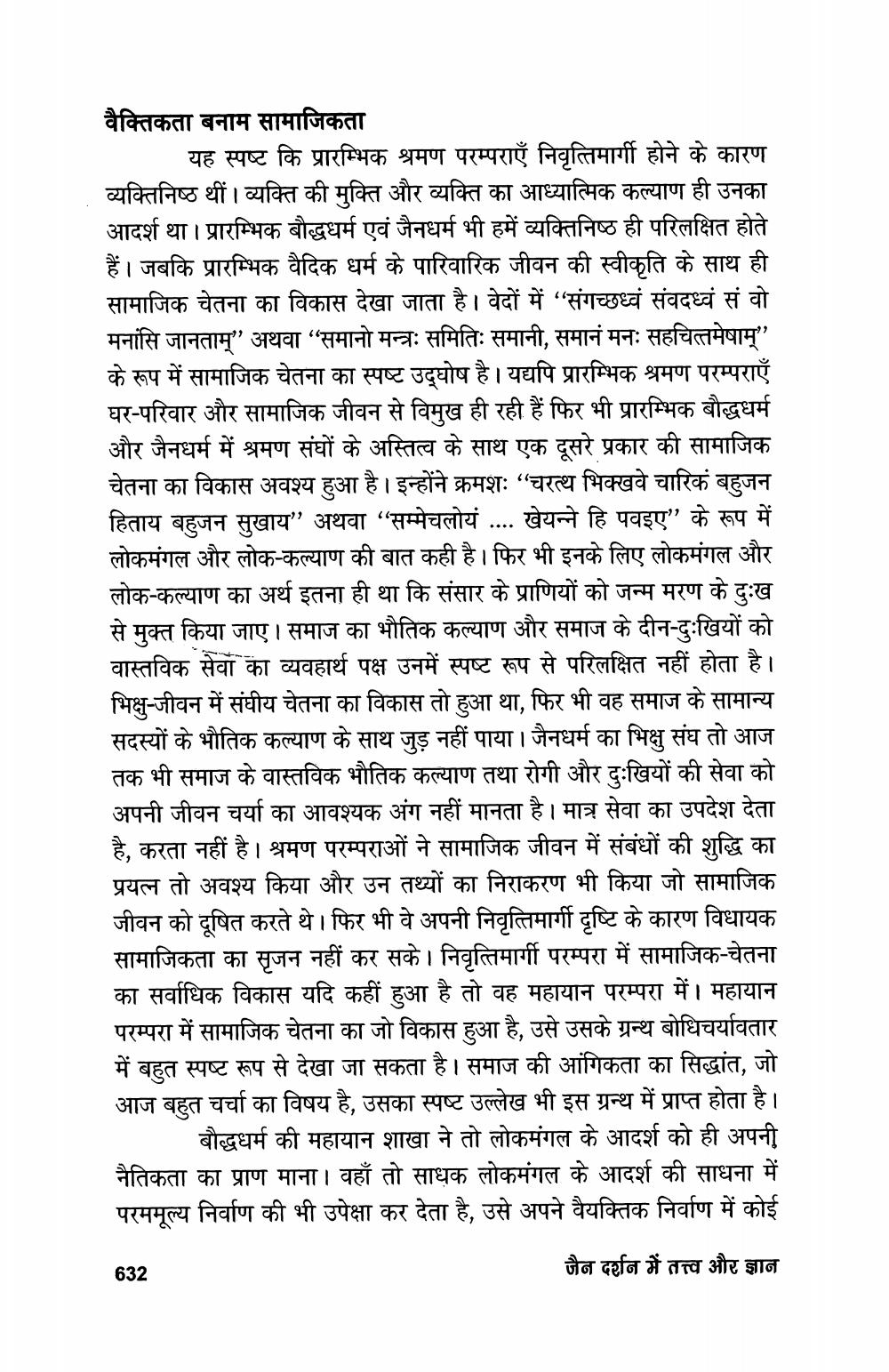________________
वैक्तिकता बनाम सामाजिकता
यह स्पष्ट कि प्रारम्भिक श्रमण परम्पराएँ निवृत्तिमार्गी होने के कारण व्यक्तिनिष्ठ थीं। व्यक्ति की मुक्ति और व्यक्ति का आध्यात्मिक कल्याण ही उनका आदर्श था । प्रारम्भिक बौद्धधर्म एवं जैनधर्म भी हमें व्यक्तिनिष्ठ ही परिलक्षित होते हैं। जबकि प्रारम्भिक वैदिक धर्म के पारिवारिक जीवन की स्वीकृति के साथ ही सामाजिक चेतना का विकास देखा जाता है । वेदों में “संगच्छध्वं संवदध्वं सं वो मनांसि जानताम्” अथवा “समानो मन्त्रः समितिः समानी, समानं मनः सहचित्तमेषाम्” के रूप में सामाजिक चेतना का स्पष्ट उद्घोष है । यद्यपि प्रारम्भिक श्रमण परम्पराएँ घर-परिवार और सामाजिक जीवन से विमुख ही रही हैं फिर भी प्रारम्भिक बौद्धधर्म और जैनधर्म में श्रमण संघों के अस्तित्व के साथ एक दूसरे प्रकार की सामाजिक चेतना का विकास अवश्य हुआ है । इन्होंने क्रमशः “चरत्थ भिक्खवे चारिकं बहुजन हिताय बहुजन सुखाय” अथवा “सम्मेचलोयं खेयन्ने हि पवइए" के रूप में लोकमंगल और लोक-कल्याण की बात कही है। फिर भी इनके लिए लोकमंगल और लोक-कल्याण का अर्थ इतना ही था कि संसार के प्राणियों को जन्म मरण के दुःख से मुक्त किया जाए। समाज का भौतिक कल्याण और समाज के दीन-दुःखियों को वास्तविक सेवा का व्यवहार्थ पक्ष उनमें स्पष्ट रूप से परिलक्षित नहीं होता है । भिक्षु-जीवन में संघीय चेतना का विकास तो हुआ था, फिर भी वह समाज के सामान्य सदस्यों के भौतिक कल्याण के साथ जुड़ नहीं पाया। जैनधर्म का भिक्षु संघ तो आज तक भी समाज के वास्तविक भौतिक कल्याण तथा रोगी और दुःखियों की सेवा को अपनी जीवन चर्या का आवश्यक अंग नहीं मानता है । मात्र सेवा का उपदेश देता है, करता नहीं है । श्रमण परम्पराओं ने सामाजिक जीवन में संबंधों की शुद्धि का प्रयत्न तो अवश्य किया और उन तथ्यों का निराकरण भी किया जो सामाजिक जीवन को दूषित करते थे । फिर भी वे अपनी निवृत्तिमार्गी दृष्टि के कारण विधायक सामाजिकता का सृजन नहीं कर सके । निवृत्तिमार्गी परम्परा में सामाजिक चेतना का सर्वाधिक विकास यदि कहीं हुआ है तो वह महायान परम्परा में । महायान परम्परा में सामाजिक चेतना का जो विकास हुआ है, उसे उसके ग्रन्थ बोधिचर्यावतार में बहुत स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। समाज की आंगिकता का सिद्धांत, जो आज बहुत चर्चा का विषय है, उसका स्पष्ट उल्लेख भी इस ग्रन्थ में प्राप्त होता है । बौद्धधर्म की महायान शाखा ने तो लोकमंगल के आदर्श को ही अपनी नैतिकता का प्राण माना । वहाँ तो साधक लोकमंगल के आदर्श की साधना में परममूल्य निर्वाण की भी उपेक्षा कर देता है, उसे अपने वैयक्तिक निर्वाण में कोई
जैन दर्शन में तत्त्व और ज्ञान
632
****