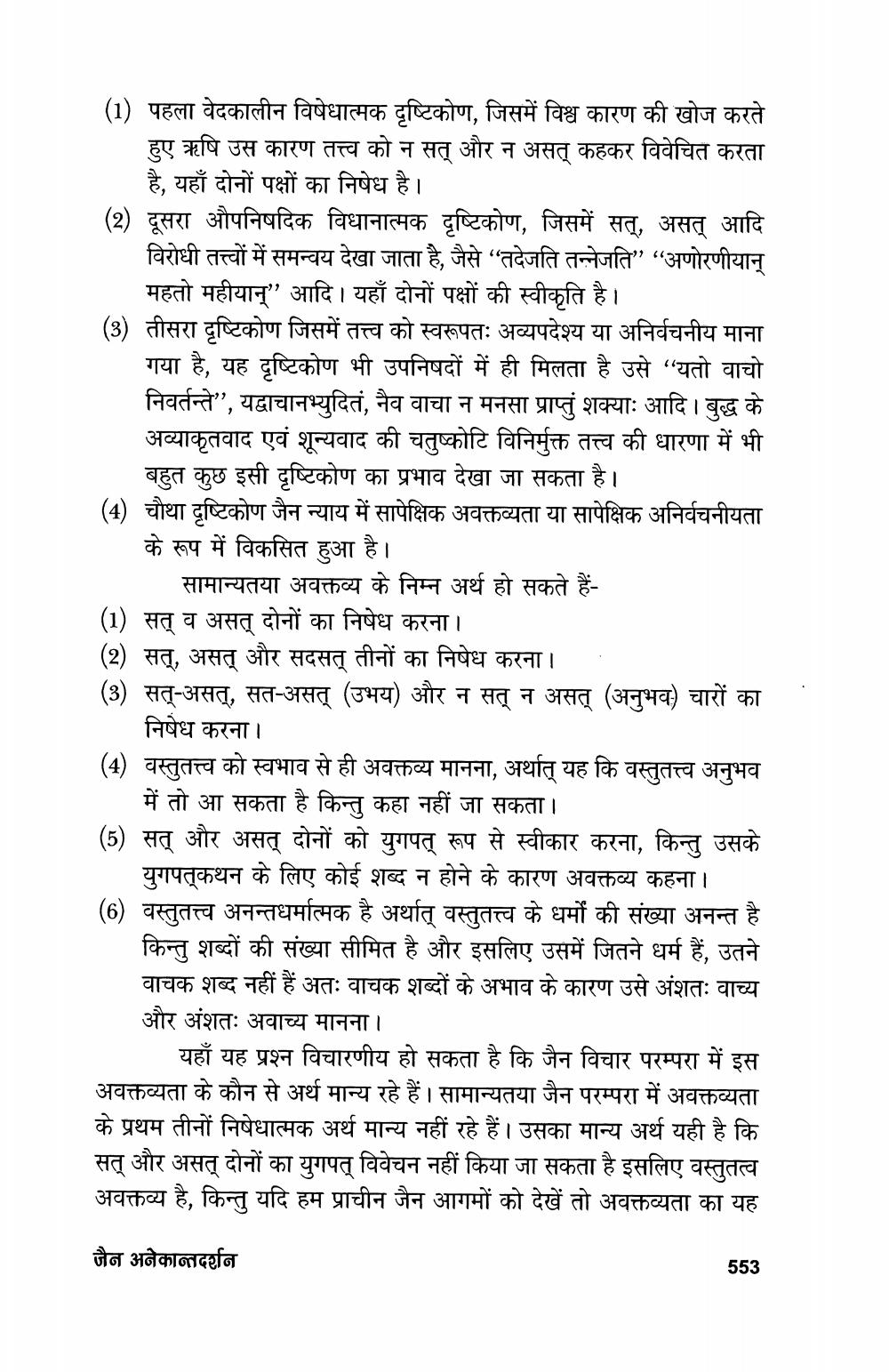________________
(1) पहला वेदकालीन विषेधात्मक दृष्टिकोण, जिसमें विश्व कारण की खोज करते
हुए ऋषि उस कारण तत्त्व को न सत् और न असत् कहकर विवेचित करता
है, यहाँ दोनों पक्षों का निषेध है। (2) दूसरा औपनिषदिक विधानात्मक दृष्टिकोण, जिसमें सत, असत आदि
विरोधी तत्त्वों में समन्वय देखा जाता है, जैसे “तदेजति तन्नेजति" "अणोरणीयान्
महतो महीयान्" आदि। यहाँ दोनों पक्षों की स्वीकृति है। (3) तीसरा दृष्टिकोण जिसमें तत्त्व को स्वरूपतः अव्यपदेश्य या अनिर्वचनीय माना
गया है, यह दृष्टिकोण भी उपनिषदों में ही मिलता है उसे “यतो वाचो निवर्तन्ते", यद्वाचानभ्युदितं, नैव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्याः आदि । बुद्ध के अव्याकृतवाद एवं शून्यवाद की चतुष्कोटि विनिर्मुक्त तत्त्व की धारणा में भी
बहुत कुछ इसी दृष्टिकोण का प्रभाव देखा जा सकता है। (4) चौथा दृष्टिकोण जैन न्याय में सापेक्षिक अवक्तव्यता या सापेक्षिक अनिर्वचनीयता के रूप में विकसित हुआ है।
सामान्यतया अवक्तव्य के निम्न अर्थ हो सकते हैं(1) सत् व असत् दोनों का निषेध करना। (2) सत्, असत् और सदसत् तीनों का निषेध करना। (3) सत्-असत्, सत-असत् (उभय) और न सत् न असत् (अनुभव) चारों का
निषेध करना। (4) वस्तुतत्त्व को स्वभाव से ही अवक्तव्य मानना, अर्थात् यह कि वस्तुतत्त्व अनुभव
में तो आ सकता है किन्तु कहा नहीं जा सकता। (5) सत् और असत् दोनों को युगपत् रूप से स्वीकार करना, किन्तु उसके
युगपत्कथन के लिए कोई शब्द न होने के कारण अवक्तव्य कहना। (6) वस्तुतत्त्व अनन्तधर्मात्मक है अर्थात् वस्तुतत्त्व के धर्मों की संख्या अनन्त है
किन्तु शब्दों की संख्या सीमित है और इसलिए उसमें जितने धर्म हैं, उतने वाचक शब्द नहीं हैं अतः वाचक शब्दों के अभाव के कारण उसे अंशतः वाच्य और अंशतः अवाच्य मानना।
यहाँ यह प्रश्न विचारणीय हो सकता है कि जैन विचार परम्परा में इस अवक्तव्यता के कौन से अर्थ मान्य रहे हैं। सामान्यतया जैन परम्परा में अवक्तव्यता के प्रथम तीनों निषेधात्मक अर्थ मान्य नहीं रहे हैं। उसका मान्य अर्थ यही है कि सत् और असत् दोनों का युगपत् विवेचन नहीं किया जा सकता है इसलिए वस्तुतत्व अवक्तव्य है, किन्तु यदि हम प्राचीन जैन आगमों को देखें तो अवक्तव्यता का यह
जैन अनेकान्तदर्शन
553