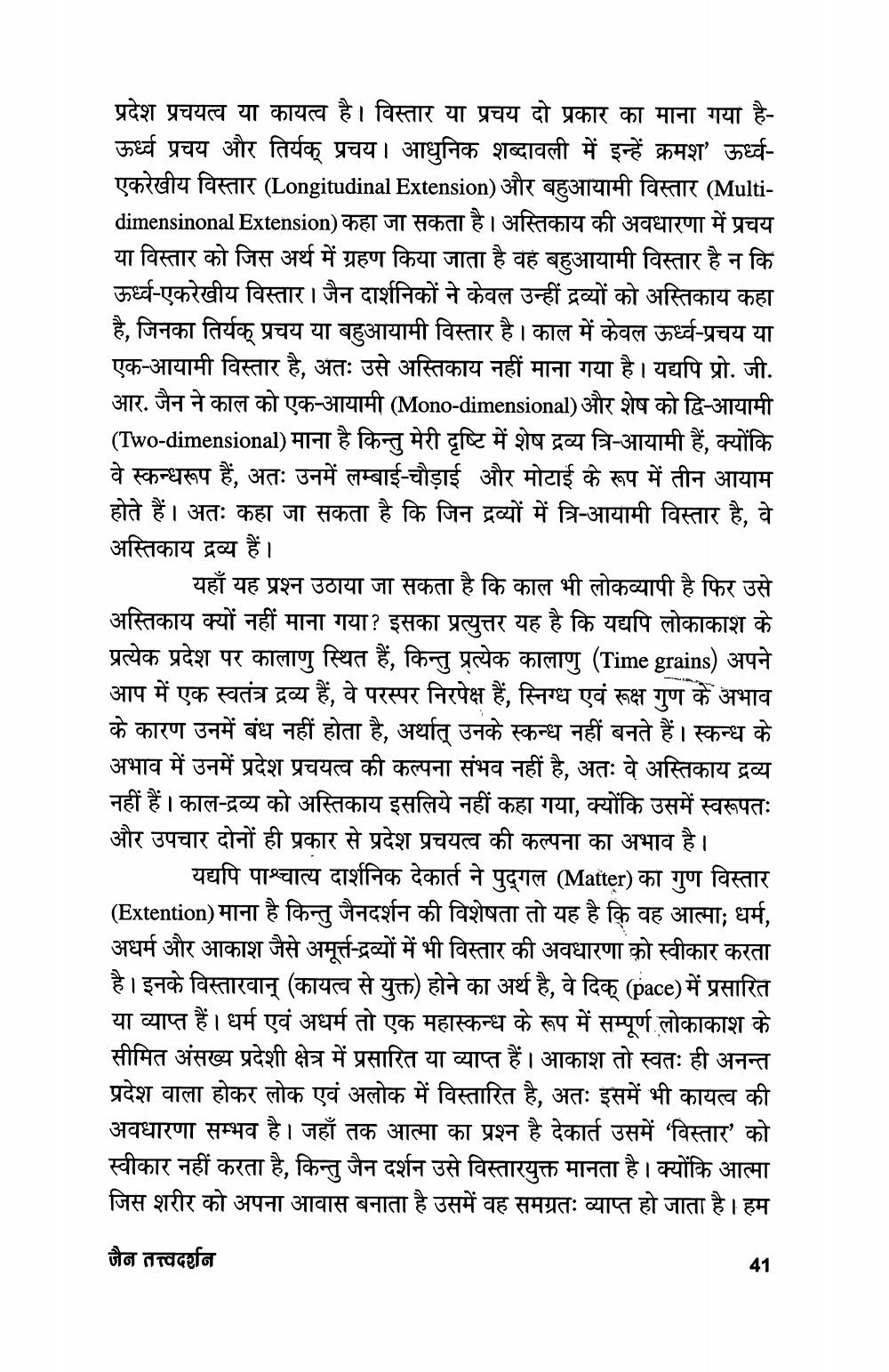________________
प्रदेश प्रचयत्व या कायत्व है। विस्तार या प्रचय दो प्रकार का माना गया हैऊर्ध्व प्रचय और तिर्यक् प्रचय। आधुनिक शब्दावली में इन्हें क्रमश' ऊर्ध्वएकरेखीय विस्तार (Longitudinal Extension) और बहुआयामी विस्तार (Multidimensinonal Extension) कहा जा सकता है। अस्तिकाय की अवधारणा में प्रचय या विस्तार को जिस अर्थ में ग्रहण किया जाता है वह बहुआयामी विस्तार है न कि ऊर्ध्व-एकरेखीय विस्तार। जैन दार्शनिकों ने केवल उन्हीं द्रव्यों को अस्तिकाय कहा है, जिनका तिर्यक् प्रचय या बहुआयामी विस्तार है। काल में केवल ऊर्ध्व-प्रचय या एक-आयामी विस्तार है, अतः उसे अस्तिकाय नहीं माना गया है। यद्यपि प्रो. जी. आर. जैन ने काल को एक-आयामी (Mono-dimensional) और शेष को द्वि-आयामी (Two-dimensional) माना है किन्तु मेरी दृष्टि में शेष द्रव्य त्रि-आयामी हैं, क्योंकि वे स्कन्धरूप हैं, अतः उनमें लम्बाई-चौड़ाई और मोटाई के रूप में तीन आयाम होते हैं। अतः कहा जा सकता है कि जिन द्रव्यों में त्रि-आयामी विस्तार है, वे अस्तिकाय द्रव्य हैं।
यहाँ यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि काल भी लोकव्यापी है फिर उसे अस्तिकाय क्यों नहीं माना गया? इसका प्रत्युत्तर यह है कि यद्यपि लोकाकाश के प्रत्येक प्रदेश पर कालाणु स्थित हैं, किन्तु प्रत्येक कालाणु (Time grains) अपने आप में एक स्वतंत्र द्रव्य हैं, वे परस्पर निरपेक्ष हैं, स्निग्ध एवं रूक्ष गुण के अभाव के कारण उनमें बंध नहीं होता है, अर्थात् उनके स्कन्ध नहीं बनते हैं। स्कन्ध के अभाव में उनमें प्रदेश प्रचयत्व की कल्पना संभव नहीं है, अतः वे अस्तिकाय द्रव्य नहीं हैं। काल-द्रव्य को अस्तिकाय इसलिये नहीं कहा गया, क्योंकि उसमें स्वरूपतः और उपचार दोनों ही प्रकार से प्रदेश प्रचयत्व की कल्पना का अभाव है।
यद्यपि पाश्चात्य दार्शनिक देकार्त ने पुद्गल (Matter) का गुण विस्तार (Extention) माना है किन्तु जैनदर्शन की विशेषता तो यह है कि वह आत्मा; धर्म, अधर्म और आकाश जैसे अमूर्त-द्रव्यों में भी विस्तार की अवधारणा को स्वीकार करता है। इनके विस्तारवान् (कायत्व से युक्त) होने का अर्थ है, वे दिक् (pace) में प्रसारित या व्याप्त हैं। धर्म एवं अधर्म तो एक महास्कन्ध के रूप में सम्पूर्ण लोकाकाश के सीमित अंसख्य प्रदेशी क्षेत्र में प्रसारित या व्याप्त हैं। आकाश तो स्वतः ही अनन्त प्रदेश वाला होकर लोक एवं अलोक में विस्तारित है, अतः इसमें भी कायत्व की अवधारणा सम्भव है। जहाँ तक आत्मा का प्रश्न है देकार्त उसमें 'विस्तार' को स्वीकार नहीं करता है, किन्तु जैन दर्शन उसे विस्तारयुक्त मानता है। क्योंकि आत्मा जिस शरीर को अपना आवास बनाता है उसमें वह समग्रतः व्याप्त हो जाता है। हम
जैन तत्त्वदर्शन
41