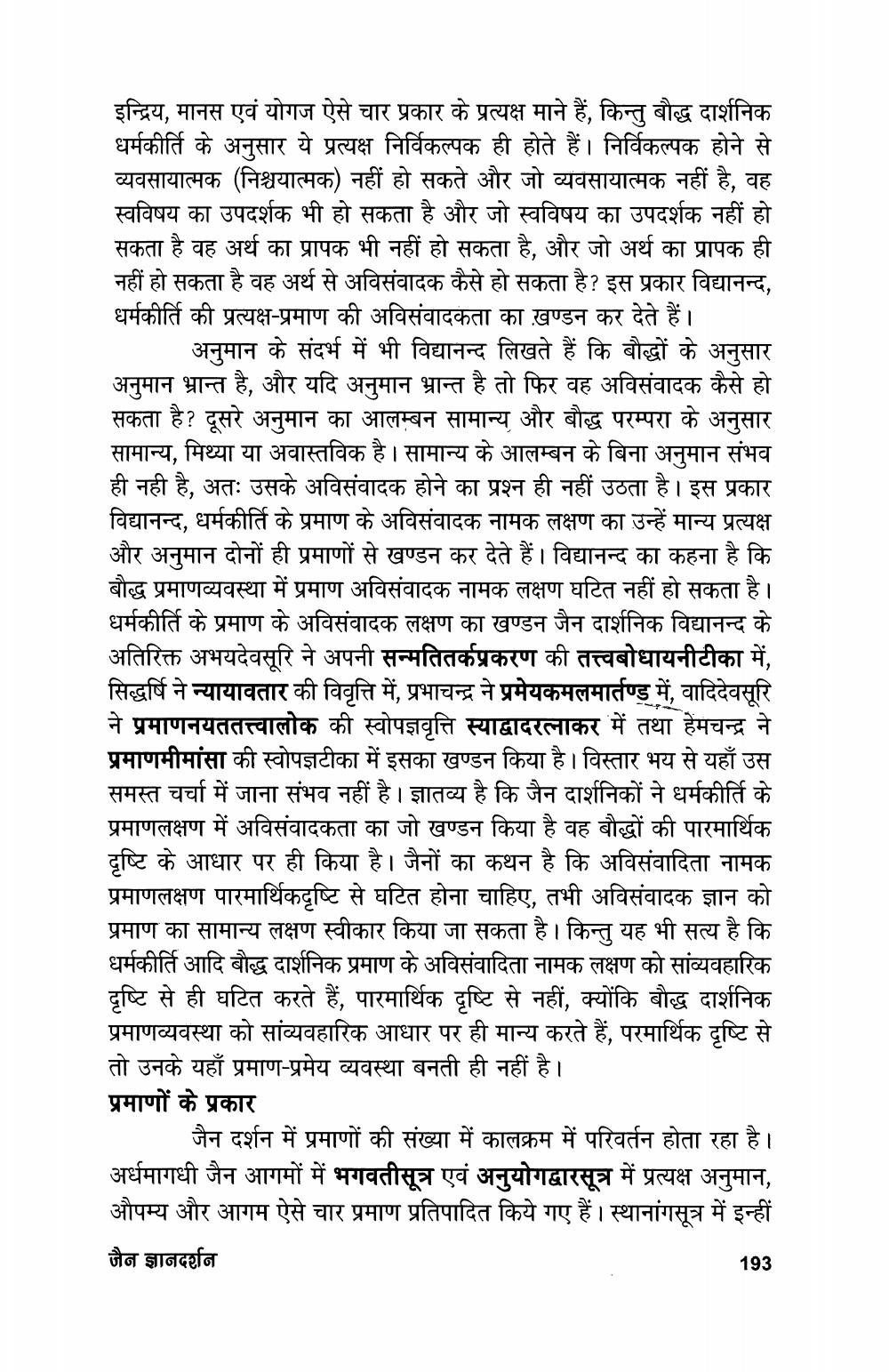________________
इन्द्रिय, मानस एवं योगज ऐसे चार प्रकार के प्रत्यक्ष माने हैं, किन्तु बौद्ध दार्शनिक धर्मकीर्ति के अनुसार ये प्रत्यक्ष निर्विकल्पक ही होते हैं। निर्विकल्पक होने से व्यवसायात्मक (निश्चयात्मक) नहीं हो सकते और जो व्यवसायात्मक नहीं है, वह स्वविषय का उपदर्शक भी हो सकता है और जो स्वविषय का उपदर्शक नहीं हो सकता है वह अर्थ का प्रापक भी नहीं हो सकता है, और जो अर्थ का प्रापक ही नहीं हो सकता है वह अर्थ से अविसंवादक कैसे हो सकता है? इस प्रकार विद्यानन्द, धर्मकीर्ति की प्रत्यक्ष-प्रमाण की अविसंवादकता का खण्डन कर देते हैं।
अनुमान के संदर्भ में भी विद्यानन्द लिखते हैं कि बौद्धों के अनुसार अनुमान भ्रान्त है, और यदि अनुमान भ्रान्त है तो फिर वह अविसंवादक कैसे हो सकता है? दूसरे अनुमान का आलम्बन सामान्य और बौद्ध परम्परा के अनुसार सामान्य, मिथ्या या अवास्तविक है। सामान्य के आलम्बन के बिना अनुमान संभव ही नही है, अतः उसके अविसंवादक होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। इस प्रकार विद्यानन्द, धर्मकीर्ति के प्रमाण के अविसंवादक नामक लक्षण का उन्हें मान्य प्रत्यक्ष
और अनुमान दोनों ही प्रमाणों से खण्डन कर देते हैं। विद्यानन्द का कहना है कि बौद्ध प्रमाणव्यवस्था में प्रमाण अविसंवादक नामक लक्षण घटित नहीं हो सकता है। धर्मकीर्ति के प्रमाण के अविसंवादक लक्षण का खण्डन जैन दार्शनिक विद्यानन्द के अतिरिक्त अभयदेवसूरि ने अपनी सन्मतितर्कप्रकरण की तत्त्वबोधायनीटीका में, सिद्धर्षि ने न्यायावतार की विवृत्ति में, प्रभाचन्द्र ने प्रमेयकमलमार्तण्ड में, वादिदेवसूरि ने प्रमाणनयततत्त्वालोक की स्वोपज्ञवृत्ति स्याद्वादरत्नाकर में तथा हेमचन्द्र ने प्रमाणमीमांसा की स्वोपज्ञटीका में इसका खण्डन किया है। विस्तार भय से यहाँ उस समस्त चर्चा में जाना संभव नहीं है। ज्ञातव्य है कि जैन दार्शनिकों ने धर्मकीर्ति के प्रमाणलक्षण में अविसंवादकता का जो खण्डन किया है वह बौद्धों की पारमार्थिक दृष्टि के आधार पर ही किया है। जैनों का कथन है कि अविसंवादिता नामक प्रमाणलक्षण पारमार्थिकदृष्टि से घटित होना चाहिए, तभी अविसंवादक ज्ञान को प्रमाण का सामान्य लक्षण स्वीकार किया जा सकता है। किन्तु यह भी सत्य है कि धर्मकीर्ति आदि बौद्ध दार्शनिक प्रमाण के अविसंवादिता नामक लक्षण को सांव्यवहारिक दृष्टि से ही घटित करते हैं, पारमार्थिक दृष्टि से नहीं, क्योंकि बौद्ध दार्शनिक प्रमाणव्यवस्था को सांव्यवहारिक आधार पर ही मान्य करते हैं, परमार्थिक दृष्टि से तो उनके यहाँ प्रमाण-प्रमेय व्यवस्था बनती ही नहीं है। प्रमाणों के प्रकार
जैन दर्शन में प्रमाणों की संख्या में कालक्रम में परिवर्तन होता रहा है। अर्धमागधी जैन आगमों में भगवतीसूत्र एवं अनुयोगद्वारसूत्र में प्रत्यक्ष अनुमान, औपम्य और आगम ऐसे चार प्रमाण प्रतिपादित किये गए हैं। स्थानांगसूत्र में इन्हीं जैन ज्ञानदर्शन
193