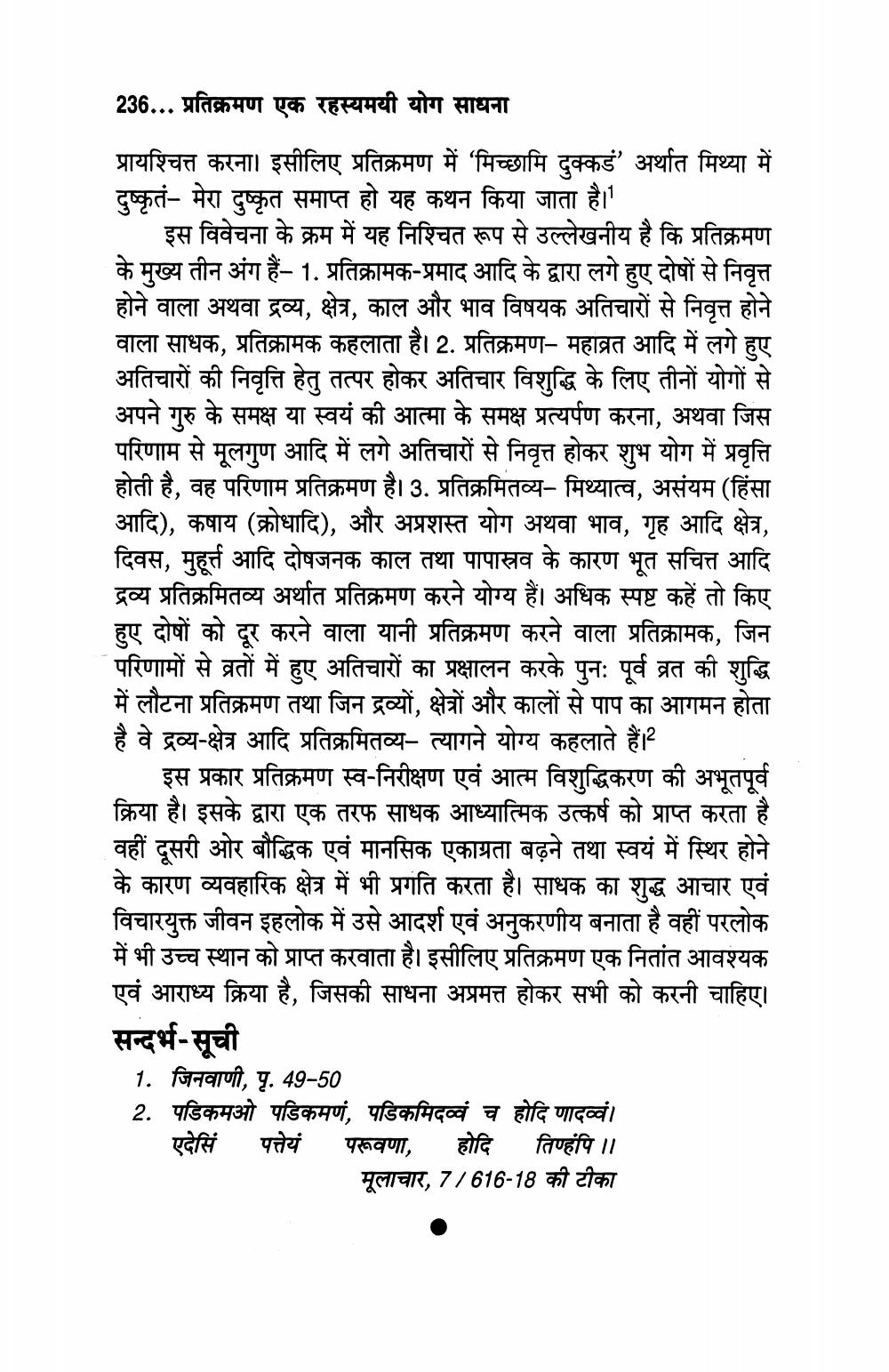________________
236... प्रतिक्रमण एक रहस्यमयी योग साधना प्रायश्चित्त करना। इसीलिए प्रतिक्रमण में 'मिच्छामि दुक्कडं' अर्थात मिथ्या में दुष्कृतं- मेरा दुष्कृत समाप्त हो यह कथन किया जाता है।
इस विवेचना के क्रम में यह निश्चित रूप से उल्लेखनीय है कि प्रतिक्रमण के मुख्य तीन अंग हैं- 1. प्रतिक्रामक-प्रमाद आदि के द्वारा लगे हुए दोषों से निवृत्त होने वाला अथवा द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव विषयक अतिचारों से निवृत्त होने वाला साधक, प्रतिक्रामक कहलाता है। 2. प्रतिक्रमण- महाव्रत आदि में लगे हुए अतिचारों की निवृत्ति हेतु तत्पर होकर अतिचार विशुद्धि के लिए तीनों योगों से अपने गुरु के समक्ष या स्वयं की आत्मा के समक्ष प्रत्यर्पण करना, अथवा जिस परिणाम से मूलगुण आदि में लगे अतिचारों से निवृत्त होकर शुभ योग में प्रवृत्ति होती है, वह परिणाम प्रतिक्रमण है। 3. प्रतिक्रमितव्य- मिथ्यात्व, असंयम (हिंसा आदि), कषाय (क्रोधादि), और अप्रशस्त योग अथवा भाव, गृह आदि क्षेत्र, दिवस, मुहूर्त आदि दोषजनक काल तथा पापास्रव के कारण भूत सचित्त आदि द्रव्य प्रतिक्रमितव्य अर्थात प्रतिक्रमण करने योग्य हैं। अधिक स्पष्ट कहें तो किए हुए दोषों को दूर करने वाला यानी प्रतिक्रमण करने वाला प्रतिक्रामक, जिन परिणामों से व्रतों में हुए अतिचारों का प्रक्षालन करके पुन: पूर्व व्रत की शुद्धि में लौटना प्रतिक्रमण तथा जिन द्रव्यों, क्षेत्रों और कालों से पाप का आगमन होता है वे द्रव्य-क्षेत्र आदि प्रतिक्रमितव्य- त्यागने योग्य कहलाते हैं।
इस प्रकार प्रतिक्रमण स्व-निरीक्षण एवं आत्म विशुद्धिकरण की अभूतपूर्व क्रिया है। इसके द्वारा एक तरफ साधक आध्यात्मिक उत्कर्ष को प्राप्त करता है वहीं दूसरी ओर बौद्धिक एवं मानसिक एकाग्रता बढ़ने तथा स्वयं में स्थिर होने के कारण व्यवहारिक क्षेत्र में भी प्रगति करता है। साधक का शुद्ध आचार एवं विचारयुक्त जीवन इहलोक में उसे आदर्श एवं अनुकरणीय बनाता है वहीं परलोक में भी उच्च स्थान को प्राप्त करवाता है। इसीलिए प्रतिक्रमण एक नितांत आवश्यक एवं आराध्य क्रिया है, जिसकी साधना अप्रमत्त होकर सभी को करनी चाहिए। सन्दर्भ-सूची 1. जिनवाणी, पृ. 49-50 2. पडिकमओ पडिकमणं, पडिकमिदव्वं च होदि णादव्वं। एदेसिं पत्तेयं परूवणा, होदि तिण्हपि ।।
मूलाचार, 7/616-18 की टीका