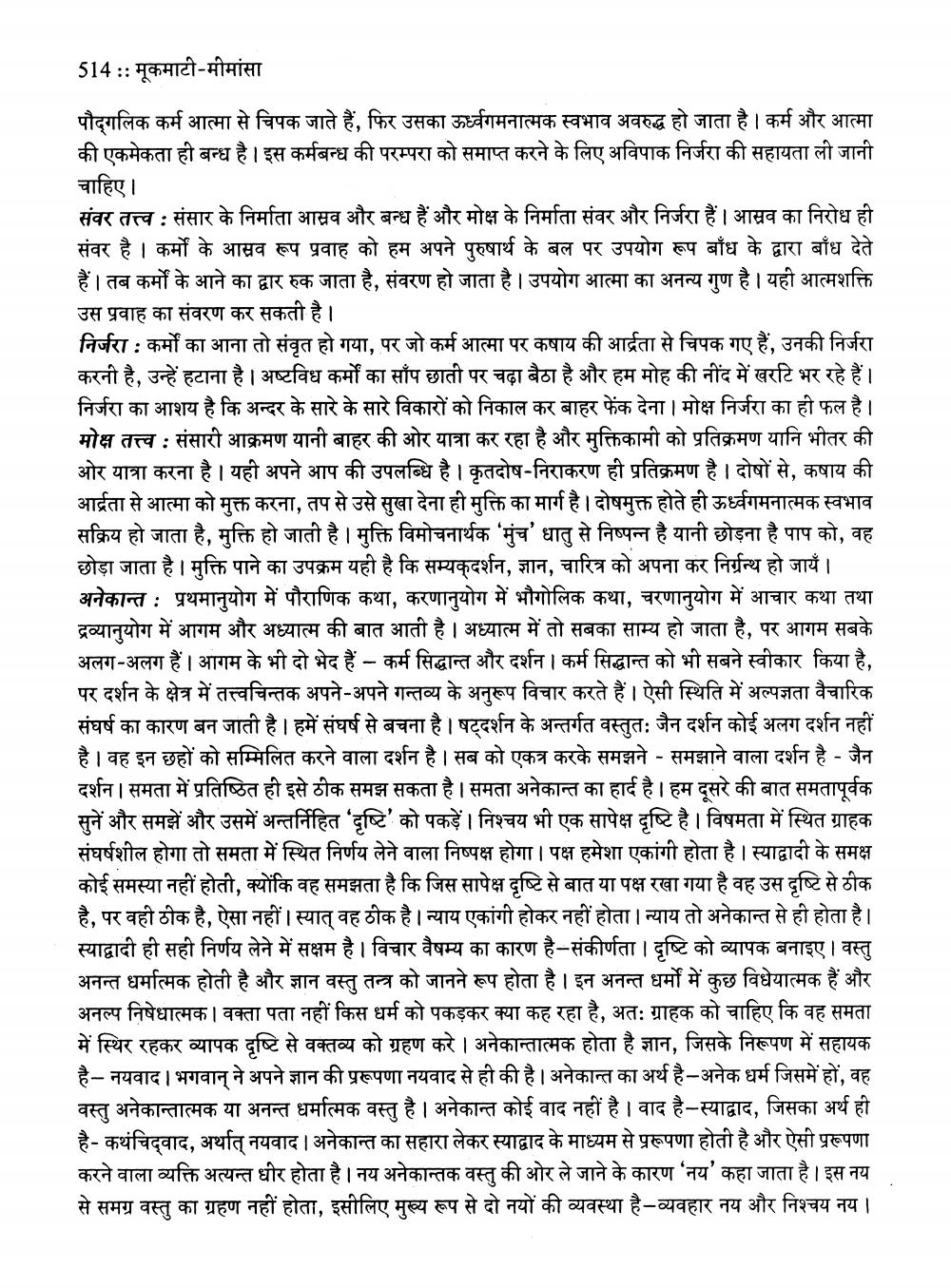________________
514 :: मूकमाटी-मीमांसा
पौद्गलिक कर्म आत्मा से चिपक जाते हैं, फिर उसका ऊर्ध्वगमनात्मक स्वभाव अवरुद्ध हो जाता है। कर्म और आत्मा एकता ही है । इस कर्मबन्ध की परम्परा को समाप्त करने के लिए अविपाक निर्जरा की सहायता ली जानी
चाहिए ।
संवर तत्त्व : संसार के निर्माता आस्रव और बन्ध हैं और मोक्ष के निर्माता संवर और निर्जरा हैं। आस्रव का निरोध ही संवर है । कर्मों के आस्रव रूप प्रवाह को हम अपने पुरुषार्थ के बल पर उपयोग रूप बाँध के द्वारा बाँध देते हैं । तब कर्मों के आने का द्वार रुक जाता है, संवरण हो जाता है। उपयोग आत्मा का अनन्य गुण है । यही आत्मशक्ति उस प्रवाह का संवरण कर सकती है ।
1
निर्जरा : कर्मों का आना तो संवृत हो गया, पर जो कर्म आत्मा पर कषाय की आर्द्रता से चिपक गए हैं, उनकी निर्जरा करनी है, उन्हें हटाना है । अष्टविध कर्मों का साँप छाती पर चढ़ा बैठा है और हम मोह की नींद में खरटि भर रहे हैं । निर्जरा का आशय है कि अन्दर के सारे के सारे विकारों को निकाल कर बाहर फेंक देना । मोक्ष निर्जरा का ही फल है। मोक्ष तत्त्व : संसारी आक्रमण यानी बाहर की ओर यात्रा कर रहा है और मुक्तिकामी को प्रतिक्रमण यानि भीतर की ओर यात्रा करना है । यही अपने आप की उपलब्धि है । कृतदोष-निराकरण ही प्रतिक्रमण है । दोषों से, कषाय की आत्मा को मुक्त करना, तप से उसे सुखा देना ही मुक्ति का मार्ग है। दोषमुक्त होते ही ऊर्ध्वगमनात्मक स्वभाव सक्रिय हो जाता है, मुक्ति हो जाती है। मुक्ति विमोचनार्थक 'मुंच' धातु से निष्पन्न है यानी छोड़ना है पाप को, वह छोड़ा जाता है । मुक्ति पाने का उपक्रम यही है कि सम्यक्दर्शन, ज्ञान, चारित्र को अपना कर निर्ग्रन्थ हो जायँ । अनेकान्त : प्रथमानुयोग में पौराणिक कथा, करणानुयोग में भौगोलिक कथा, चरणानुयोग में आचार कथा तथा द्रव्यानुयोग में आगम और अध्यात्म की बात आती है । अध्यात्म में तो सबका साम्य हो जाता है, पर आगम सबके अलग-अलग हैं । आगम के भी दो भेद हैं- कर्म सिद्धान्त और दर्शन । कर्म सिद्धान्त को भी सबने स्वीकार किया है, पर दर्शन के क्षेत्र में तत्त्वचिन्तक अपने - अपने गन्तव्य के अनुरूप विचार करते हैं । ऐसी स्थिति में अल्पज्ञता वैचारिक संघर्ष का कारण बन जाती है। हमें संघर्ष से बचना है । षट्दर्शन के अन्तर्गत वस्तुतः जैन दर्शन कोई अलग दर्शन नहीं है । वह इन छहों को सम्मिलित करने वाला दर्शन है । सब को एकत्र करके समझने - समझाने वाला दर्शन है - जैन दर्शन । समता में प्रतिष्ठित ही इसे ठीक समझ सकता है । समता अनेकान्त का हार्द है । हम दूसरे की बात समतापूर्वक सुनें और समझें और उसमें अन्तर्निहित 'दृष्टि' को पकड़ें । निश्चय भी एक सापेक्ष दृष्टि है । विषमता में स्थित ग्राहक संघर्षशील होगा तो समता में स्थित निर्णय लेने वाला निष्पक्ष होगा । पक्ष हमेशा एकांगी होता है । स्याद्वादी के समक्ष कोई समस्या नहीं होती, क्योंकि वह समझता है कि जिस सापेक्ष दृष्टि से बात या पक्ष रखा गया है वह उस दृष्टि से ठीक है, पर वही ठीक है, ऐसा नहीं । स्यात् वह ठीक है। न्याय एकांगी होकर नहीं होता। न्याय तो अनेकान्त से ही होता है। स्याद्वादी ही सही निर्णय लेने में सक्षम है। विचार वैषम्य का कारण है - संकीर्णता । दृष्टि को व्यापक बनाइए । वस्तु अनन्त धर्मात्मक होती है और ज्ञान वस्तु तन्त्र को जानने रूप होता है । इन अनन्त धर्मों में कुछ विधेयात्मक हैं और अनल्प निषेधात्मक । वक्ता पता नहीं किस धर्म को पकड़कर क्या कह रहा है, अत: ग्राहक को चाहिए कि वह समता में स्थिर रहकर व्यापक दृष्टि से वक्तव्य को ग्रहण करे । अनेकान्तात्मक होता है ज्ञान, जिसके निरूपण में सहायक है - नयवाद । भगवान् ने अपने ज्ञान की प्ररूपणा नयवाद से ही की है । अनेकान्त का अर्थ है - अनेक धर्म जिसमें हों, वह वस्तु अनेकान्तात्मक या अनन्त धर्मात्मक वस्तु है । अनेकान्त कोई वाद नहीं है । वाद है - स्याद्वाद, जिसका अर्थ ही है- कथंचिद्वाद, अर्थात् नयवाद । अनेकान्त का सहारा लेकर स्याद्वाद के माध्यम से प्ररूपणा होती है और ऐसी प्ररूपणा करने वाला व्यक्ति अत्यन्त धीर होता है। नय अनेकान्तक वस्तु की ओर ले जाने के कारण 'नय' कहा जाता है। इस नय से समग्र वस्तु का ग्रहण नहीं होता, इसीलिए मुख्य रूप से दो नयों की व्यवस्था है - व्यवहार नय और निश्चय नय ।