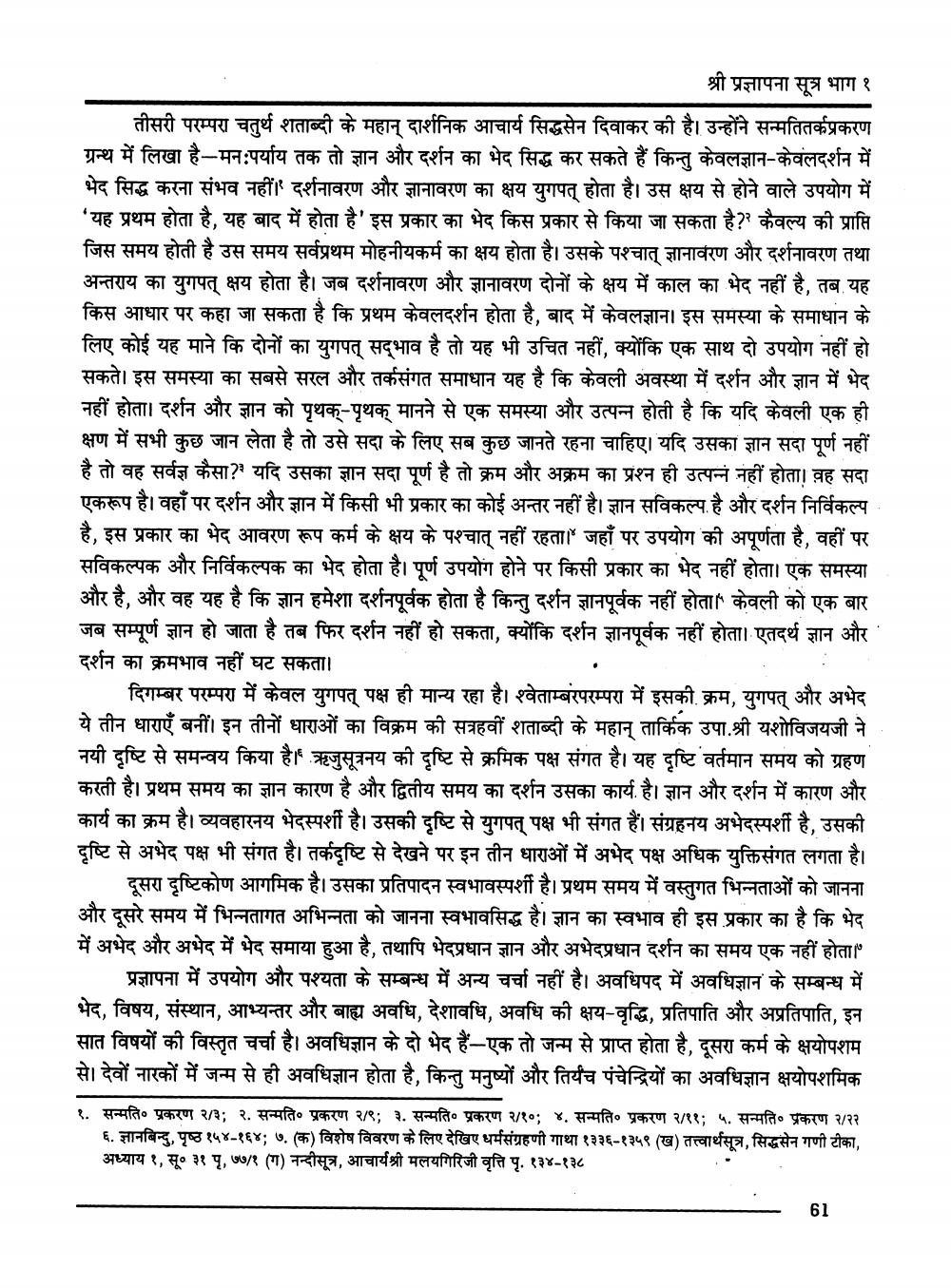________________
श्री प्रज्ञापना सूत्र भाग १ तीसरी परम्परा चतुर्थ शताब्दी के महान् दार्शनिक आचार्य सिद्धसेन दिवाकर की है। उन्होंने सन्मतितर्कप्रकरण ग्रन्थ में लिखा है - मन: पर्याय तक तो ज्ञान और दर्शन का भेद सिद्ध कर सकते हैं किन्तु केवलज्ञान - केवलदर्शन में भेद सिद्ध करना संभव नहीं।' दर्शनावरण और ज्ञानावरण का क्षय युगपत् होता है। उस क्षय से होने वाले उपयोग में 'यह प्रथम होता है, यह बाद में होता है' इस प्रकार का भेद किस प्रकार से किया जा सकता है? कैवल्य की प्राप्ति जिस समय होती है उस समय सर्वप्रथम मोहनीयकर्म का क्षय होता है। उसके पश्चात् ज्ञानावरण और दर्शनावरण तथा अन्तराय का युगपत् क्षय होता है। जब दर्शनावरण और ज्ञानावरण दोनों के क्षय में काल का भेद नहीं है, तब यह किस आधार पर कहा जा सकता है कि प्रथम केवलदर्शन होता है, बाद में केवलज्ञान। इस समस्या के समाधान के लिए कोई यह माने कि दोनों का युगपत् सद्भाव है तो यह भी उचित नहीं, क्योंकि एक साथ दो उपयोग नहीं हो सकते। इस समस्या का सबसे सरल और तर्कसंगत समाधान यह है कि केवली अवस्था में दर्शन और ज्ञान में भेद नहीं होता। दर्शन और ज्ञान को पृथक् पृथक् मानने से एक समस्या और उत्पन्न होती है कि यदि केवली एक ही क्षण में सभी कुछ जान लेता है तो उसे सदा के लिए सब कुछ जानते रहना चाहिए। यदि उसका ज्ञान सदा पूर्ण नहीं है तो वह सर्वज्ञ कैसा ? यदि उसका ज्ञान सदा पूर्ण है तो क्रम और अक्रम का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। वह सदा एकरूप है। वहाँ पर दर्शन और ज्ञान में किसी भी प्रकार का कोई अन्तर नहीं है। ज्ञान सविकल्प है और दर्शन निर्विकल्प है, इस प्रकार का भेद आवरण रूप कर्म के क्षय के पश्चात् नहीं रहता। जहाँ पर उपयोग की अपूर्णता है, वहीं पर सविकल्पक और निर्विकल्पक का भेद होता है। पूर्ण उपयोग होने पर किसी प्रकार का भेद नहीं होता । एक समस्या और है, और वह यह है कि ज्ञान हमेशा दर्शनपूर्वक होता है किन्तु दर्शन ज्ञानपूर्वक नहीं होता।' केवली को एक बार जब सम्पूर्ण ज्ञान हो जाता है तब फिर दर्शन नहीं हो सकता, क्योंकि दर्शन ज्ञानपूर्वक नहीं होता । एतदर्थ ज्ञान और दर्शन का क्रमभाव नहीं घट सकता।
दिगम्बर परम्परा में केवल युगपत् पक्ष ही मान्य रहा है। श्वेताम्बरपरम्परा में इसकी क्रम, युगपत् और अभेद ये तीन धाराएँ बनीं। इन तीनों धाराओं का विक्रम की सत्रहवीं शताब्दी के महान् तार्किक उपा. श्री यशोविजयजी ने नयी दृष्टि से समन्वय किया है। ऋजुसूत्रनय की दृष्टि से क्रमिक पक्ष संगत है। यह दृष्टि वर्तमान समय को करती है। प्रथम समय का ज्ञान कारण है और द्वितीय समय का दर्शन उसका कार्य है। ज्ञान और दर्शन में कारण और कार्य का क्रम है। व्यवहारनय भेदस्पर्शी है। उसकी दृष्टि से युगपत् पक्ष भी संगत हैं। संग्रहनय अभेदस्पर्शी है, उसकी दृष्टि से अभेद पक्ष भी संगत है। तर्कदृष्टि से देखने पर इन तीन धाराओं में अभेद पक्ष अधिक युक्तिसंगत लगता है। दूसरा दृष्टिकोण आगमिक है। उसका प्रतिपादन स्वभावस्पर्शी है। प्रथम समय में वस्तुगत भिन्नताओं को जानना और दूसरे समय में भिन्नतागत अभिन्नता को जानना स्वभावसिद्ध है। ज्ञान का स्वभाव ही इस प्रकार का है कि भेद अभेद और अभेद में भेद समाया हुआ है, तथापि भेदप्रधान ज्ञान और अभेदप्रधान दर्शन का समय एक नहीं होता ।
प्रज्ञापना में उपयोग और पश्यता के सम्बन्ध में अन्य चर्चा नहीं है । अवधिपद में अवधिज्ञान के सम्बन्ध में भेद, विषय, संस्थान, आभ्यन्तर और बाह्य अवधि, देशावधि, अवधि की क्षय वृद्धि, प्रतिपाति और अप्रतिपाति, इन सात विषयों की विस्तृत चर्चा है। अवधिज्ञान के दो भेद हैं- एक तो जन्म से प्राप्त होता है, दूसरा कर्म के क्षयोपशम से। देवों नारकों में जन्म से ही अवधिज्ञान होता है, किन्तु मनुष्यों और तिर्यच पंचेन्द्रियों का अवधिज्ञान क्षयोपशमिक
१. सन्मति० प्रकरण २/३; २. सन्मति० प्रकरण २ / ९ ३ सन्मति० प्रकरण २/१० ४. सन्मति० प्रकरण २/११ ५. सन्मति० प्रकरण २ / २२ ६. ज्ञानबिन्दु, पृष्ठ १५४-१६४ ७. (क) विशेष विवरण के लिए देखिए धर्मसंग्रहणी गाथा १३३६ - १३५९ (ख) तत्त्वार्थसूत्र, सिद्धसेन गणी टीका, अध्याय १, सू० ३१ पृ, ७७/१ (ग) नन्दीसूत्र, आचार्य श्री मलयगिरिजी वृत्ति पृ. १३४ - १३८
61