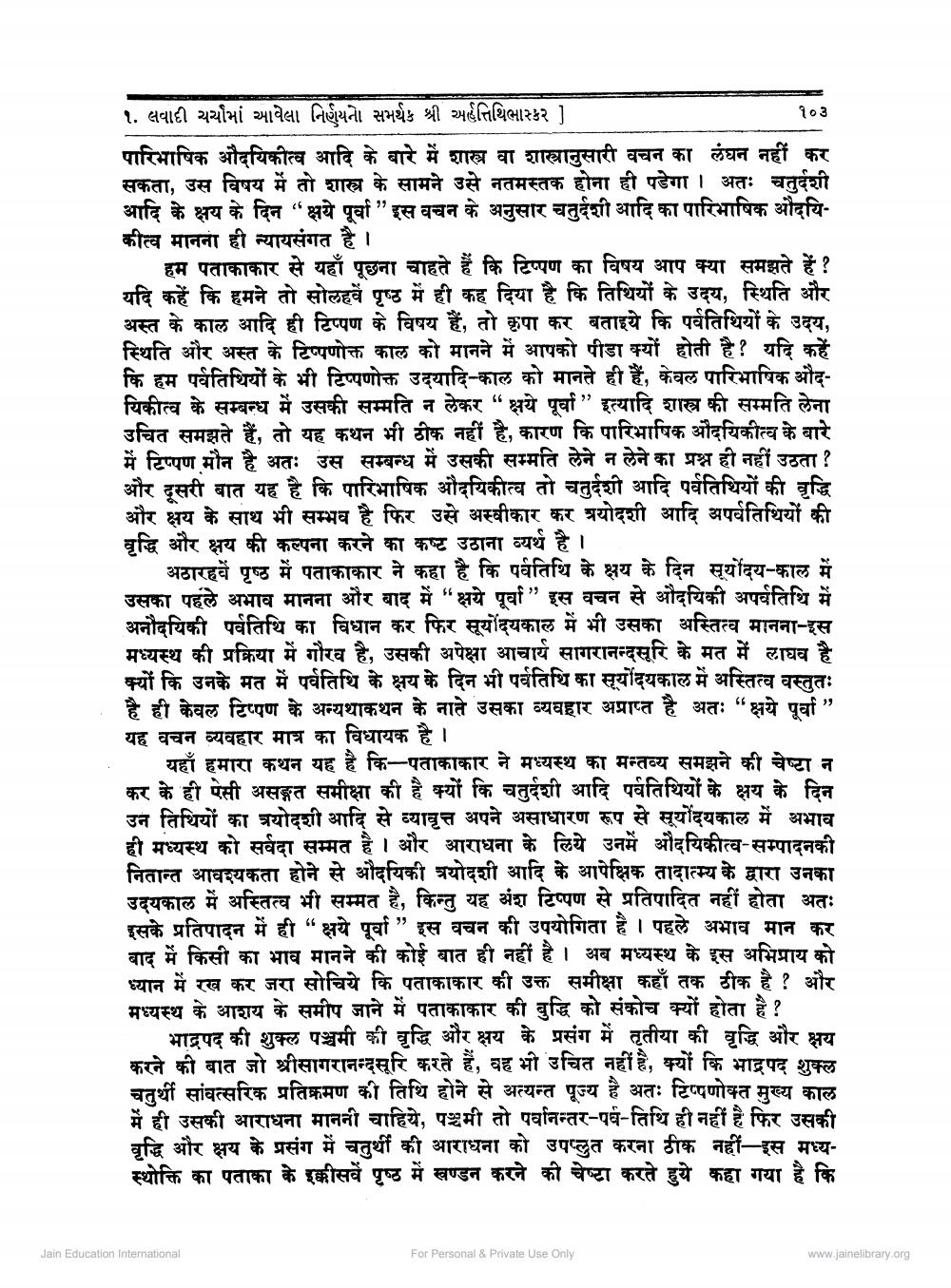________________
103
૧. લવાદી ચર્ચામાં આવેલા નિર્ણયને સમર્થક શ્રી અહરિથિભાસ્કર ] पारिभाषिक औदयिकीत्व आदि के बारे में शास्त्र वा शास्त्रानुसारी वचन का लंघन नहीं कर सकता, उस विषय में तो शास्त्र के सामने उसे नतमस्तक होना ही पडेगा । अतः चतुर्दशी आदि के क्षय के दिन “क्षये पूर्वा" इस वचन के अनुसार चतुर्दशी आदि का पारिभाषिक औदयिकीत्व मानना ही न्यायसंगत है।
हम पताकाकार से यहाँ पूछना चाहते हैं कि टिप्पण का विषय आप क्या समझते हैं ? यदि कहें कि हमने तो सोलहवें पृष्ठ में ही कह दिया है कि तिथियों के उदय, स्थिति और अस्त के काल आदि ही टिप्पण के विषय हैं, तो कृपा कर बताइये कि पर्वतिथियों के उदय, स्थिति और अस्त के टिप्पणोक्त काल को मानने में आपको पीडा क्यों होती है ? यदि कहें कि हम पर्वतिथियों के भी टिप्पणोक्त उदयादि-काल को मानते ही हैं, केवल पारिभाषिक औदयिकीत्व के सम्बन्ध में उसकी सम्मति न लेकर "क्षये पूर्वा" इत्यादि शास्त्र की सम्मति लेना उचित समझते हैं, तो यह कथन भी ठीक नहीं है, कारण कि पारिभाषिक औदयिकीत्व के बारे में टिप्पण मौन है अतः उस सम्बन्ध में उसकी सम्मति लेने न लेने का प्रश्न ही नहीं उठता ? और दूसरी बात यह है कि पारिभाषिक औदयिकीत्व तो चतुर्दशी आदि पर्वतिथियों की वृद्धि और क्षय के साथ भी सम्भव है फिर उसे अस्वीकार कर त्रयोदशी आदि अपर्वतिथियों की वृद्धि और क्षय की कल्पना करने का कष्ट उठाना व्यर्थ है।
अठारहवें पृष्ठ में पताकाकार ने कहा है कि पर्वतिथि के क्षय के दिन सर्योदय-काल में उसका पहले अभाव मानना और बाद में “क्षये पूर्वा" इस वचन से औदयिकी अपर्वतिथि में अनौदयिकी पर्वतिथि का विधान कर फिर सूर्योदयकाल में भी उसका अस्तित्व मानना-इस मध्यस्थ की प्रक्रिया में गौरव है, उसकी अपेक्षा आचार्य सागरानन्दसूरि के मत में लाघव है क्यों कि उनके मत में पर्वतिथि के क्षय के दिन भी पर्वतिथि का सूर्योदयकाल में अस्तित्व वस्तुतः
ही केवल टिप्पण के अन्यथाकथन के नाते उसका व्यवहार अप्राप्त है अतः "क्षये पर्वा" यह वचन व्यवहार मात्र का विधायक है।
यहाँ हमारा कथन यह है कि-पताकाकार ने मध्यस्थ का मन्तव्य समझने की चेष्टा न कर के ही ऐसी असङ्गत समीक्षा की है क्यों कि चतुर्दशी आदि पर्वतिथियों के क्षय के दिन उन तिथियों का त्रयोदशी आदि से व्यावृत्त अपने असाधारण रूप से सूर्योदयकाल में अभाव ही मध्यस्थ को सर्वदा सम्मत है । और आराधना के लिये उनमें औदयिकीत्व-सम्पादनकी नितान्त आवश्यकता होने से औदयिकी त्रयोदशी आदि के आपेक्षिक तादात्म्य के द्वारा उनका उदयकाल में अस्तित्व भी सम्मत है, किन्तु यह अंश टिप्पण से प्रतिपादित नहीं होता अतः इसके प्रतिपादन में ही “क्षये पूर्वा” इस वचन की उपयोगिता है । पहले अभाव मान कर बाद में किसी का भाव मानने की कोई बात ही नहीं है। अब मध्यस्थ के इस अभिप्राय को ध्यान में रख कर जरा सोचिये कि पताकाकार की उक्त समीक्षा कहाँ तक ठीक है ? और मध्यस्थ के आशय के समीप जाने में पताकाकार की बुद्धि को संकोच क्यों होता है? ___ भाद्रपद की शुक्ल पञ्चमी की वृद्धि और क्षय के प्रसंग में तृतीया की वृद्धि और क्षय करने की बात जो श्रीसागरानन्दसूरि करते हैं, वह भी उचित नहीं है, क्यों कि भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी सांवत्सरिक प्रतिक्रमण की तिथि होने से अत्यन्त पूज्य है अतः टिप्पणोक्त मुख्य काल में ही उसकी आराधना माननी चाहिये, पञ्चमी तो पर्वानन्तर-पर्व-तिथि ही नहीं है फिर उसकी वृद्धि और क्षय के प्रसंग में चतुर्थी की आराधना को उपप्लुत करना ठीक नहीं-इस मध्यस्थोक्ति का पताका के इक्कीसवें पृष्ठ में खण्डन करने की चेष्टा करते हुये कहा गया है कि
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org