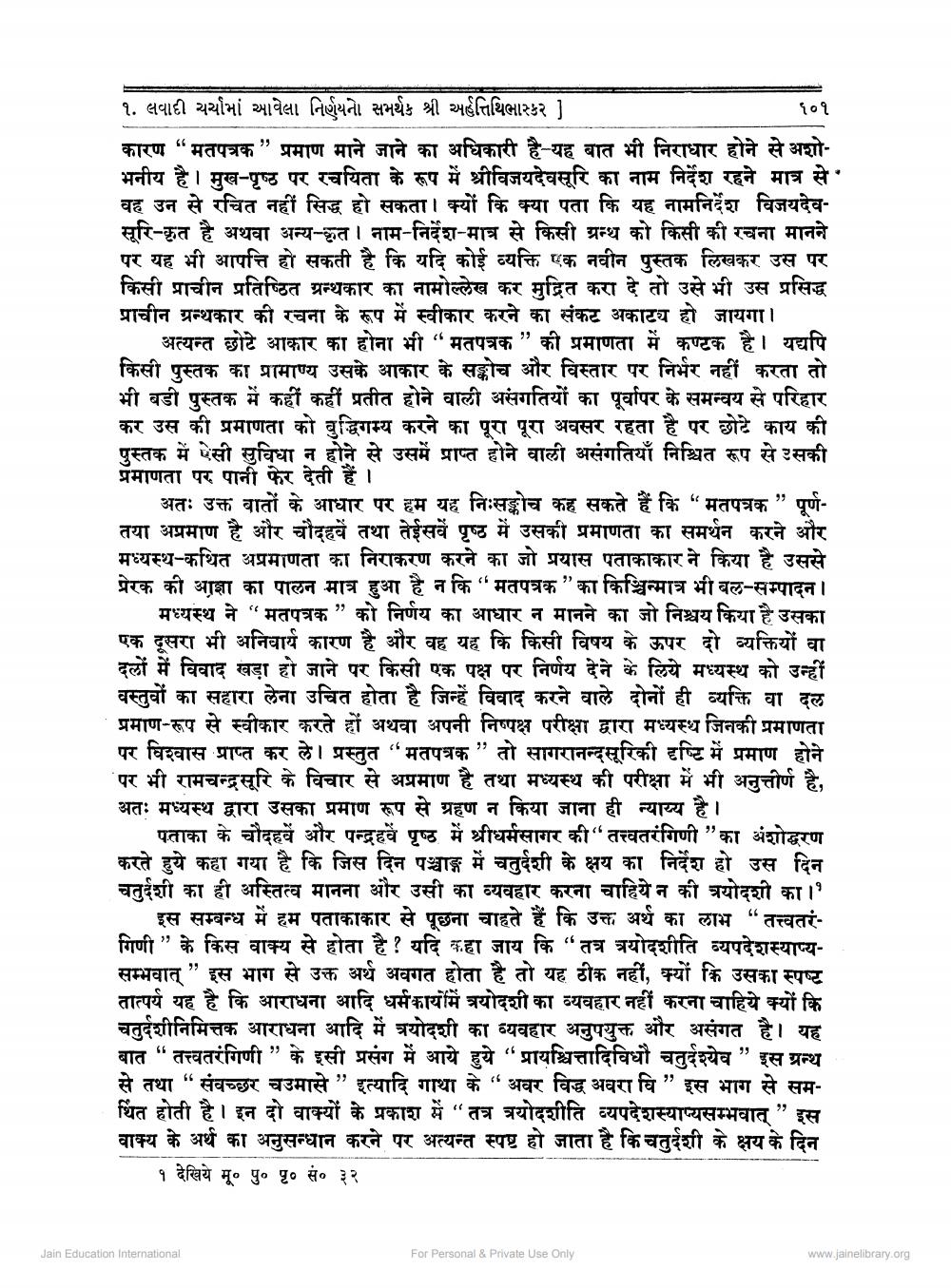________________
१०१
૧. લવાદી ચર્ચામાં આવેલા નિર્ણયને સમર્થક શ્રી અહતિથિભાસ્કર ]. कारण “मतपत्रक" प्रमाण माने जाने का अधिकारी है-यह बात भी निराधार होने से अशोभनीय है। मुख-पृष्ठ पर रचयिता के रूप में श्रीविजयदेवसूरि का नाम निर्देश रहने मात्र से वह उन से रचित नहीं सिद्ध हो सकता। क्यों कि क्या पता कि यह नामनिर्देश विजयदेवसूरि-कृत है अथवा अन्य-कृत । नाम-निर्देश-मात्र से किसी ग्रन्थ को किसी की रचना मानने पर यह भी आपत्ति हो सकती है कि यदि कोई व्यक्ति एक नवीन पुस्तक लिखकर उस पर किसी प्राचीन प्रतिष्ठित ग्रन्थकार का नामोल्लेख कर मुद्रित करा दे तो उसे भी उस प्रसिद्ध प्राचीन ग्रन्थकार की रचना के रूप में स्वीकार करने का संकट अकाटय हो जायगा। ___अत्यन्त छोटे आकार का होना भी “मतपत्रक" की प्रमाणता में कण्टक है। यद्यपि किसी पुस्तक का प्रामाण्य उसके आकार के सङ्कोच और विस्तार पर निर्भर नहीं करता तो भी बडी पुस्तक में कहीं कहीं प्रतीत होने वाली असंगतियों का पूर्वापर के समन्वय से परिहार कर उस की प्रमाणता को बुद्धिगम्य करने का पूरा पूरा अवसर रहता है पर छोटे काय की पुस्तक में ऐसी सुविधा न होने से उसमें प्राप्त होने वाली असंगतियाँ निश्चित रूप से उसकी प्रमाणता पर पानी फेर देती हैं। ___अतः उक्त बातों के आधार पर हम यह निःसङ्कोच कह सकते हैं कि “मतपत्रक" पूर्णतया अप्रमाण है और चौदहवें तथा तेईसवें पृष्ठ में उसकी प्रमाणता का समर्थन करने और मध्यस्थ-कथित अप्रमाणता का निराकरण करने का जो प्रयास पताकाकार ने किया है उससे प्रेरक की आज्ञा का पालन मात्र हुआ है न कि "मतपत्रक" का किश्चिन्मात्र भी बल-सम्प
मध्यस्थ ने “मतपत्रक" को निर्णय का आधार न मानने का जो निश्चय किया है उसका एक दूसरा भी अनिवार्य कारण है और वह यह कि किसी विषय के ऊपर दो व्यक्तियों वा दलों में विवाद खड़ा हो जाने पर किसी एक पक्ष पर निर्णय देने के लिये मध्यस्थ को उन्हीं वस्तुवों का सहारा लेना उचित होता है जिन्हें विवाद करने वाले दोनों ही व्यक्ति वा दल प्रमाण-रूप से स्वीकार करते हों अथवा अपनी निष्पक्ष परीक्षा द्वारा मध्यस्थ जिनकी प्रमाणता पर विश्वास प्राप्त कर ले। प्रस्तुत “मतपत्रक" तो सागरानन्दसूरिकी दृष्टि में प्रमाण होने पर भी रामचन्द्रसूरि के विचार से अप्रमाण है तथा मध्यस्थ की परीक्षा में भी अनुत्तीर्ण है, अतः मध्यस्थ द्वारा उसका प्रमाण रूप से ग्रहण न किया जाना ही न्याय्य है।
पताका के चौदहवें और पन्द्रहवें पृष्ठ में श्रीधर्मसागर की “तत्त्वतरंगिणी" का अंशोद्धरण करते हुये कहा गया है कि जिस दिन पञ्चाङ्ग में चतुर्दशी के क्षय का निर्देश हो उस दिन चतुर्दशी का ही अस्तित्व मानना और उसी का व्यवहार करना चाहिये न की त्रयोदशी का।' ___ इस सम्बन्ध में हम पताकाकार से पूछना चाहते हैं कि उक्त अर्थ का लाभ “तत्त्वतरंगिणी" के किस वाक्य से होता है ? यदि कहा जाय कि “तत्र त्रयोदशीति व्यपदेशस्याप्यसम्भवात्" इस भाग से उक्त अर्थ अवगत होता है तो यह ठीक नहीं, क्यों कि उसका स्पष्ट तात्पर्य यह है कि आराधना आदि धर्मकार्योमें त्रयोदशी का व्यवहार नहीं करना चाहिये क्यों कि चतुर्दशीनिमित्तक आराधना आदि में त्रयोदशी का व्यवहार अनुपयुक्त और असंगत है। यह बात " तत्त्वतरंगिणी" के इसी प्रसंग में आये हुये "प्रायश्चित्तादिविधौ चतुर्दश्येव" इस ग्रन्थ से तथा “संवच्छर चउमासे” इत्यादि गाथा के “ अवर विद्ध अवरा वि" इस भाग से समथित होती है। इन दो वाक्यों के प्रकाश में “तत्र त्रयोदशीति व्यपदेशस्याप्यसम्भवात् " इस वाक्य के अर्थ का अनुसन्धान करने पर अत्यन्त स्पष्ट हो जाता है कि चतुर्दशी के क्षय के दिन
१ देखिये मू० पु. पृ० सं० ३२
Jain Education International
For Personal & Private Use Only
www.jainelibrary.org