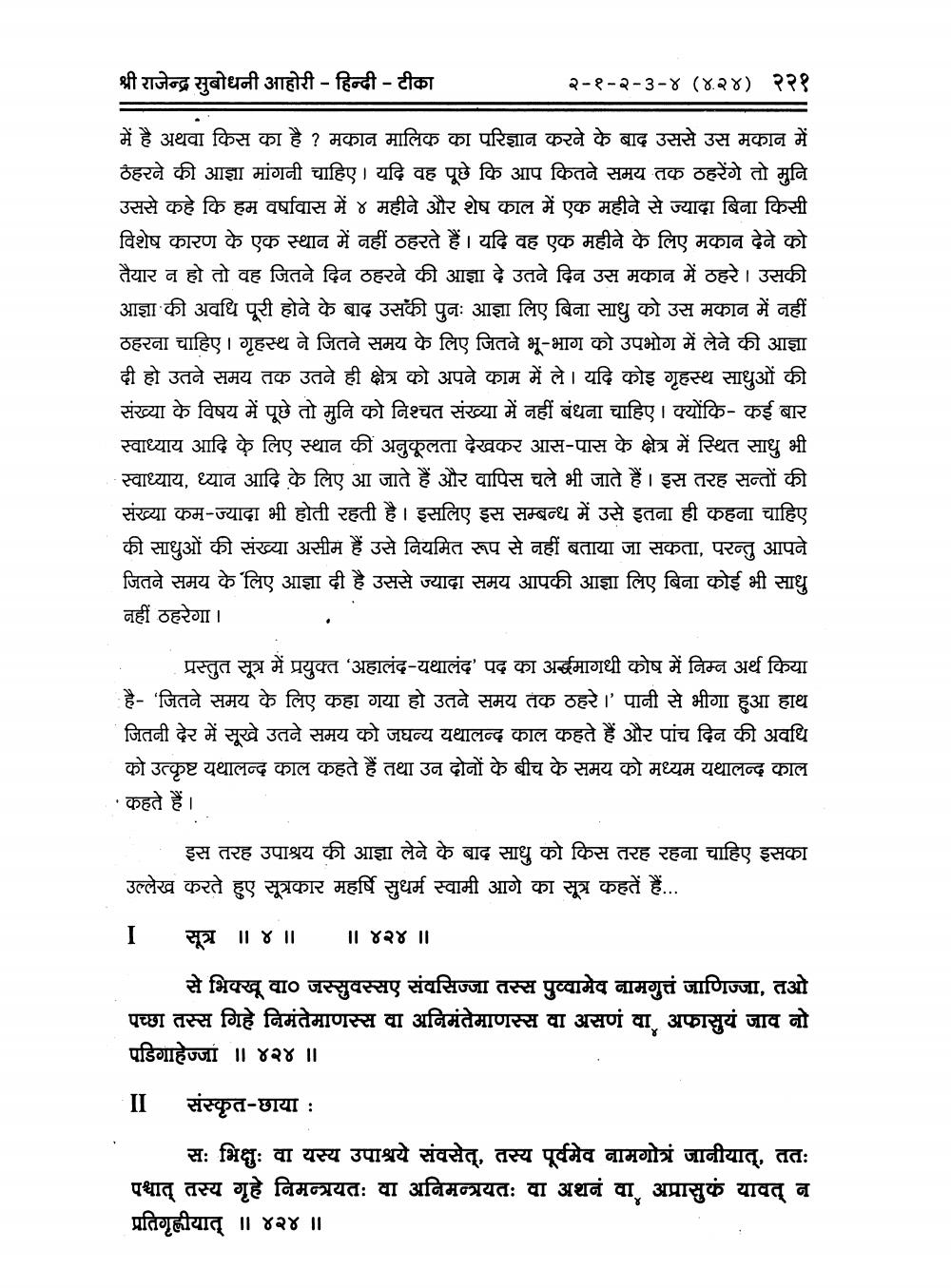________________ श्री राजेन्द्र सुबोधनी आहोरी - हिन्दी - टीका 2-1-2-3-4 (4.24) 221 में है अथवा किस का है ? मकान मालिक का परिज्ञान करने के बाद उससे उस मकान में ठहरने की आज्ञा मांगनी चाहिए। यदि वह पूछे कि आप कितने समय तक ठहरेंगे तो मुनि उससे कहे कि हम वर्षावास में 4 महीने और शेष काल में एक महीने से ज्यादा बिना किसी विशेष कारण के एक स्थान में नहीं ठहरते हैं। यदि वह एक महीने के लिए मकान देने को तैयार न हो तो वह जितने दिन ठहरने की आज्ञा दे उतने दिन उस मकान में ठहरे। उसकी आज्ञा की अवधि पूरी होने के बाद उसकी पुनः आज्ञा लिए बिना साधु को उस मकान में नहीं ठहरना चाहिए। गृहस्थ ने जितने समय के लिए जितने भू-भाग को उपभोग में लेने की आज्ञा दी हो उतने समय तक उतने ही क्षेत्र को अपने काम में ले। यदि कोइ गृहस्थ साधुओं की संख्या के विषय में पूछे तो मुनि को निश्चत संख्या में नहीं बंधना चाहिए। क्योंकि- कई बार स्वाध्याय आदि के लिए स्थान की अनुकूलता देखकर आस-पास के क्षेत्र में स्थित साधु भी स्वाध्याय, ध्यान आदि के लिए आ जाते हैं और वापिस चले भी जाते हैं। इस तरह सन्तों की संख्या कम-ज्यादा भी होती रहती है। इसलिए इस सम्बन्ध में उसे इतना ही कहना चाहिए की साधुओं की संख्या असीम हैं उसे नियमित रूप से नहीं बताया जा सकता, परन्तु आपने जितने समय के लिए आज्ञा दी है उससे ज्यादा समय आपकी आज्ञा लिए बिना कोई भी साधु नहीं ठहरेगा। . प्रस्तुत सूत्र में प्रयुक्त 'अहालंद-यथालंद' पद का अर्द्धमागधी कोष में निम्न अर्थ किया है- 'जितने समय के लिए कहा गया हो उतने समय तक ठहरे।' पानी से भीगा हुआ हाथ जितनी देर में सूखे उतने समय को जघन्य यथालन्द काल कहते हैं और पांच दिन की अवधि को उत्कृष्ट यथालन्द काल कहते हैं तथा उन दोनों के बीच के समय को मध्यम यथालन्द काल * कहते हैं। - इस तरह उपाश्रय की आज्ञा लेने के बाद साधु को किस तरह रहना चाहिए इसका उल्लेख करते हुए सूत्रकार महर्षि सुधर्म स्वामी आगे का सूत्र कहतें हैं... सूत्र // 4 // // 424 // से भिक्खू वा० जस्सुवस्सए संवसिज्जा तस्स पुव्वामेव नामगुत्तं जाणिज्जा, तओ पच्छा तस्स गिहे निमंतेमाणस्स वा अनिमंतेमाणस्स वा असणं वा, अफासुयं जाव नो पडिगाहेज्जा // 424 // II संस्कृत-छाया : स: भिक्षुः वा यस्य उपाश्रये संवसेत्, तस्य पूर्वमेव नामगोत्रं जानीयात्, ततः पश्चात् तस्य गृहे निमन्त्रयतः वा अनिमन्त्रयतः वा अथनं वा, अप्रासुकं यावत् न प्रतिगृह्णीयात् // 424 //