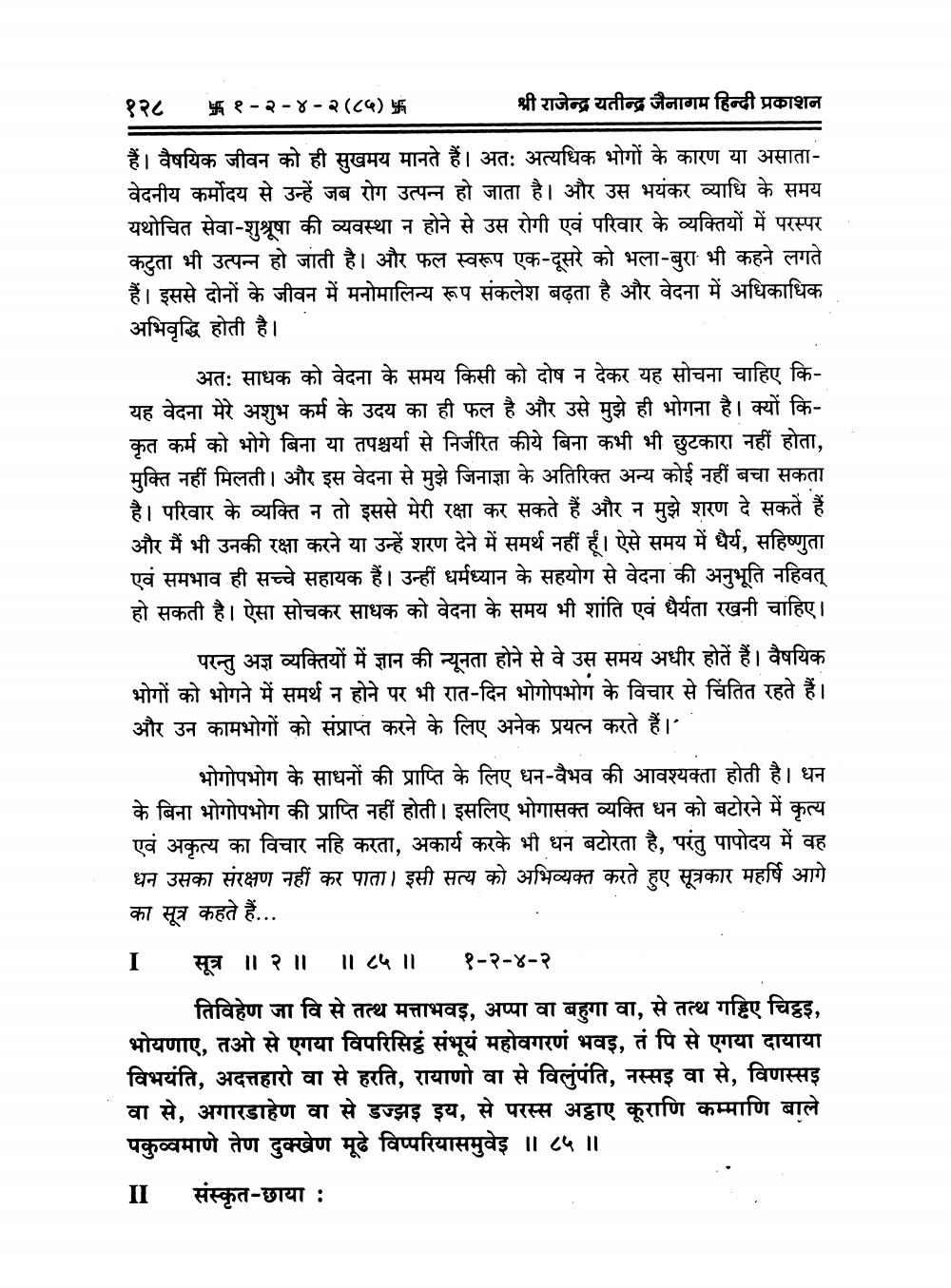________________ 128 1-2-4-2(85) // श्री राजेन्द्र यतीन्द्र जैनागम हिन्दी प्रकाशन हैं। वैषयिक जीवन को ही सुखमय मानते हैं। अतः अत्यधिक भोगों के कारण या असातावेदनीय कर्मोदय से उन्हें जब रोग उत्पन्न हो जाता है। और उस भयंकर व्याधि के समय यथोचित सेवा-शुश्रूषा की व्यवस्था न होने से उस रोगी एवं परिवार के व्यक्तियों में परस्पर कटुता भी उत्पन्न हो जाती है। और फल स्वरूप एक-दूसरे को भला-बुरा भी कहने लगते हैं। इससे दोनों के जीवन में मनोमालिन्य रूप संकलेश बढ़ता है और वेदना में अधिकाधिक अभिवृद्धि होती है। __ अत: साधक को वेदना के समय किसी को दोष न देकर यह सोचना चाहिए कियह वेदना मेरे अशुभ कर्म के उदय का ही फल है और उसे मुझे ही भोगना है। क्यों किकृत कर्म को भोगे बिना या तपश्चर्या से निर्जरित कीये बिना कभी भी छुटकारा नहीं होता, मुक्ति नहीं मिलती। और इस वेदना से मुझे जिनाज्ञा के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं बचा सकता है। परिवार के व्यक्ति न तो इससे मेरी रक्षा कर सकते हैं और न मुझे शरण दे सकते हैं और मैं भी उनकी रक्षा करने या उन्हें शरण देने में समर्थ नहीं हूँ। ऐसे समय में धैर्य, सहिष्णुता एवं समभाव ही सच्चे सहायक हैं। उन्हीं धर्मध्यान के सहयोग से वेदना की अनुभूति नहिवत् हो सकती है। ऐसा सोचकर साधक को वेदना के समय भी शांति एवं धैर्यता रखनी चाहिए। परन्तु अज्ञ व्यक्तियों में ज्ञान की न्यूनता होने से वे उस समय अधीर होते हैं। वैषयिक भोगों को भोगने में समर्थ न होने पर भी रात-दिन भोगोपभोग के विचार से चिंतित रहते हैं। और उन कामभोगों को संप्राप्त करने के लिए अनेक प्रयत्न करते हैं।' भोगोपभोग के साधनों की प्राप्ति के लिए धन-वैभव की आवश्यक्ता होती है। धन के बिना भोगोपभोग की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए भोगासक्त व्यक्ति धन को बटोरने में कृत्य एवं अकृत्य का विचार नहि करता, अकार्य करके भी धन बटोरता है, परंतु पापोदय में वह धन उसका संरक्षण नहीं कर पाता। इसी सत्य को अभिव्यक्त करते हुए सूत्रकार महर्षि आगे का सूत्र कहते हैं... I सूत्र // 2 // // 85 // 1-2-4-2 तिविहेण जा वि से तत्थ मत्ताभवइ, अप्पा वा बहुगा वा, से तत्थ गड्डिए चिट्ठइ, भोयणाए, तओ से एगया विपरिसिहॅ संभूयं महोवगरणं भवइ, तं पि से एगया दायाया विभयंति, अदत्तहारो वा से हरति, रायाणो वा से विलुपंति, नस्सइ वा से, विणस्सइ वा से, अगारडाहेण वा से डज्झइ इय, से परस्स अट्ठाए कूराणि कम्माणि बाले पकुव्वमाणे तेण दुक्खेण मूढे विप्परियासमुवेइ // 85 // II संस्कृत-छाया :