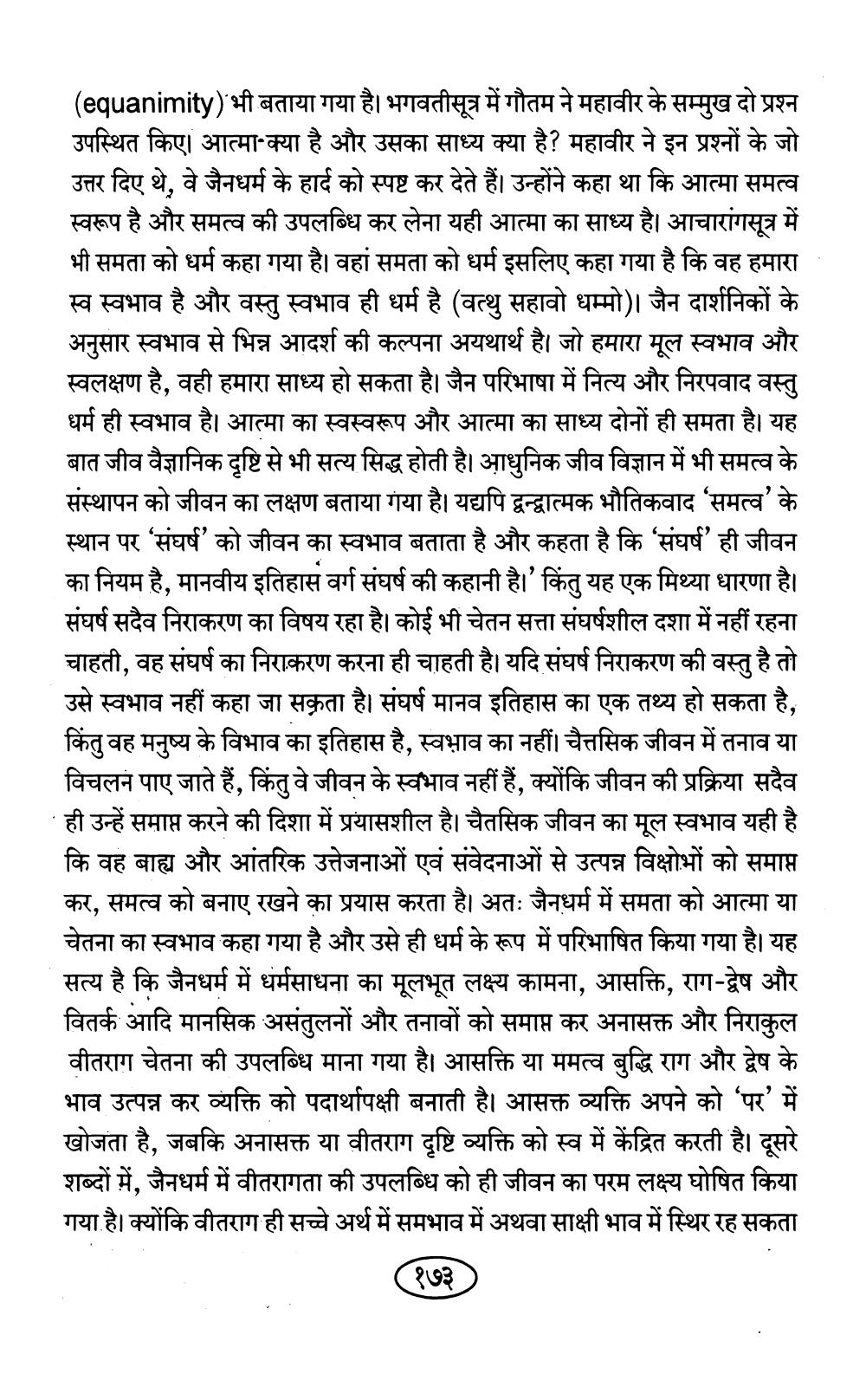________________ (equanimity) भी बताया गया है। भगवतीसूत्र में गौतम ने महावीर के सम्मुख दो प्रश्न उपस्थित किए। आत्मा क्या है और उसका साध्य क्या है? महावीर ने इन प्रश्नों के जो उत्तर दिए थे, वे जैनधर्म के हार्द को स्पष्ट कर देते हैं। उन्होंने कहा था कि आत्मा समत्व स्वरूप है और समत्व की उपलब्धि कर लेना यही आत्मा का साध्य है। आचारांगसूत्र में भी समता को धर्म कहा गया है। वहां समता को धर्म इसलिए कहा गया है कि वह हमारा स्व स्वभाव है और वस्तु स्वभाव ही धर्म है (वत्थु सहावो धम्मो)। जैन दार्शनिकों के अनुसार स्वभाव से भिन्न आदर्श की कल्पना अयथार्थ है। जो हमारा मूल स्वभाव और स्वलक्षण है, वही हमारा साध्य हो सकता है। जैन परिभाषा में नित्य और निरपवाद वस्तु धर्म ही स्वभाव है। आत्मा का स्वस्वरूप और आत्मा का साध्य दोनों ही समता है। यह बात जीव वैज्ञानिक दृष्टि से भी सत्य सिद्ध होती है। आधुनिक जीव विज्ञान में भी समत्व के संस्थापन को जीवन का लक्षण बताया गया है। यद्यपि द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद 'समत्व' के स्थान पर 'संघर्ष' को जीवन का स्वभाव बताता है और कहता है कि 'संघर्ष' ही जीवन का नियम है, मानवीय इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है। किंतु यह एक मिथ्या धारणा है। संघर्ष सदैव निराकरण का विषय रहा है। कोई भी चेतन सत्ता संघर्षशील दशा में नहीं रहना चाहती, वह संघर्ष का निराकरण करना ही चाहती है। यदि संघर्ष निराकरण की वस्तु है तो उसे स्वभाव नहीं कहा जा सकता है। संघर्ष मानव इतिहास का एक तथ्य हो सकता है, किंतु वह मनुष्य के विभाव का इतिहास है, स्वभाव का नहीं। चैत्तसिक जीवन में तनाव या विचलन पाए जाते हैं, किंतु वे जीवन के स्वभाव नहीं हैं, क्योंकि जीवन की प्रक्रिया सदैव ही उन्हें समाप्त करने की दिशा में प्रयासशील है। चैतसिक जीवन का मूल स्वभाव यही है कि वह बाह्य और आंतरिक उत्तेजनाओं एवं संवेदनाओं से उत्पन्न विक्षोभों को समाप्त कर, समत्व को बनाए रखने का प्रयास करता है। अतः जैनधर्म में समता को आत्मा या चेतना का स्वभाव कहा गया है और उसे ही धर्म के रूप में परिभाषित किया गया है। यह सत्य है कि जैनधर्म में धर्मसाधना का मूलभूत लक्ष्य कामना, आसक्ति, राग-द्वेष और वितर्क आदि मानसिक असंतुलनों और तनावों को समाप्त कर अनासक्त और निराकुल वीतराग चेतना की उपलब्धि माना गया है। आसक्ति या ममत्व बुद्धि राग और द्वेष के भाव उत्पन्न कर व्यक्ति को पदार्थापक्षी बनाती है। आसक्त व्यक्ति अपने को 'पर' में खोजता है, जबकि अनासक्त या वीतराग दृष्टि व्यक्ति को स्व में केंद्रित करती है। दूसरे शब्दों में, जैनधर्म में वीतरागता की उपलब्धि को ही जीवन का परम लक्ष्य घोषित किया गया है। क्योंकि वीतराग ही सच्चे अर्थ में समभाव में अथवा साक्षी भाव में स्थिर रह सकता