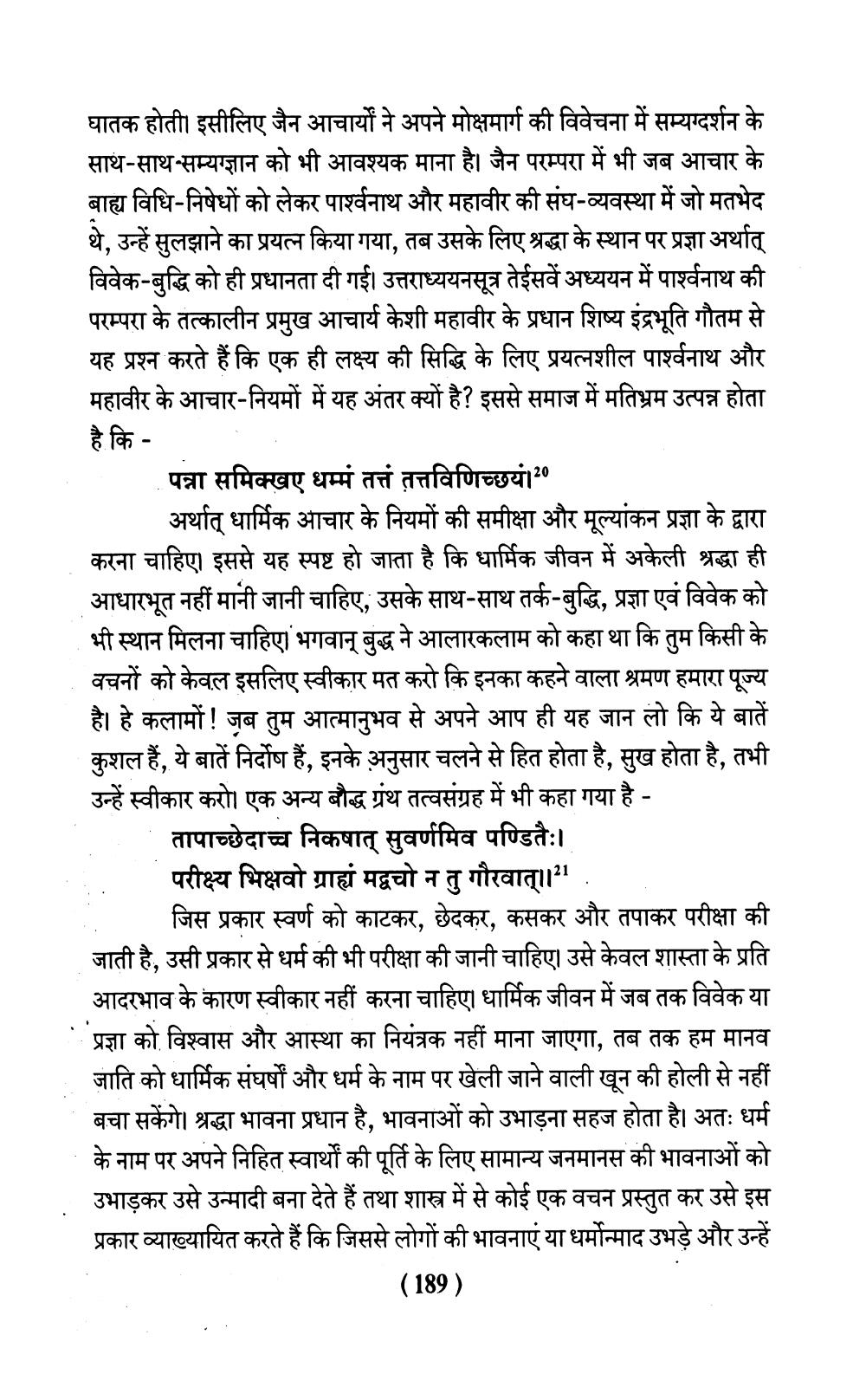________________ घातक होती। इसीलिए जैन आचार्यों ने अपने मोक्षमार्ग की विवेचना में सम्यग्दर्शन के साथ-साथ-सम्यग्ज्ञान को भी आवश्यक माना है। जैन परम्परा में भी जब आचार के बाह्य विधि-निषेधों को लेकर पार्श्वनाथ और महावीर की संघ-व्यवस्था में जो मतभेद थे, उन्हें सुलझाने का प्रयत्न किया गया, तब उसके लिए श्रद्धा के स्थान पर प्रज्ञा अर्थात् विवेक-बुद्धि को ही प्रधानता दी गई। उत्तराध्ययनसूत्र तेईसवें अध्ययन में पार्श्वनाथ की परम्परा के तत्कालीन प्रमुख आचार्य केशी महावीर के प्रधान शिष्य इंद्रभूति गौतम से यह प्रश्न करते हैं कि एक ही लक्ष्य की सिद्धि के लिए प्रयत्नशील पार्श्वनाथ और महावीर के आचार-नियमों में यह अंतर क्यों है? इससे समाज में मतिभ्रम उत्पन्न होता है कि - पन्ना समिक्खए धम्मं तत्तं तत्तविणिच्छया अर्थात् धार्मिक आचार के नियमों की समीक्षा और मूल्यांकन प्रज्ञा के द्वारा करना चाहिए। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि धार्मिक जीवन में अकेली श्रद्धा ही आधारभूत नहीं मानी जानी चाहिए, उसके साथ-साथ तर्क-बुद्धि, प्रज्ञा एवं विवेक को भी स्थान मिलना चाहिए। भगवान् बुद्ध ने आलारकलाम को कहा था कि तुम किसी के वचनों को केवल इसलिए स्वीकार मत करो कि इनका कहने वाला श्रमण हमारा पूज्य है। हे कलामों! जब तुम आत्मानुभव से अपने आप ही यह जान लो कि ये बातें कुशल हैं, ये बातें निर्दोष हैं, इनके अनुसार चलने से हित होता है, सुख होता है, तभी उन्हें स्वीकार करो। एक अन्य बौद्ध ग्रंथ तत्वसंग्रह में भी कहा गया है - तापाच्छेदाच्च निकषात् सुवर्णमिव पण्डितैः। परीक्ष्य भिक्षवो ग्राह्यं मद्वचो न तु गौरवात्॥ . जिस प्रकार स्वर्ण को काटकर, छेदकर, कसकर और तपाकर परीक्षा की जाती है, उसी प्रकार से धर्म की भी परीक्षा की जानी चाहिए। उसे केवल शास्ता के प्रति आदरभाव के कारण स्वीकार नहीं करना चाहिए। धार्मिक जीवन में जब तक विवेक या प्रज्ञा को विश्वास और आस्था का नियंत्रक नहीं माना जाएगा, तब तक हम मानव जाति को धार्मिक संघर्षों और धर्म के नाम पर खेली जाने वाली खून की होली से नहीं बचा सकेंगे। श्रद्धा भावना प्रधान है, भावनाओं को उभाड़ना सहज होता है। अतः धर्म के नाम पर अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए सामान्य जनमानस की भावनाओं को उभाड़कर उसे उन्मादी बना देते हैं तथा शास्त्र में से कोई एक वचन प्रस्तुत कर उसे इस प्रकार व्याख्यायित करते हैं कि जिससे लोगों की भावनाएं या धर्मोन्माद उभड़े और उन्हें (189)