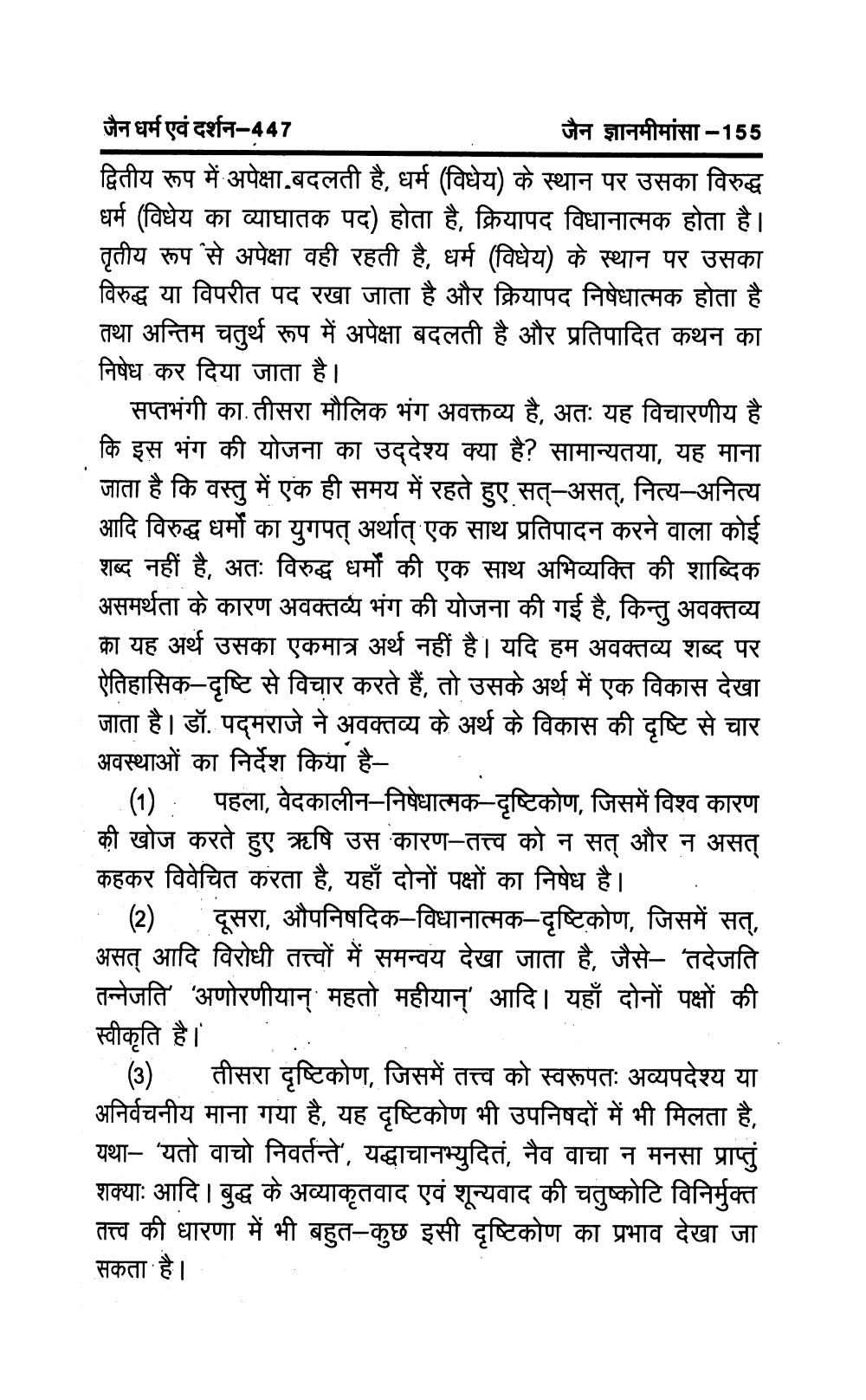________________ जैन धर्म एवं दर्शन-447 जैन ज्ञानमीमांसा-155 द्वितीय रूप में अपेक्षा.बदलती है, धर्म (विधेय) के स्थान पर उसका विरुद्ध धर्म (विधेय का व्याघातक पद) होता है, क्रियापद विधानात्मक होता है। तृतीय रूप से अपेक्षा वही रहती है, धर्म (विधेय) के स्थान पर उसका विरुद्ध या विपरीत पद रखा जाता है और क्रियापद निषेधात्मक होता है तथा अन्तिम चतुर्थ रूप में अपेक्षा बदलती है और प्रतिपादित कथन का निषेध कर दिया जाता है। ___ सप्तभंगी का तीसरा मौलिक भंग अवक्तव्य है, अतः यह विचारणीय है कि इस भंग की योजना का उद्देश्य क्या है? सामान्यतया, यह माना जाता है कि वस्तु में एक ही समय में रहते हुए सत्-असत्, नित्य-अनित्य आदि विरुद्ध धर्मों का युगपत् अर्थात् एक साथ प्रतिपादन करने वाला कोई शब्द नहीं है, अतः विरुद्ध धर्मों की एक साथ अभिव्यक्ति की शाब्दिक असमर्थता के कारण अवक्तव्य भंग की योजना की गई है, किन्तु अवक्तव्य का यह अर्थ उसका एकमात्र अर्थ नहीं है। यदि हम अवक्तव्य शब्द पर ऐतिहासिक-दृष्टि से विचार करते हैं, तो उसके अर्थ में एक विकास देखा जाता है। डॉ. पद्मराजे ने अवक्तव्य के अर्थ के विकास की दृष्टि से चार अवस्थाओं का निर्देश किया है___(1) : पहला, वेदकालीन-निषेधात्मक दृष्टिकोण, जिसमें विश्व कारण की खोज करते हुए ऋषि उस कारण-तत्त्व को न सत् और न असत् कहकर विवेचित करता है, यहाँ दोनों पक्षों का निषेध है। . (2) दूसरा, औपनिषदिक-विधानात्मक-दृष्टिकोण, जिसमें सत्, असत् आदि विरोधी तत्त्वों में समन्वय देखा जाता है, जैसे- 'तदेजति तन्नेजति' 'अणोरणीयान् महतो महीयान्' आदि। यहाँ दोनों पक्षों की स्वीकृति है। (3) तीसरा दृष्टिकोण, जिसमें तत्त्व को स्वरूपतः अव्यपदेश्य या अनिर्वचनीय माना गया है, यह दृष्टिकोण भी उपनिषदों में भी मिलता है, यथा- 'यतो वाचो निवर्तन्ते', यद्धाचानभ्युदितं, नैव वाचा न मनसा प्राप्तुं शक्याः आदि / बुद्ध के अव्याकृतवाद एवं शून्यवाद की चतुष्कोटि विनिर्मुक्त तत्त्व की धारणा में भी बहुत कुछ इसी दृष्टिकोण का प्रभाव देखा जा सकता है।